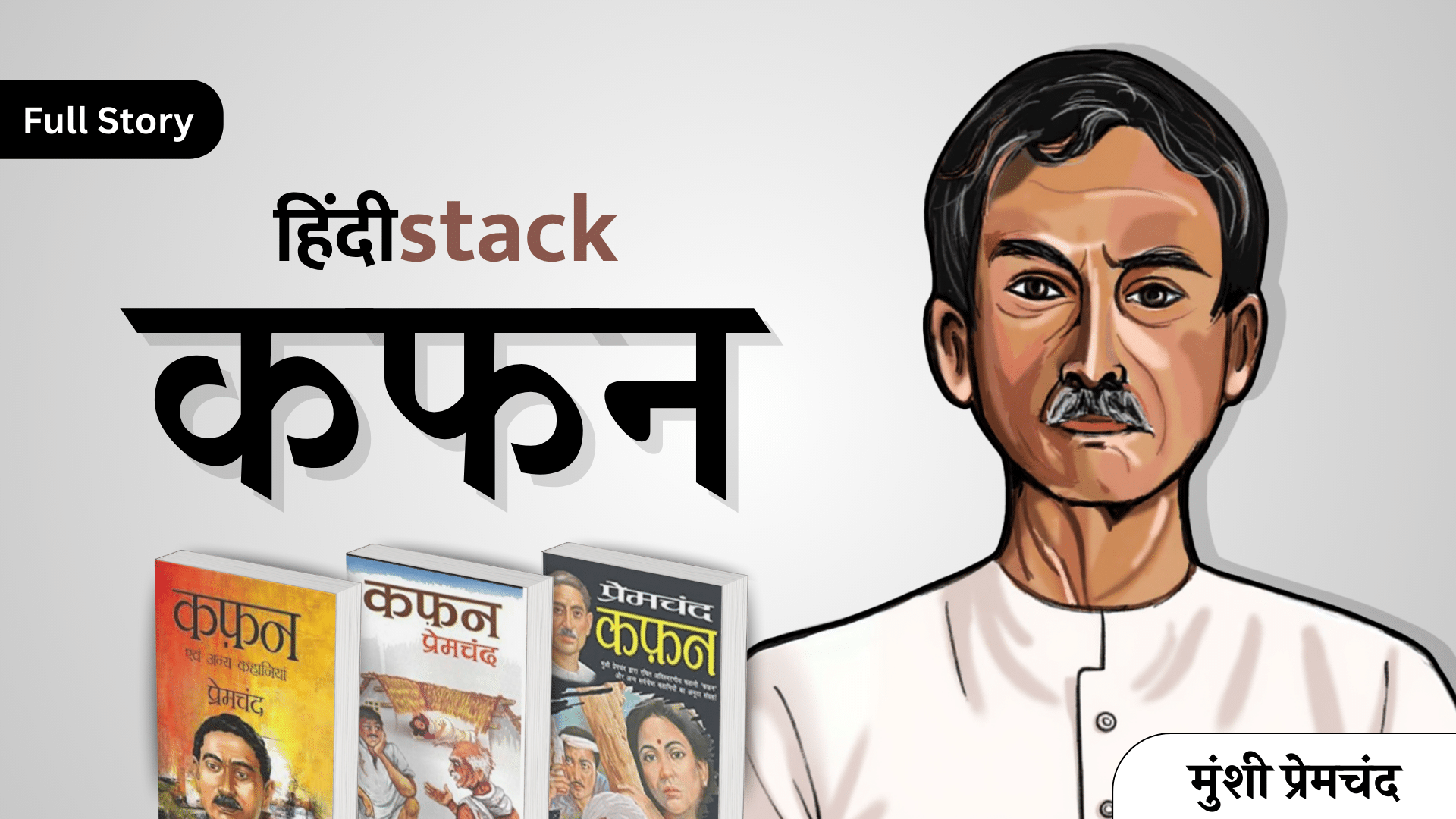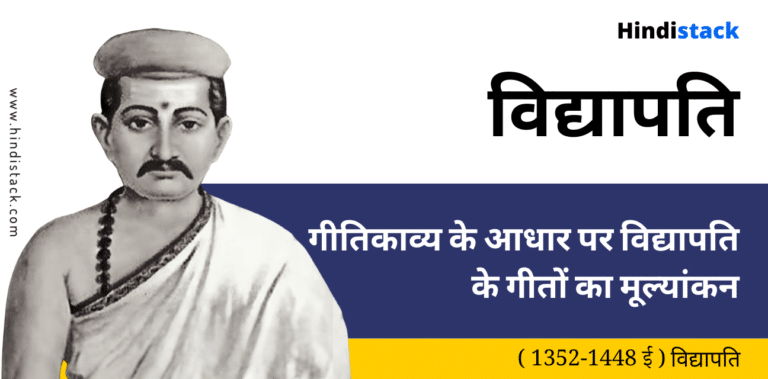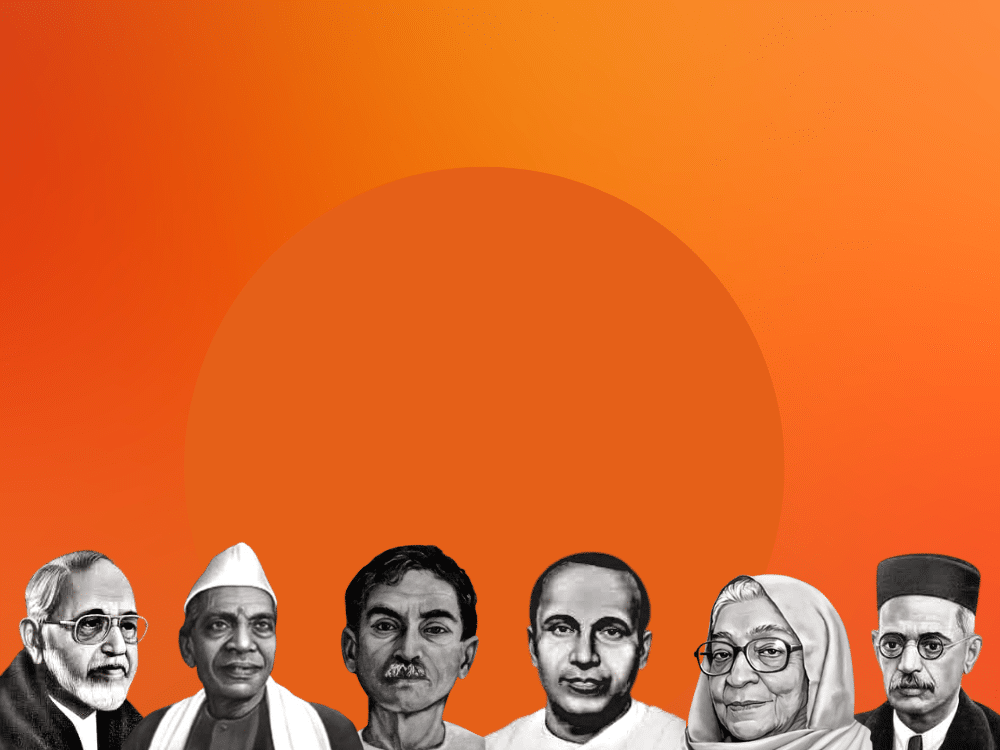हिंदी साहित्य का काल-विभाजन एवं विभिन्न कालखण्डों का उपयुक्त नामकरण साहित्य के इतिहास की महत्वपूर्ण समस्या है। इस संबंध में सबसे पहला प्रश्न यह है कि काल-विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? काल-विभाजन की आवश्यकता काव्य-रचना का काल क्रम की दृष्टि से अवलोकन करना आवश्यक है। मिश्र बंधुओं ने काल-विभाजन के उद्देश्य पर इस प्रकार दृष्टि डाली है कि
“काल-विभाजन इतिहास के प्रासाद की दीवारें हैं। काल-विभाजन द्वारा यह जाना जा सकता है कि कल , कैसे और किधर लोगों की विचारधारा प्रवर्तित हुई।”
काल-विभाजन का आधार यह एक विचारणीय प्रश्न हो सकता है कि साहित्य के काल-विभाजन का आधार क्या हो? हिंदी साहित्य में इतिहास-लेखन की प्रवृत्ति का प्रायः अभाव ही रहा है। अधिकांश साहित्यकारों एवं कवियों ने अपने विषय में अधिक नहीं लिखा, अतः इसका रूप प्रायः स्थूल एवं अनुमान पर आधारित है। आधुनिक युग में अवश्य ही साहित्यकारों का रुझान इस और बढ़ा है। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास भी अपने-अपने स्तर पर किया है।
हिन्दी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण का प्रश्न हिन्दी भाषा की उत्पत्ति से जुड़ा है। मोटे तौर पर हिन्दी भाषा की उत्पत्ति 1000 ई० के आसपास से माना जाती है। इससे पूर्व की भाषा अपभ्रंश थी, जिसका समय 500 ई० से 1000 ई० तक माना जाता है, किन्तु अपभ्रंश से हिन्दी तक के सफर में लगभग 7वीं – 8वीं शताब्दी के मध्य में एक नई भाषा उभरकर सामने आई, जिसे उत्तर अपभ्रंश या अवहट्ठ कहा गया। दरअसल यह अवहट्ठ भाषा ही हिन्दी की आरम्भिक रूप मानी गई, जिसे हम ‘पुरानी हिन्दी’ कहते हैं।
यह समय सिद्धों के उद्भव का समय था, जो बौद्ध धर्म से उत्पन्न बताए जाते हैं। ये धार्मिक चेतना को आधार बनाकर साहित्य सृजन कर रहे थे। बौद्ध धर्म लगभग 500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आया, जो तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद दो शाखाओं – हीनयान और महायान में विभाजित हो गया।
हीनयान शाखा के लोग बुद्ध को प्रतीक के रूप में मानते थे और उनके आदर्शों पर चलते थे। वहीं महायान शाखा के अनुयायी बुद्ध को देवता या भगवान मानते थे और उनकी मूर्ति की पूजा करते थे। वहीं 7वीं – 9वीं शताब्दी के आते-आते बौद्ध धर्म के नियमों में और परिवर्तन आया। परिणामस्वरूप शाखा या सम्प्रदाय का उदय हुआ। इस सम्प्रदाय के लोग बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानने लगे और उदय हुआ एक ऐसी पद्धति का, जिसमें तंत्र-मंत्र पर बल दिया जाने लगा। वज्रयान शाखा के लोग गुह्य साधना का प्रयोग करते हुए पंचमकार (मद्य, मांस, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा) की साधना करने लगे।
यह भी पढ़ें: हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल अपने ग्रन्थ ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ में लिखते हैं कि ‘बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान सम्प्रदाय के देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम रूप में सीमा को पहुँचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे।”[1]
वज्रयान शाखा के इन साधुओं ने जनता के मध्य अपने मत का प्रचार-प्रसार करने के लिए साहित्य को माध्यम बनाया, जिनकी भाषा थी- अपभ्रंश मिश्रित देशभाषा अर्थात् उत्तर अपभ्रंश अथवा अवहट्ठ, जिसे पुरानी हिन्दी की संज्ञा दी गई। इन्हीं सिद्धों के साहित्य से ही हिन्दी साहित्य का आरम्भ माना जाता है। हालांकि आचार्य शुक्ल तो सिद्ध और नाथ योगियों की रचनाओं को आदिकालीन साहित्य से बाहर मानने के पक्ष में हैं।
वे लिखते हैं कि
“उनकी रचनाएँ तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्म निग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अन्तर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की साम्प्रदायिक शिक्षा मात्र है, जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः वे शुद्ध साहित्य के अन्तर्गत नहीं आतीं।”[2]
किन्तु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल के इस तर्क से सहमत नहीं होते। वे कहते हैं कि यदि सिद्धों- नाथों के साहित्य को आदिकालीन साहित्य से बाहर कर दिया जाएगा, जिसका पर्याप्त प्रभाव परवर्ती साहित्य पर स्पष्ट दिखाई पडता है, तब तो कबीर जैसे सन्त कवियों का साहित्य भी हिन्दी तब साहित्य से बाहर हो जाएगा। अतः सिद्धों-नाथों की रचनाओं को आदिकालीन साहित्य में रखा जाना आवश्यक है।
चूँकि सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद है, जिन्हें राहुल सांकृत्यायन ने हिन्दी का पहला कवि भी माना है। जिन्होंने ‘सरहपाद’ अथवा ‘सरहपा’ का समय 769 ई० के आसपास मौना है, जो पालशासक हधर्मपाल (770 ई० – 820 ई०) के समकालीन थे। तब तो हिन्दी साहित्य का आरम्भ ईसा की आठवीं शताब्दी के मध्य से माना जाना चाहिए।
जहाँ तक सुकुल आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा सेना की हिन्दी साहित्य का आरम्भ ईसा की 8वीं शताब्दी का मध्य न मानकर 993 ई० अर्थात् विक्रम संवत् 1050 मानने का है, तो वे अपने ग्रन्थ ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ के आदिकाल खण्ड के आरम्भ में लिखते हैं कि
“प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिन्दी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे ‘गाथा’ कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही ‘दोहा’ या ‘दूहा’ कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिन्दी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की साम्प्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की सातवीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है।”[3]
इस प्रकार आदिकाल का आरम्भ 8वीं शताब्दी के मध्य से मानने में कोई संदेह ही नहीं रह जाता। अब सवाल इस बात का है कि हिन्दी साहित्य का काल-विभाजन एवं नामकरण किस आधार पर किया जाना चाहिए, तो इसका जवाब यही है कि साहित्य के काल-निर्धारण एवं उसके नामकरण में विशेष रूप से साहित्यिक प्रवृत्तियाँ उत्तरदायी मानी जाती हैं किन्तु यह भी स्मरण रहे कि किसी भी काल विशेष में अनेक साहित्यिक प्रवृत्तियाँ पाई जा सकती हैं; जैसे – आदिकाल में धार्मिकता के साथ-साथ श्रृंगारिकता, वीरता आदि अनेक प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती है। दरअसल समाज में होने वाली समस्त गतिविधियों का सीधा असर तत्कालीन साहित्य पर पड़ता है और उस साहित्य में निहित प्रवृत्तियाँ ही हमें काल-निर्धारण और नामकरण की ओर प्रेरित करती हैं।
वहीं काल विशेष में उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियों में भी उतार-चढ़ाव होता है। जो प्रवृत्तियों उत्पन्न होती हैं, उनमें कुछ समय पश्चात् परिवर्तन आना आरम्भ हो जाता है। भले ही इस परिवर्तन के आदि और अन्त का समय निर्धारित न हो। अपने ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ ग्रन्थ में डॉ० नगेन्द्र ने लिखा है,
“जनजीवन की प्रवृत्तियों व रीति-आदर्शों की समानता के आधार पर सामाजिक इतिहास का काल विभाजन होता है और राजनीतिक परिस्थितियों की समानता राजनीतिक इतिहास के काल विभाजन का आधार बनती है। इसी प्रकार साहित्यिक प्रवृत्तियों और रीति-आदर्शों का साम्य-वैषम्य ही साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का आधार हो सकता है।”[4]
हिन्दी साहित्य का काल विभाजन करने हेतु इतिहासकारो द्वारा साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार के अतिरिक्त अन्य आधारों का भी सहारा भी लिया गया है। ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर आदिकाल, मध्यकाल, संक्रान्तिकाल, आधुनिक काल आदि के रूप में, शासक और उनके शासनकाल के आधार पर एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा काल आदि के रूप में, लोकनायक और उनके प्रभावकाल के आधार पर चैतन्य काल, गाँधी युग आदि के रूप में, साहित्यिक नेता एवं उनके प्रभाव काल के अनुसार रवीन्द्र युग, भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग आदि के रूप में और राष्ट्रीय सामाजिक अपवा सांस्कृतिक आन्दोलन के आधार पर भक्तिकाल, पुनर्जागरण काल, सुधारकाल, युद्धोत्तरकाल, स्वातंत्र्योत्तर काल आदि के रूप में कालखण्डों के नाम दिए जा सकते हैं, किन्तु इन सभी आधारों में से साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन अधिक तर्कसंगत माना जा सकता है।
जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि समाज व राष्ट्र में होने वाली गतिनिधियों का प्रभाव वहाँ के साहित्य पर पड़ता है और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ उन गतिविधियों के प्रभाव के कारण परिवर्तित होती रहती हैं। इस प्रकार ‘हिन्दी साहित्य का काल विभाजन’ साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर करने में कोई संदेह ही नहीं रह जाता।
हिन्दी साहित्य के काल निर्धारण के समानान्तर ही एक और बड़ी समस्या थी – नामकरण की, कि आखिर किस कालाखण्ड को क्या नाम दिया जाए? अर्थात् किसी कालखण्ड को कोई नाम देने का आधार क्या होना चाहिए? दरअसल साहित्य के किसी कालखण्ड को कोई नाम देने के लिए उस समय की मूल साहित्यिक चेतना उत्तरदायी मानी जाती है अर्थात् यदि हम शासक और उसके शासनकाल के आधार पर कालखण्ड का नामकरण करते हैं, तो यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि क्या उस शासक के व्यक्तित्व का प्रभाव तत्कालीन साहित्य पर दृष्टिगोचर होता है अथवा नहीं?
इसी प्रकार लोकनायकों, साहित्यिकारों तथा राष्ट्रीय, सामाजिक व सांस्कृतिक आन्दोलनों का प्रभाव भी उस समय के साहित्य पर पड़ना चाहिए। कहने का आशय यह है कि साहित्य के किसी काण्ड के नामकरण का मूल आधार तत्कालीन साहित्यिक चेतना का प्रतिफलन होता है, जिसका माध्यम सामान्यतः उस समय की साहित्यिक प्रवृत्ति ही हो सकती है।
अब सवाल इस बात का है कि हिन्दी साहित्य के कालखण्डों की समय-सीमा और उनके नाम कैसे तय किए जाएँ? इनके लिए इतिहासकारों के अलग-अलग मत हैं।पहले मतानुसार, सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य का विभाजन चार युगों अथवा कालखण्डों में किया गया है –
- आदिकाल
- भक्तिकाल
- रीतिकाल
- आधुनिक काल
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और उनके अनुसरण पर नागरी प्रचारणी सभा के इतिहासों में इसी को ग्रहण किया गया है। दूसरे मत के आधार पर हिन्दी साहित्य को केवल तीन कालखण्डों में ही विभक्त किया गया है –
- आदिकाल
- मध्यकाल
- आधुनिक काल
इस मत को डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त द्वारा अपने ‘हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास’ (प्रकाशन वर्ष 1965 ई०) तथा ‘भारतीय हिन्दी परिषद के इतिहास’ में स्वीकार किया गया है। हिन्दी साहित्य रसज्ञ एवं प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी ने भी इसी मत का अनुमोदन किया है।
वहीं आधुनिक काल को कई उपकालों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं–
- भारतेन्दु युग (पुनर्जागरण काल )
- द्विवेदी युग ( जागरण- सुधार काल)
- छायावाद युग
- प्रगतिवाद गुग
- प्रयोगवाद पुग
- नई कविता युग (नवलेखन युग)
मोटे तौर पर वर्ष 1850 ई० से 1900 ई० तक के काल को ‘भारतेन्दु युग’ और 1900 ई० से 1918 ई० तक के काल को ‘द्विवेदी युग’ नाम दिया गया है। 1918 ई० से हिन्दी साहित्य में काव्य की जो धारा बही, उसे ‘छायावाद युग’ नाम दिया गया। हिन्दी साहित्य में छायावाद का विकास आचार्य महावीर प्रसादयुगीन कविता के उपरान्त बंग्ला काव्य के प्रभाव स्वरूप हिन्दी में प्रकट हुआ। ‘छायावाद’ नाम सर्वप्रथम मुकुटधर पाण्डेय ने दिया, जिसकी समय सीमा 1918 ई० से 1936 ई० तक मानी जाती है। 1936 ई० में प्रेमचन्द के नेतृत्व में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई।
उसके बाद साहित्य में प्रगतिवादी काव्य की सर्जना हुई और 1936 ई० से 1943 ई० के काल को ‘प्रगतिवाद युग’ नाम से अभिहित किया गया। 1943 ई० के बाद काव्य के क्षेत्र में एक संक्रान्ति का दौर चला, जिसके अन्तर्गत प्रयोगवाद नामक नई काव्यधारा का उदय हुआ, जिसकी समय सीमा 1943 ई० से 1953 ई० तक मानी जाती है। 1953 ई० से डॉ० जगदीश गुप्त द्वारा सम्पादित ‘नई कविता’ पत्रिका के माध्यम से नई काव्यधारा का जन्म हुआ, जिसका नामकरण इसी पत्रिका के नाम पर ‘नई कविता युग’ (नवलेखन युग) पड़ा, जिसकी अजस्र धारा आज भी अनवरत बह रही है।
हिन्दी साहित्य का काल-विभाजन एवं नामकरण
अब हम क्रमश: हिन्दी साहित्य के उन इतिहासकारों तथा उनके द्वारा तय किए गए कालखण्डों की समयसीमा एवं नामकरण के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे, जिन्होंने इस क्षेत्र में प्रयास किया है। इस क्रम में सबसे पहला नाम आता है सर जॉर्ज ग्रियर्सन का । उनके द्वारा रचित ‘द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ़ हिन्दुस्तान’ में हिन्दी साहित्य का काल-विभाजन एवं नामकरण इस प्रकार है –
1. जार्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन –
जार्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ मे ग्यारह अध्यायो का वर्णन किया है जो निम्न लिखित है – (1) चारण काल (2) 15 वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण (3) मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता (4) ब्रज का कृष्ण सम्प्रदाय (5) मुगल दरबार (6) तुलसीदास (7) रीतिकाव्य (8) तुलसीदास के परवर्ती कवि (9) 18वीं शताब्दी (10) कंपनी के शासन मे हिन्दुस्तान (11) विक्टोरिया के शासन मे हिन्दुस्तान
ग्रियर्सन ने हिन्दी साहित्य का काल विभाजन केवल साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर किया है, लेकिन कालखण्डों के नामकरण हेतु उन्होंने अनेक आधारों का सहारा लिया है। ग्रियर्सन ने सबसे पहले हिन्दी साहित्य के आरम्भिक कालको ‘चारण काल’ कहा है, जिसके अन्तर्गत उन्होंने 9 कवियों का उल्लेख किया हैं, जिनके नाम हैं. पुष्य कवि, खुमाण सिंह, केदार, कुमार पाल, अनन्यदास, चन्द्र, जगनिक, जोधराज और शारङ्गधर।
गियर्सन के बाद हिंदी साहित्य का काल-विभाजन एवं नामकरण के क्षेत्र में लेखनी चलाने वाले साहित्येतिहासकारों में मिश्र बंधुओं का नाम आता है। मिश्र बंधुओं ने सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य को पाँच खण्डों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार हैं –
2. मिश्र बन्धुओं का काल विभाजन–
‘मिश्र बन्धु विनोद’ निम्न काल विभाजन वर्णित है-
1. आरम्भिक काल –
(क) पूर्व आरम्भिक काल (सं0 700 से 1343 वि0) (ख) उत्तर आरम्भिक काल (सं0 1344 से 1444 वि0)
2. माध्यमिक काल –
(क) पूर्व माध्यमिक काल (सं0 1445 से 1560 वि0) (ख) प्रौढ माध्यमिक काल (सं0 1561 से 1680 वि0)
3. अलंकृत काल –
(क) पूर्व अलंकृत काल (सं0 1681 से 1790 वि0) (ख) उत्तर अलंकृत काल (सं0 1791 से 1889 वि0)
4. परिवर्तन काल – (सं0 1890 से 1925 वि0)
5. वर्तमान काल – (सं0 1926 वि0 से आज तक)
इन विद्वानों ने कालों के वर्गीकरण में युगीन प्रवृत्तियों की उपेक्षा की। इसी कारण से इनके द्वारा किए गए काल विभाजन एवं नामकरण को अधिक मान्यता नहीं मिली। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने युगीन प्रवृत्तियों को आधार बनाकर अपने ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ ग्रन्थ में सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य को चार कालों में बाँटा है –
3. आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन –
आचार्य शुक्ल ने ‘हिंदी साहित्य का इतिहास’ (1929 ई0) मे काल विभाजन मे दोहरा नामकरण करते हुए उसका प्रारुप निम्न प्रकार दिया है। 1. आदिकाल (वीरगाथा काल) 1050 – 1375 वि0 सं0 2. पूर्व मध्यकाल (भक्तिकाल) 1375 – 1700 वि0 सं0 3. उत्तर मध्यकाल (रीतिकाल) 1700 – 1900 वि0 सं0 4. आधुनिक काल (गद्य काल) 1900 – 1984 वि0 सं0
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के आरम्भिक काल, जिसे उन्होंने ‘वीरगाथा काल’ नाम दिया है, की समय सीमा को 1050 विक्रमी से 1375 विक्रमी तक मानकर उसे यथार्थ सीमा के निकट ला दिया है। साथ ही अन्य विद्वानों द्वारा किए गए अनेक भेदों को सीमित करके सम्पूर्ण साहित्य को सिर्फ चार कालों में विभाजित कर दिया, जिससे अध्ययन की दृष्टि से काल-विभाजन न केवल सरल एवं सुबोध हो गया बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी निहित है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रन्थ ‘हिन्दी साहित्य : उद्भव और विकास’ में हिन्दी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार किया है –
- आदिकाल (1000 ई० – 1400 ई०)
- पूर्व मध्यकाल (1400 ई० – 1700 ई०)
- उत्तर मध्यकाल (1700 ई० – 1900 ई०)
- आधुनिक काल (1900 ई ० – अब तक)
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किए गए काल-विभाजन की मुख्य विशेषता यह है कि उन्होंने पूरी शताब्दी को काल-विभाजन का आधार माना। साथ ही उन्होंने विक्रम संवत् के स्थान पर ईसवी सन् का प्रयोग किया। आचार्य द्विवेदी ने आदिकाल को आचार्य शुक्ल के द्वारा दिए गए नाम ‘वीरगाथा काल’ का विरोध किया है। कारण कि जिन रचनाओं के आधार पर आचार्य शुक्ल प वीरगाथा काल नाम देते हैं, वे रचनाएँ हैं –
- विजयपाल रासो
- हम्मीर रासो
- कीर्तिलता
- कीर्तिपताका
- खुमान रासो
- बीसलदेव रासो
- पृथ्वीराज रासो
- जयमयंक जसचंद्रिका
- जयचंद प्रकाश
- परमाल रासो (आल्हा खण्ड)
- खुसरो की पहेलियाँ
- विद्यापति पदावली
इनमें से काफी रचनाएँ उपलब्ध ही नहीं हैं और कुछ रचनाओं की प्रामाणिकता पर संदेह है। साथ ही वीरगाथा नाम देने से वीर रस से इतर रचनाएँ; जैसे- हमीर रासो, विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो के पद हैं, ये सभी फुटकल रचनाओं में चली जाती हैं। इसलिए आचार्य द्विवेदी ने प्रारम्भिक काल को वीरगाथा काल के स्थान पर आदिकाल नाम दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने आचार्य शुक्ल के काल विभाजन की पद्धति को स्वीकार किया है।
4. डॉ० रामकुमार वर्मा का काल विभाजन –
डॉ० रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ ‘हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास’ (1938) मे निम्न प्रकार से काल विभाजन किया है- 1. सान्धिकाल (सं0 750 से 1000 वि0) 2. चारणकाल (सं0 1000 से 1375 वि0) 3. भक्तिकाल (सं0 1375 से 1700 वि0) 4. रीतिकाल (सं0 1700 से 1900 वि0) 5. आधुनिक काल (सं0 1900 वि0 से अब तक)
डॉ० रामकुमार वर्मा ने अपने ग्रन्थ ‘हिन्दी साहित्य का आलोचना इतिहास’ में वीरगाथा काल के स्थान पर चारण काल नाम दिया है। साथ ही उन्होंने सम्वत् 750 से 1000 विक्रमी तक की अवधि को जोड़ते हुए एक नया नाम दिया है, जिसे ‘संधिकाल’ कहा गया। डॉ० रामकुमार वर्मा ने हिन्दी साहित्य का आरम्भ विक्रम संवत् 1050 न मानकर सम्वत् 750 से माना है। इसके बाद के कालों का निर्धारण आचार्य शुक्ल के काल-निर्धारण के आधार पर किया है।
5. हजारी प्रसाद व्दिवेदी का काल विभाजन –
इस प्रकार है – 1. आदिकाल (1000 ई0 से 1400 ई0) 2. पूर्व मध्यकाल (1400 ई0 1700 ई0) 3. उत्तर मध्यकाल (1700 ई0 1900 ई0) 4. आधुनिक काल (1900 ई0 से अब तक)
6. डॉ० गणपति चन्द्रगुप्त का काल विभाजन –
इस प्रकार है – 1. प्रारम्भिक काल (1184 ई0 से 1350 ई0) 2. मध्यकाल – (i) पूर्व मध्यकाल (1350 ई0 से 1500 ई0) (ii) उत्तर मध्यकाल (1500 ई0 से 1857 ई0) 3. आधुनिक काल (1857ई0 से 1965 ई0)डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त में हिन्दी साहित्य के काल-विभाजन एवं नामकरण करने में वैज्ञानिक तरीका अपनाया तो है, किन्तु अनेक इतिहासकारों द्वारा इसे भी तर्क संगत नहीं माना गया है।
हिन्दी साहित्य के काल-विभाजन एवं नामकरण में डॉ० नगेन्द्र का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता हैं। उन्होंने ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ नाम ग्रन्थ का सम्पादन किया है, जिसमें उन्होंने काल-विभाजन एवं नामकरण इस प्रकार दर्शाया है –
- आदिकाल (ईसवी की सातवीं शताब्दी के मध्य से – चौदहवीं शताब्दी के मध्य तक)
- भक्तिकाल (चौदहवीं शताब्दी के मध्य से सत्रहवीं शताब्दी के मध्य तक)
- रीतिकाल (सत्रहवीं शताब्दी के मध्य से उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक)
- आधुनिक काल (उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से अब तक) –
हिन्दी साहित्यकारों के द्वारा डॉ० नगेन्द्र द्वारा किए गए द्वारा ‘काल-विभाजन और नामकरण’ को अन्य विद्वानों की अपेक्षाकृत अधिक मान्यता प्रदान की गई है और काफी हद तक यह वैज्ञानिक भी है।
उपर्युक्त विद्वानों के वर्गीकरण पर गौर करें तो ‘काल विभाजन एवं नामकरण’ के जितने भी प्रयास किए गए, उन सबमें गुण-दोष विद्यमान हैं, फिर भी तुलनात्मक रूप से आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉ० नगेन्द्र द्वारा किए गए ‘काल विभाजन एवं नामकरण’ को अधिक मान्यता प्रदान की गई।
- भारतेन्दु युग (पुनर्जागरण काल) – 1850 ई० से 1900 ई० तक
- द्विवेदी युग (जागरण-सुधार काल) – 1900 ई० से 1918 ई० तक
- छायावाद युग – 1918 ई० से 1936 ई० तक
- प्रगतिवाद युग – 1936 ई० से 1943 ई० तक
- प्रयोगवाद युग – 1943 ई० से 1955 ई० तक
- नई कविता (नवलेखन) – 1955 ई० – अब तक
निष्कर्ष – हिन्दी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण
एक बात विशेष रूप से हमारे समक्ष आती है, वह यह कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल शताब्दियों में चल थे। दो सौ साल, तीन सौ साल या इससे भी अधिक समय का निर्धारण किया गया, किन्तु जैसे ही आधुनिक काल आया, तो इस काल में परिवर्तन बहुत जल्दी-जल्दी होने लगे। इस काल में शताब्दियों की जगह दशकों में कालखण्डों को विभाजित किया जाने लगा, जिसकी मुख्य वजहें थीं – प्रकाशन की सुविधा सुलभ होना, पत्रकारिता का प्रचार-प्रसार बढ़ने लगना, साहित्यकारों को लेखन के क्षेत्र अनेक सुविधाओं का मिलना, राजनीतिक स्तर पर भी परिवर्तन शीघ्र-शीघ्र होना, जिनका सीधा असर साहित्य पर पड़ने लगा और ये ही वजहें थीं कि भारतेन्दु युग लगभग 50 वर्ष, द्विवेदी युग लगभग 20 वर्ष, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तो इनसे भी कम समय में सिमट कर रह गए। सन् 1955 से नवलेखन काल का आगमन हुआ, जो अब तक चल रहा है। हालांकि इस बीच नया लेखक वर्ग कई बार युग-परिवर्तन की घोषणा चुका है, परन्तु साहित्यिक प्रवृत्तियों के अत्यधिक सामीप्य के कारण इस विषय में अभी कुछ भी कहना आसान नहीं होगा।
संदर्भ –
- हिंदी साहित्य का इतिहास/ लेखक – आचार्य रामचंद्र शुक्ल/ संस्करण 2021/ प्रकाशक- प्रभात पेपरबैक्स, नई दिल्ली/ पृष्ठ 23
- हिंदी साहित्य का इतिहास/ लेखक – आचार्य रामचंद्र शुक्ल/ संस्करण 2021/ प्रकाशक- प्रभात पेपरबैक्स, नई दिल्ली/ पृष्ठ 32
- हिंदी साहित्य का इतिहास/ लेखक – आचार्य रामचंद्र शुक्ल/ संस्करण 2021/ प्रकाशक- प्रभात पेपरबैक्स, नई दिल्ली/ पृष्ठ 19
- हिंदी साहित्य का इतिहास/ संपादक – डॉ० नगेंद्र/ प्रकाशन – मयूर पेपरबैक्स, नई दिल्ली/ संस्करण 2016/ पृष्ठ 35
हिंदी साहित्य का काल-विभाजन और नामकरण से सबंधित प्रश्नों को हल करें :
- हिन्दी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ‘ब्रज का कृष्ण काव्य’ नामकरण किस साहित्येतिहासकार ने सुझाया है ?
हिन्दी साहित्य के किस काल को ‘स्वर्णयुग’ कहा जाता है ?
हिंदी साहित्य का आदिकाल’ के लेखक कौन हैं?
पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ‘उत्तर मध्यकाल’ को किस नाम से अभिहित किया है ?