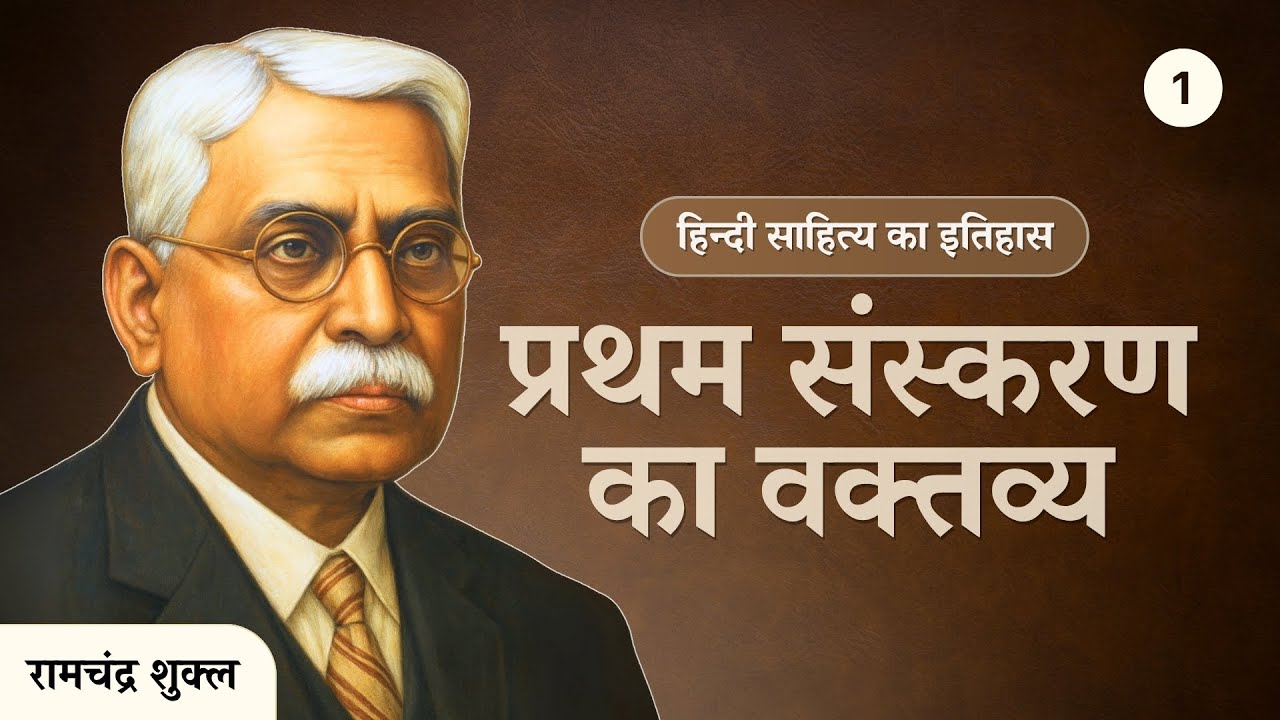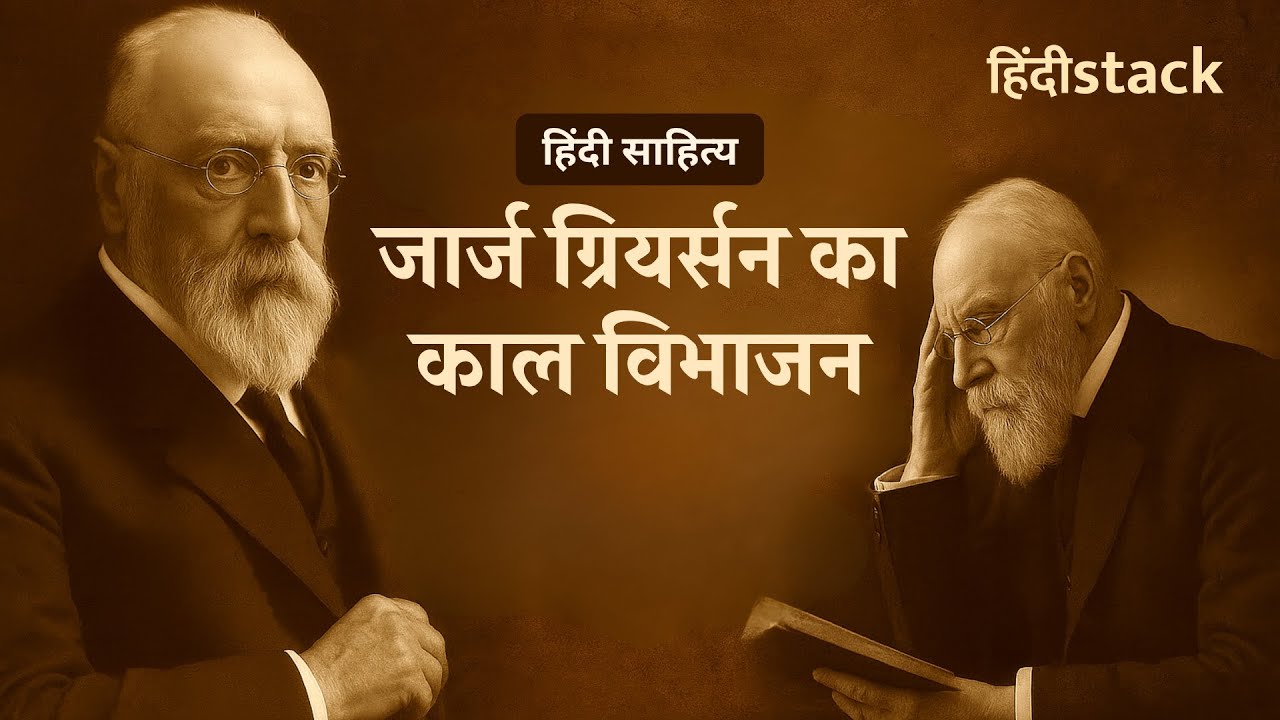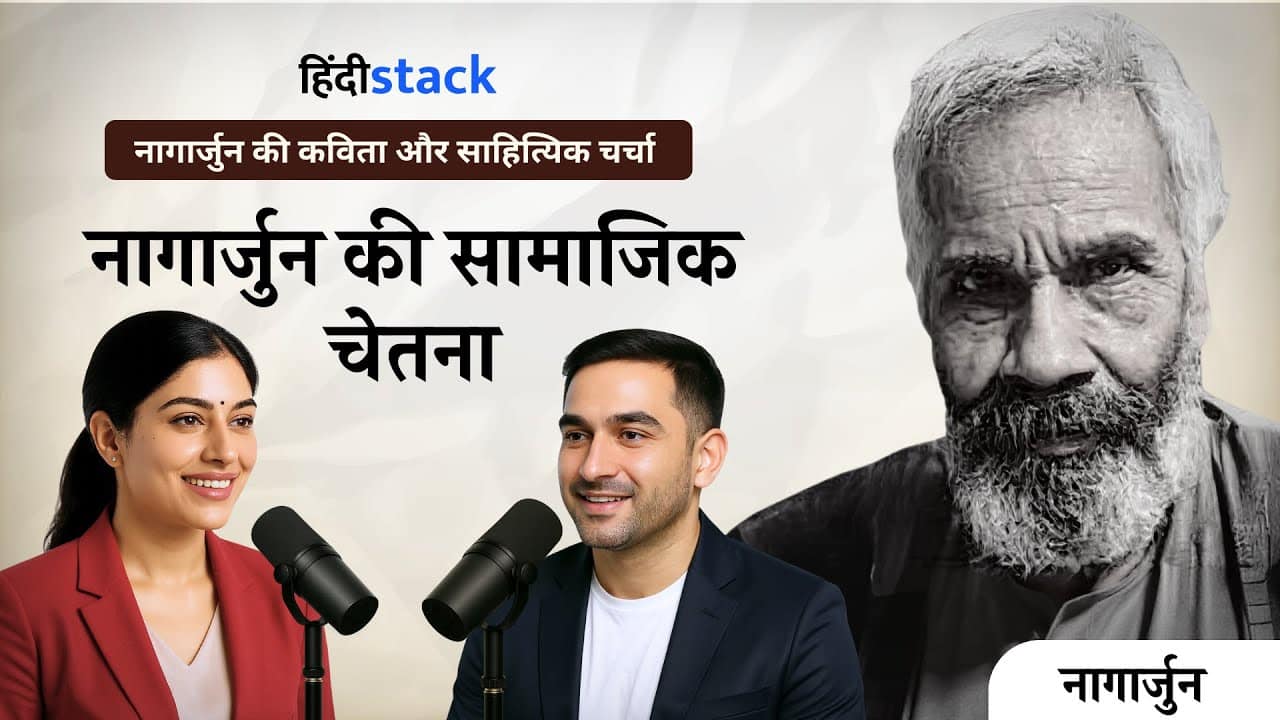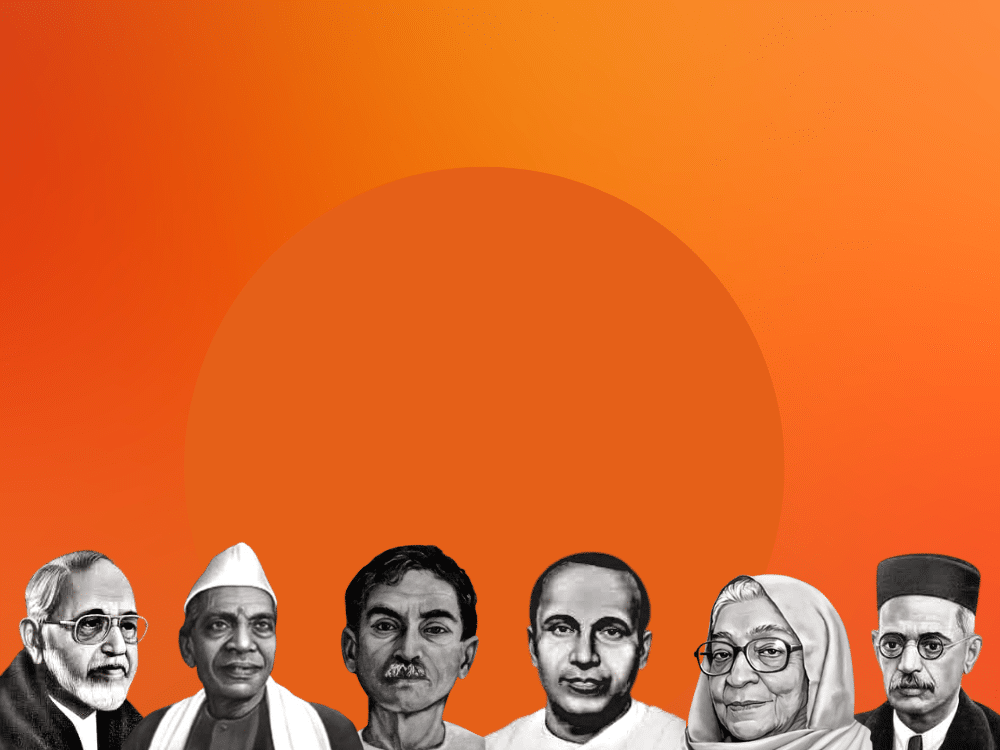यह स्टडी गाइड, आदिकाल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों और विशेषताओं (Aadikal ki Visheshta) को ध्यान में रख कर आपके लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें आदिकाल की परिभाषा, कालक्रम, प्रमुख धाराएँ और विभिन्न आलोचनात्मक दृष्टिकोण शामिल हैं।
I. आदिकाल का सामान्य परिचय
- कालक्रम: आदिकाल का समय संवत् 1050 से 1375 (10वीं से 14वीं शताब्दी) के बीच माना जाता है।
- उद्भव और विकास: यह हिंदी साहित्य के उद्भव और प्रारंभिक विकास का काल है।
- आलोचक कथन:
आचार्य रामचंद्र शुक्ल: आदिकाल में किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय कठिन है; इसमें धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएँ मिलती हैं।हजारी प्रसाद द्विवेदी: यह काल हिंदी भाषा की आधारभूमि है, जिसमें परिनिष्ठित अपभ्रंश से आगे बढ़ी हुई लोकभाषा का रूप दिखाई देता है।
- प्रमुख साहित्यिक धाराएँ:धर्माश्रित काव्य: सिद्ध, नाथ और जैन परम्पराएँ।
- वीरगाथात्मक या रासो साहित्य: राजपूत दरबारों से जुड़ी चारण परम्परा।
- लोकाश्रित धारा: लोकाभिरुचि के गीत, संदेश काव्य, और लोकरंजक रचनाएँ (विद्यापति, अमीर खुसरो)।
II. आदिकाल की प्रमुख विशेषताएँ और प्रवृत्तियाँ
- वीर रस की प्रधानता:
- आदिकालीन काव्य का प्रमुख सौंदर्य-तत्व वीरता, जो राजसत्ता, सरहदी संघर्ष और गौरव-युद्धों के वर्णन से केंद्र में रहा।
- छोटे राज्यों की राजनीति, आपसी युद्ध और विदेशी आक्रमणों ने वीरता को सांस्कृतिक मूल्य बनाया। चारण कवि दरबार और रणभूमि दोनों के साक्षी थे।
- आलोचक कथन: डॉ. श्यामसुंदर दास ने वीरगाथाओं के युद्ध-वर्णन को इतना सजीव माना है कि उनके सामने उत्तरवर्ती कवियों के अनेक युद्ध-चित्र फीके लगते हैं।
- यह केवल युद्ध का वर्णन नहीं, बल्कि सामूहिक साहस, आन-बान और रक्षा-संस्कृति का काव्यकरण है।
- युद्धों का सजीव चित्रण:
- रण का दृश्यात्मक, श्रव्य और मनोवैज्ञानिक प्रभाव सहित चित्रण।
- चारण कवि आश्रयदाताओं के साथ युद्ध में होते थे, जिससे कविताओं में प्रत्यक्ष अनुभूति झलकती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने वाला वर्ग आवश्यक था।
- युद्ध-वर्णन योद्धा-मन के उठान और अवसाद का भी ग्राफ प्रस्तुत करते हैं।
- ऐतिहासिकता का अभाव और प्रामाणिकता का प्रश्न:
- चरित-आधारित रचनाएँ होते हुए भी तिथियों, क्रम और तथ्य-प्रमाण में असंगतियाँ।
- दरबारी आश्रय, यशोगान और कल्पना-प्रधान शैली के कारण तथ्य-शुद्धता गौण हुई। चारण कवियों ने ऐतिहासिक तथ्यों की अवहेलना की।
- आलोचक कथन: आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो परम्परा की अप्रमाणिकताओं की ओर स्पष्ट संकेत किया है, यहाँ तक कि पृथ्वीराज रासो को “जाली” बताया है।
- आदिकालीन ग्रंथ इतिहास के स्रोत तो हैं, पर उन्हें परखते समय काव्य-उत्प्रेक्षा और दरबारी आशय को ध्यान में रखना चाहिए।
- जन-जीवन के चित्रण का अभाव:
- दरबारी फोकस के कारण साधारण जन का जीवन अपेक्षाकृत अनुपस्थित।
- चारण कवि का प्राथमिक दायित्व आश्रयदाता का यशोगान था।
- यह अभाव आगे लोकाश्रित धारा और भक्तिकाल में पूरित होता है।
- डिंगल-पिंगल भाषा-शैली का प्रयोग:
- वीरता और कठोर भाव के लिए डिंगल (राजस्थानी-अपभ्रंश मिश्रित) तथा कोमल, श्रृंगारिक और गीतात्मक भाव के लिए पिंगल (ब्रज-अपभ्रंश मिश्रित) का प्रयोग।
- भाषा-विन्यास और भाव-विन्यास का तालमेल आदिकाल की बड़ी तकनीकी उपलब्धि है।
- रासो शब्द और रासक शैली:
- रासो – चरितप्रधान, गेय-नाट्यात्मक प्रसंगविधान; रासक – ताल-लययुक्त वार्तालाप-निरूपण वाला गेय रूप।
- रासो-रूप ने कथा, गायन और शौर्य-गाथा को एक मंच दिया, जिससे उसकी सामाजिक पहुँच बनी।
- संकुचित राष्ट्रीय भावना:
- व्यापक राष्ट्र-बोध के स्थान पर राज्य-विशेष के गौरव की भावना।
- छोटे-छोटे राज्यों की राजनीति, सीमित क्षितिज। कवि अपने आश्रयदाता की विजय को ‘देश-गौरव’ मानते थे, पर ‘देश’ की अवधारणा अक्सर राज्य-सीमित थी।
- आदिकाल का राष्ट्र-बोध बाद के कालों में विकसित होता है।
- आश्रयदाताओं की प्रशंसा और अतिशयोक्ति:
- दान-वीरता, शौर्य, ऐश्वर्य का बढ़ा-चढ़ाकर चित्रण।
- आश्रय-संबंध और चारण-नीति का सामाजिक-सांस्कृतिक अनुबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, राजा के पराक्रम का चित्रण करने वाले चारण ही सम्मान पाते थे।
- अतिशयोक्ति यहाँ काव्यालंकार भी है और दरबारी अपेक्षा की पूर्ति भी।
- विविध छंदों का प्रयोग:
- दोहा, गाथा, रोला, तोटक, उल्लाला, कुण्डलिया, आर्या, आल्हा आदि का बहुविध प्रयोग।
- आलोचक कथन: चंदबरदाई को छंद-सम्राट और पृथ्वीराज रासो को “छन्दों का अजायबघर” कहा जाता है।
- छंद-व्यवस्था कार्यात्मक है – जिस भाव की जरूरत, उसी का लयबद्ध वाहक छंद।
- वीर और श्रृंगार रस का समन्वय:
- वीर-प्रधान प्रवृत्ति के भीतर श्रृंगार की सह-उपस्थिति।
- अनेक युद्ध प्रसंग विवाह-प्रतियोग, दुल्हन-हरण, स्वयंबर आदि से जुड़े थे, इसलिए श्रृंगार का प्रवेश स्वाभाविक था।
- युद्ध केवल विध्वंस नहीं, बल्कि वर-वधू, वंश, राज्य-गौरव की सांस्कृतिक कड़ी भी है।
- अलंकारों का स्वाभाविक समावेश:
- उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष, अनुप्रास आदि का सहज, प्रसंगोचित प्रयोग।
- रीतिकाल की तरह अलंकार-प्रदर्शन लक्ष्य नहीं था, बल्कि भाव-चित्र और ध्वनि-प्रधानता के लिए प्रयुक्त होते थे
- प्रबंध काव्य और मुक्तक – दोनों रूपों की उपस्थिति:
- चरितप्रधान, अध्यायबद्ध प्रबंध (जैसे पृथ्वीराज रासो) के साथ-साथ स्वतंत्र, गीतिधर्मी मुक्तक रचनाएँ (जैसे संदेश रासक)।
- रचनात्मक बहुरंगी बनावट आदिकाल की एक विशिष्ट शक्ति है।
- प्रकृति-चित्रण:
- आलंबन और उद्दीपन – दोनों रूपों में प्रकृति का उपयोग।
- युद्ध-यात्रा, नगर, किलों के संदर्भ में नदियाँ, पर्वत, भोर-सांझ का दृश्य-काव्य।
- प्रकृति यहाँ रस-वर्धक है, आत्म-केन्द्रित नहीं।
- धर्माश्रित साहित्य – सिद्ध, नाथ और जैन परम्परा:
- निर्गुण-उन्मुख वज्रयान-सिद्ध बानियाँ, हठयोग और साधना-प्रवचन केन्द्रित नाथ-पंथ, और शास्त्र-व्याकरण-चरितकाव्य में जैन परम्परा।
- धर्माश्रित काव्य ने भाषा को जन-जीवन की ओर खींचा, भावभूमि को अंतर्मुख किया और रूढ़ियों पर वैचारिक प्रहार की परम्परा दी।
- लोकाश्रित धारा – संदेश रासक, विद्यापति, अमीर खुसरो:
- लोकप्रिय, गेय, श्रृंगार-रस और दूत-काव्य परम्परा से पोषित रचनाएँ, साथ ही लोकोन्मुख सूझ-बूझ।
- लोकाश्रित साहित्य ने भाषा को सहज, कर्णप्रिय और जनोन्मुख बनाया, जो आगे हिंदी की व्यापकता का बीज बना।
- हिंदी कविता का प्रारंभिक स्वरूप:
- संस्कृत-प्राकृत-अपभ्रंश के बाद लोक-माध्यम के रूप में हिंदी पद्य का संगठित आरम्भ।
- हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ‘पद्य-भाषा में तद्भव का एकछत्र राज्य’ को हिंदी की मानकीकृत काव्य-भाषा की भूमि तैयार करने वाला बताया।
- आदिकाल वह द्वार है जिससे हिंदी अपनी लोक-ध्वनि के साथ काव्य-भूमि पर प्रवेश करती है।
III. आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य
- आचार्य रामचंद्र शुक्ल: आदिकाल में प्रवृत्ति-विशेष का निश्चय कठिन मानते हुए धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सभी प्रकार की रचनाओं की उपस्थिति स्वीकार करते हैं। रासो-पुस्तकों की प्रमाणिकता पर संयत सन्देह और पाठ-समालोचना की आवश्यकता पर बल देते हैं।
- हजारी प्रसाद द्विवेदी: 10वीं से 14वीं शती के बीच पद्य की भाषा को तद्भव-प्रधान और लोकभाषा का उदीयमान रूप मानते हैं, जिसे हिंदी की आरंभभूमि कहते हैं। वे धर्माश्रित परम्पराओं को निर्गुण भक्ति की भाषा तैयार करने वाला मानते हैं।
- डॉ. श्यामसुंदर दास: युद्ध-वर्णन की सजीवता को अद्वितीय मानते हैं, जिसकी तुलना में उत्तरवर्ती कवियों के वर्णन फीके लगते हैं।
IV. निष्कर्ष
आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास में एक संक्रमणकालीन और अंतर्विरोधों का युग है। यहाँ युद्ध और शौर्य की गाथाओं के साथ-साथ धर्म, दर्शन और लोकजीवन की अनुगूँज भी मिलती है। यद्यपि इसकी ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता पर प्रश्नचिह्न लगे हैं, फिर भी यह काल हिंदी भाषा और साहित्य की प्रारंभिक पृष्ठभूमि तैयार करता है, जिसमें आगे आने वाले भक्तिकाल और रीतिकाल के बीज अंतर्निहित हैं। यह अपनी विविध शैलियों, भाषिक प्रयोगों और भावगत समन्वय के कारण महत्वपूर्ण है, जो हिंदी साहित्य की नींव को मजबूती देता है।
आदिकाल: लघु-उत्तरीय प्रश्नोत्तरी
निर्देश: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दें।
- आदिकाल का सामान्य कालक्रम क्या है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ कैसी थीं?
- हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को हिंदी भाषा की आधारभूमि क्यों माना है?
- आदिकालीन साहित्य की तीन प्रमुख धाराएँ कौन-कौन सी हैं? संक्षेप में बताएँ।
- वीर रस की प्रधानता आदिकाल की एक प्रमुख विशेषता क्यों मानी जाती है? इसके पीछे क्या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य था?
- युद्धों के सजीव चित्रण के लिए चारण कवियों की क्या भूमिका थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी का इस संदर्भ में क्या मत है?
- आदिकालीन रासो ग्रंथों में ऐतिहासिकता के अभाव और प्रामाणिकता के प्रश्न पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की टिप्पणी क्या है?
- डिंगल और पिंगल भाषा-शैलियों में क्या अंतर है और इनका प्रयोग किन भावों की अभिव्यक्ति के लिए होता था?
- आदिकाल की “संकुचित राष्ट्रीय भावना” से क्या अभिप्राय है?
- आश्रयदाताओं की प्रशंसा आदिकालीन कवियों की एक प्रमुख विशेषता क्यों थी?
- धर्माश्रित साहित्य के अंतर्गत सिद्ध, नाथ और जैन परम्पराओं का संक्षिप्त परिचय दें और इनका महत्व बताएँ।
आदिकाल: लघु-उत्तरीय प्रश्नोत्तरी – उत्तर कुंजी
- आदिकाल का सामान्य कालक्रम संवत् 1050 से 1375 (10वीं से 14वीं शताब्दी) है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, इस काल में रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है, बल्कि धर्म, नीति, श्रृंगार और वीर सब प्रकार की रचनाएँ मिलती हैं।
- हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को हिंदी भाषा की आधारभूमि माना है क्योंकि इस काल में लोकभाषा में लिखित साहित्य उपलब्ध हुआ, जिसमें परिनिष्ठित अपभ्रंश से कुछ आगे बढ़ी हुई भाषा का रूप दिखाई देता है। यह भाषा ही आगे चलकर हिंदी का आधार बनी।
- आदिकालीन साहित्य की तीन प्रमुख धाराएँ हैं: धर्माश्रित काव्य (सिद्ध, नाथ और जैन परम्पराएँ), वीरगाथात्मक या रासो साहित्य (राजपूत दरबारों से जुड़ी चारण परम्परा), और लोकाश्रित धारा (लोकाभिरुचि के गीत, संदेश काव्य और लोकरंजक रचनाएँ)।
- वीर रस की प्रधानता आदिकाल की प्रमुख विशेषता थी क्योंकि छोटे-छोटे राज्यों की राजनीति, आपसी युद्ध और तुर्क-अफगान आक्रमणों की आहट ने वीरता को सांस्कृतिक मूल्य बनाया। चारण कवि दरबार और रणभूमि दोनों के साक्षी थे, जिससे उनकी रचनाओं में वीरता का केंद्रीय स्थान रहा।
- चारण कवि अक्सर अपने आश्रयदाता के साथ युद्ध में होते थे, जिससे उनकी कविताओं में रण का दृश्यात्मक, श्रव्य और मनोवैज्ञानिक प्रभाव सहित सजीव चित्रण मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, “देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी 1 वर्ग आवश्यक हो गया था”।
- आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन रासो ग्रंथों की प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त किया है, उनका आशय इतिहास-लेखन नहीं, साहित्यिक प्रवृत्ति का मूल्यांकन था। उन्होंने पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथों को “जाली” तक कहा है, क्योंकि इनमें तिथियों और तथ्यों में अत्यधिक असंगतियाँ मिलती हैं।
- डिंगल भाषा (राजस्थानी-अपभ्रंश मिश्रित) का प्रयोग वीरता और कठोर भावों की अभिव्यक्ति के लिए होता था, जबकि पिंगल भाषा (ब्रज-अपभ्रंश मिश्रित) का प्रयोग कोमल, श्रृंगारिक और गीतात्मक भावों के लिए किया जाता था। यह भाव और भाषा के तालमेल की एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि थी।
- आदिकालीन साहित्य में “संकुचित राष्ट्रीय भावना” से अभिप्राय है कि उस समय व्यापक राष्ट्र-बोध के स्थान पर केवल राज्य-विशेष के गौरव की भावना प्रबल थी। कवि अपने आश्रयदाता की विजय को ‘देश-गौरव’ मानते थे, लेकिन ‘देश’ की अवधारणा अक्सर केवल सौ-पचास गाँवों तक सीमित राज्य तक ही थी।
- आश्रयदाताओं की प्रशंसा आदिकालीन कवियों की प्रमुख विशेषता थी क्योंकि वे दरबारी कवि थे और अपने राजाओं का यशोगान करने से उन्हें मान तथा धन की प्राप्ति होती थी। इसलिए, वे अपने आश्रयदाताओं की दान-वीरता, शौर्य और ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण करते थे।
- धर्माश्रित साहित्य में सिद्ध (निर्गुण-उन्मुख वज्रयान), नाथ (हठयोग, रूढ़ि-विरोध) और जैन (शास्त्र-व्याकरण-चरितकाव्य) परम्पराएँ शामिल थीं। इनका महत्व यह है कि इन्होंने लोकभाषा में साधना, रूढ़ि-विरोध और दार्शनिक सूक्तियाँ प्रस्तुत कर जन-जीवन से जुड़ने वाली भाषा और अंतर्मुखी भावभूमि का विकास किया।
आदिकाल: निबंधात्मक प्रश्न
- आदिकालीन साहित्य की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों का विस्तार से वर्णन करें, तथा यह समझाएँ कि ये प्रवृत्तियाँ तत्कालीन सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों से किस प्रकार प्रभावित थीं।
- आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के आदिकाल संबंधी विचारों की तुलनात्मक विवेचना करें। इन दोनों विद्वानों के दृष्टिकोणों में समानताएँ और भिन्नताएँ क्या हैं?
- आदिकालीन साहित्य में ऐतिहासिकता का अभाव और प्रामाणिकता का प्रश्न क्यों उठता है? इस संदर्भ में रासो ग्रंथों की भूमिका और आलोचकों के मतों का उल्लेख करें।
- डिंगल और पिंगल भाषा-शैलियों का आदिकालीन काव्य में क्या महत्व है? उदाहरणों सहित समझाएँ कि ये शैलियाँ किस प्रकार भावों की अभिव्यक्ति में सहायक थीं।
- आदिकालीन साहित्य में वीर रस और श्रृंगार रस का समन्वय किस प्रकार हुआ है? स्पष्ट करें कि ये दोनों रस एक-दूसरे के पूरक कैसे बन गए, न कि विरोधी।
आदिकाल: शब्दावली (Glossary)
- आदिकाल: हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक काल, जिसे सामान्यतः संवत् 1050 से 1375 (10वीं से 14वीं शताब्दी) के बीच माना जाता है।
- धर्माश्रित काव्य: आदिकाल की वह काव्यधारा जो धर्म से प्रेरित थी, जिसमें सिद्ध, नाथ और जैन परम्पराएँ शामिल हैं।
- वीरगाथात्मक साहित्य: आदिकाल की वह काव्यधारा जिसमें राजपूत राजाओं के शौर्य, युद्धों और यशोगान का वर्णन मिलता है, इसे रासो साहित्य भी कहते हैं।
- लोकाश्रित धारा: आदिकाल की वह काव्यधारा जो जनसामान्य की रुचि पर आधारित थी, जिसमें लोकगीत, संदेश काव्य, पहेलियाँ आदि शामिल हैं (जैसे संदेश रासक, विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो की रचनाएँ)।
- चारण कवि: आदिकालीन दरबारी कवि जो अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करते थे, विशेषकर उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते थे।
- डिंगल भाषा: अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के मिश्रण से बनी एक काव्य-शैली, जिसका प्रयोग आदिकालीन वीर रस प्रधान रचनाओं में होता था, यह कठोर और ओजपूर्ण भावों के लिए उपयुक्त थी।
- पिंगल भाषा: अपभ्रंश और ब्रजभाषा के मिश्रण से बनी एक काव्य-शैली, जिसका प्रयोग आदिकालीन कोमल, श्रृंगारिक और गीतात्मक भावों की अभिव्यक्ति के लिए होता था।
- रासो ग्रंथ: आदिकाल के वे चरित-प्रधान काव्य ग्रंथ जिनमें किसी नायक (प्रायः राजा) के शौर्य, युद्ध और प्रेम प्रसंगों का वर्णन होता था (जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो)।
- रासक शैली: ताल-लययुक्त, गेय और नाट्यात्मक काव्य शैली, जिसमें अक्सर प्रश्नोत्तर या दो व्यक्तियों के वार्तालाप का निरूपण होता था, जो दरबारों और लोक-गायन में लोकप्रिय थी।
- अप्रमाणिकता: आदिकालीन रासो ग्रंथों से संबंधित एक विवादित बिंदु, जहाँ उनकी तिथियों, घटनाओं के क्रम और ऐतिहासिक तथ्यों की सत्यता पर संदेह किया जाता है।
- अतिशयोक्ति: किसी बात का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन करना, आदिकालीन कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में इसका व्यापक प्रयोग होता था।
- प्रबंध काव्य: वह काव्य जिसमें किसी कथा का क्रमबद्ध और विस्तृत वर्णन होता है, जिसमें खंडकाव्य और महाकाव्य शामिल हैं (जैसे पृथ्वीराज रासो)।
- मुक्तक काव्य: वह काव्य रचना जो किसी कथा से बंधी नहीं होती, बल्कि स्वतंत्र पदों या गीतों के रूप में होती है, जिसमें एक ही भाव की प्रधानता होती है (जैसे संदेश रासक)।
- सिद्ध साहित्य: बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित साहित्य, जिसमें सामाजिक कुरीतियों और पाखंडों पर प्रहार किया गया और जनभाषा को माध्यम बनाया गया।
- नाथ साहित्य: हठयोग और साधना-प्रवचन पर केंद्रित साहित्य, जिसमें बाह्य आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध किया गया, परवर्ती निर्गुण भक्ति पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा।
- जैन साहित्य: जैन मुनियों द्वारा रचित धार्मिक साहित्य, जिसमें पौराणिक चरित काव्य, व्याकरण शास्त्र और नीतिपरक रचनाएँ शामिल हैं, जो जनभाषा में लिखे गए थे।
- तद्भव शब्द: वे शब्द जो संस्कृत से विकसित होकर हिंदी में आए हैं, जिनमें उच्चारण और अर्थ में परिवर्तन हुआ है। आदिकाल की पद्य भाषा में इनकी प्रधानता थी।
- आलंबन एवं उद्दीपन: प्रकृति चित्रण के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द। आलंबन वह है जिसका सहारा लेकर भाव उत्पन्न होता है (जैसे नायक-नायिका), और उद्दीपन वह है जो भावों को तीव्र करता है (जैसे प्रकृति का सुंदर दृश्य)।