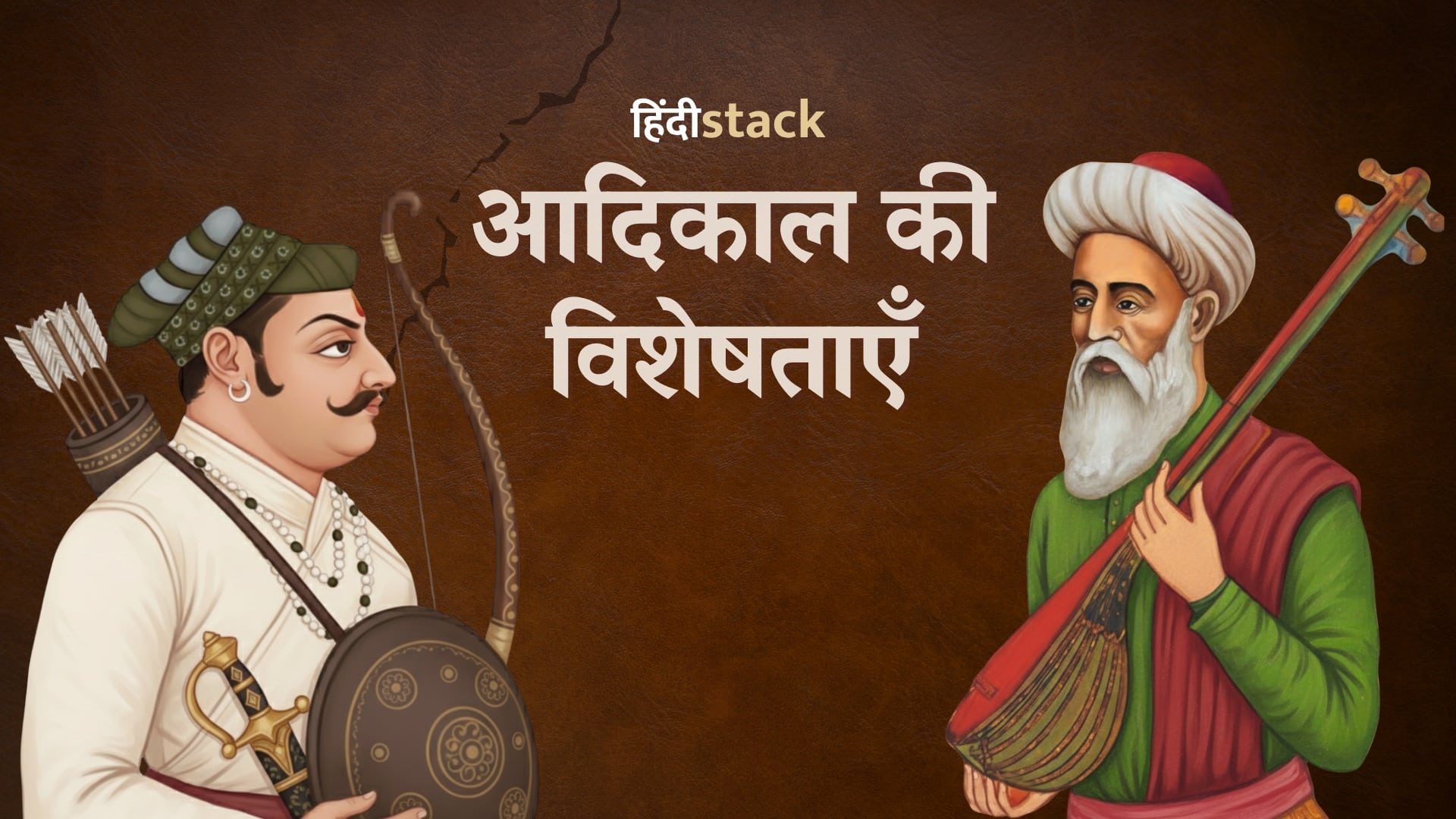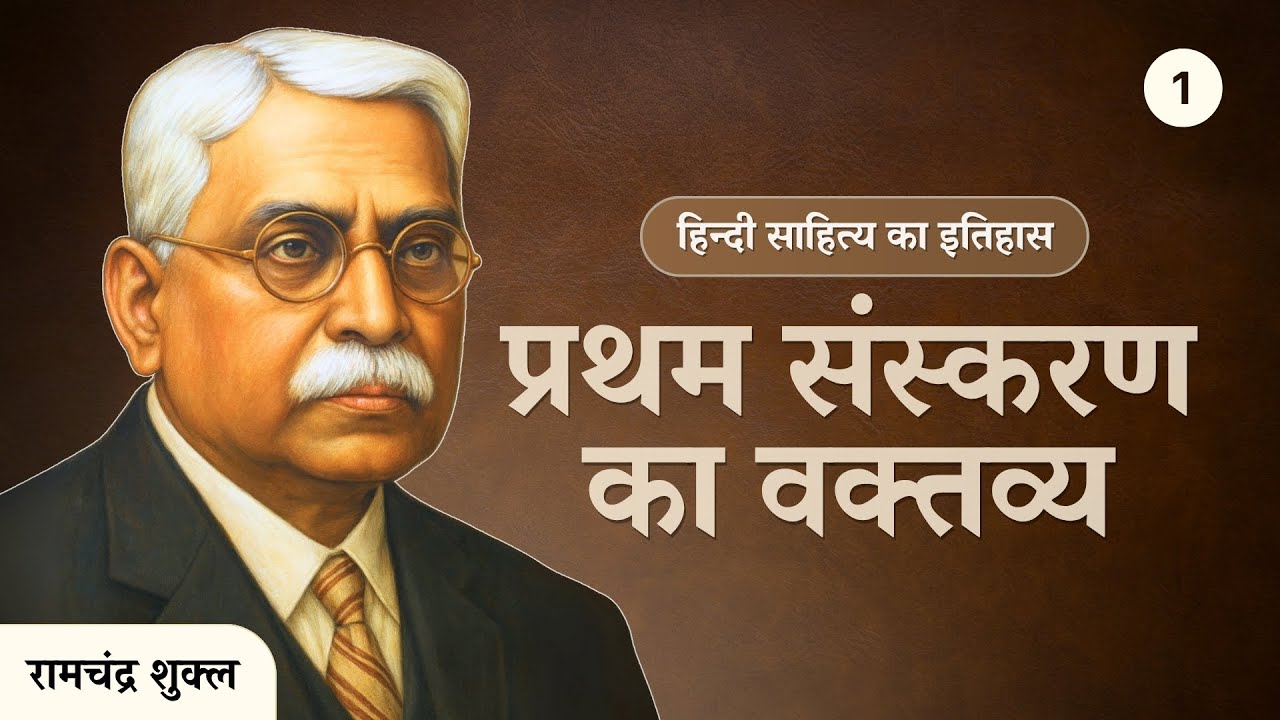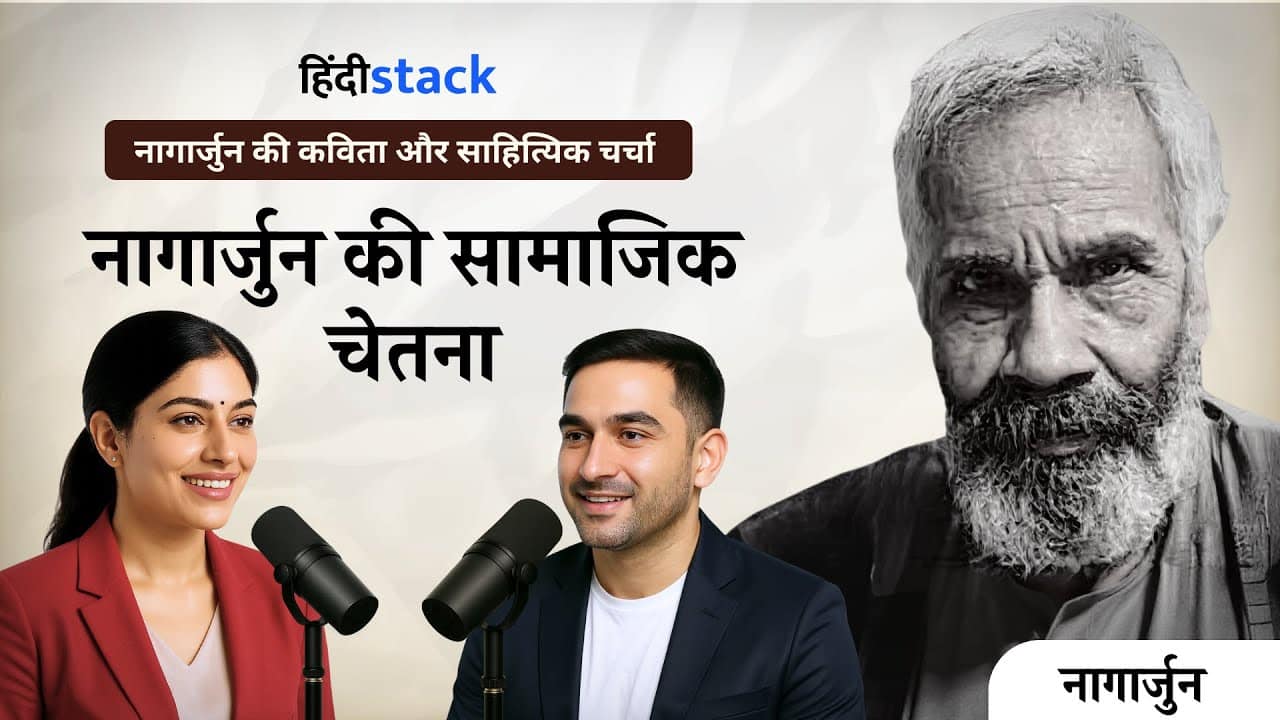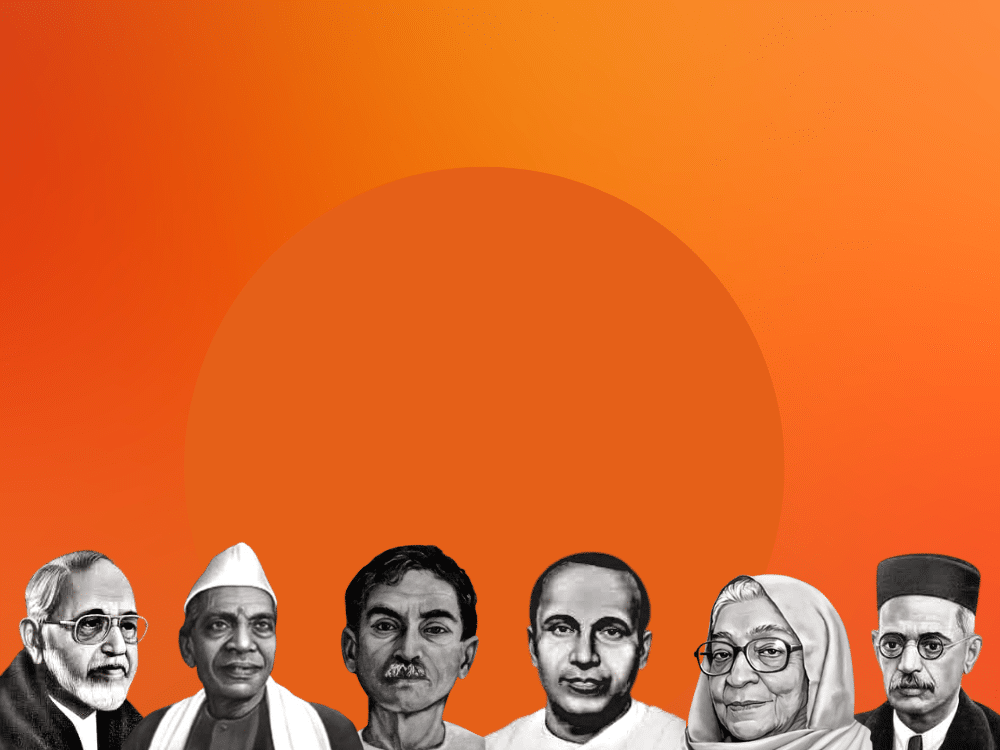हिंदी साहित्य के काल-विभाजन और नामकरण की समस्या: एक विस्तृत अध्ययन
यह अध्ययन मार्गदर्शिका हिंदी साहित्य के काल-विभाजन और नामकरण की समस्या से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं, विवादों और प्रमुख इतिहासकारों के मतों को समझने में आपकी सहायता करेगी।
I. काल-विभाजन और नामकरण की आवश्यकता एवं आधार
- काल-विभाजन की आवश्यकता:काव्य-रचना का कालक्रम की दृष्टि से अवलोकन करना।
- यह जानना कि लोगों की विचारधारा कब, कैसे और किस दिशा में परिवर्तित हुई। (मिश्र बंधुओं के अनुसार, यह इतिहास के प्रासाद की दीवारें हैं)।
- काल-विभाजन का आधार:मुख्यतः साहित्यिक प्रवृत्तियाँ।
- किसी भी कालखंड का नामकरण उस समय की मूल साहित्यिक चेतना के आधार पर होना चाहिए, जो उस समय की साहित्यिक प्रवृत्ति से परिलक्षित होती है।
- अन्य संभावित आधार: ऐतिहासिक कालक्रम, शासक और उनके शासनकाल, लोकनायक, साहित्यिक नेता, राष्ट्रीय/सामाजिक/सांस्कृतिक आंदोलन। हालाँकि, साहित्यिक प्रवृत्तियों को सर्वाधिक तर्कसंगत माना जाता है।
- आधुनिक काल में त्वरित परिवर्तनों के कारण कालखंड दशकों में सिमट गए हैं (प्रकाशन, पत्रकारिता, राजनीतिक परिवर्तन)।
II. हिंदी भाषा और साहित्य का आरंभ
- हिंदी भाषा का उद्भव:मोटे तौर पर 1000 ई० के आसपास मानी जाती है।
- पूर्व की भाषा अपभ्रंश (500 ई० – 1000 ई०)।
- 7वीं-8वीं शताब्दी के मध्य ‘उत्तर अपभ्रंश’ या ‘अवहट्ठ’ नामक नई भाषा उभरी, जिसे ‘पुरानी हिंदी’ कहा गया।
- हिंदी साहित्य का आरंभ:अधिकांश विद्वान सिद्धों के साहित्य से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं।
- सरहपाद: राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है (समय: 769 ई० के आसपास)। इस प्रकार, हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी के मध्य से माना जा सकता है।
- आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत: वे सिद्धों और नाथ योगियों की रचनाओं को शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं मानते क्योंकि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों से उनका संबंध नहीं है। वे हिंदी साहित्य का आरंभ 993 ई० (विक्रम संवत् 1050) से मानते हैं।
- आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रतिवाद: वे शुक्ल के मत से असहमत हैं। उनका तर्क है कि यदि सिद्धों-नाथों के साहित्य को आदिकाल से बाहर किया जाएगा, तो कबीर जैसे संतों का साहित्य भी बाहर हो जाएगा, जबकि उनका परवर्ती साहित्य पर स्पष्ट प्रभाव है।
III. आदिकाल का नामकरण और संबंधित विवाद
- विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल के प्रस्तावित नाम:वीरगाथा काल: आचार्य रामचंद्र शुक्ल (इस नाम पर सर्वाधिक विवाद रहा है)।
- चारण काल: डॉ. रामकुमार वर्मा।
- सिद्ध-सामंत युग: राहुल सांकृत्यायन।
- बीज-वपनकाल: महावीरप्रसाद द्विवेदी।
- संक्रमण काल: डॉ. राम खेलावन।
- आधारकाल: डॉ. मोहन अवस्थी।
- अंतर्विरोधों का काल: कुछ विद्वान।
- आदिकाल: हजारीप्रसाद द्विवेदी, मिश्रबंधु, डॉ. नगेन्द्र (सर्वाधिक स्वीकृत नाम)।
- ‘वीरगाथा काल’ नाम पर विवाद (आचार्य शुक्ल):शुक्ल जी का आधार: तत्कालीन मानव मनोविज्ञान और वीरगाथात्मक प्रवृत्ति। उन्होंने पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो जैसी रचनाओं का उल्लेख किया।
- आपत्तियाँ (हजारी प्रसाद द्विवेदी):जिन रचनाओं के आधार पर यह नाम दिया गया, उनमें से कई अनुपलब्ध या प्रामाणिकता संदिग्ध।
- ‘वीरगाथा काल’ नाम से वीर रस से इतर रचनाएँ (जैसे विद्यापति पदावली, अमीर खुसरो की पहेलियाँ) फुटकल में चली जाती हैं, जो उपयुक्त नहीं है।
- धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक चेतना काव्य में बाधक नहीं होती (रामचरितमानस, महाभारत का उदाहरण)।
- ‘आदिकाल’ नाम की स्वीकार्यता:हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ‘वीरगाथा काल’ के स्थान पर ‘आदिकाल’ नाम दिया, जिसे अधिक उपयुक्त माना गया।
- डॉ. नगेन्द्र भी ‘आदिकाल’ को सबसे उपयुक्त और व्यापक नाम मानते हैं, क्योंकि यह भाषा, भाव, विचारधारा, शिल्प-भेद आदि से संबंधित सभी गुत्थियों को सुलझाता है और आगे के साहित्य के लिए व्यापक पृष्ठभूमि प्रदान करता है।
IV. प्रमुख इतिहासकारों द्वारा काल-विभाजन और नामकरण
- सर जॉर्ज ग्रियर्सन:ग्रंथ: ‘द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ़ हिन्दुस्तान’।कुल 11 अध्याय।
- आरंभिक काल को ‘चारण काल’ कहा (9 कवियों का उल्लेख)।
- साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर काल-विभाजन, लेकिन नामकरण हेतु अनेक आधार।
- मिश्र बंधु:ग्रंथ: ‘मिश्र बंधु विनोद’।
- कुल 5 खंडों में विभाजन (आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल)।
- युगीन प्रवृत्तियों की उपेक्षा के कारण अधिक मान्यता नहीं मिली।
- आचार्य रामचंद्र शुक्ल:ग्रंथ: ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ (1929 ई०)।
- चार कालखंडों में दोहरा नामकरण किया।
- विभाजन:आदिकाल (वीरगाथा काल): 1050 – 1375 वि० सं०
- पूर्व मध्यकाल (भक्तिकाल): 1375 – 1700 वि० सं०
- उत्तर मध्यकाल (रीतिकाल): 1700 – 1900 वि० सं०
- आधुनिक काल (गद्य काल): 1900 – 1984 वि० सं०
- उनके काल-विभाजन को सरल, सुबोध और वैज्ञानिक माना जाता है।
- आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी:ग्रंथ: ‘हिन्दी साहित्य : उद्भव और विकास’।
- शुक्ल जी की पद्धति को स्वीकार किया, लेकिन विक्रम संवत् के स्थान पर ईसवी सन् का प्रयोग किया।
- ‘वीरगाथा काल’ के स्थान पर ‘आदिकाल’ नाम का समर्थन।
- विभाजन:आदिकाल: 1000 ई० – 1400 ई०
- पूर्व मध्यकाल: 1400 ई० – 1700 ई०
- उत्तर मध्यकाल: 1700 ई० – 1900 ई०
- आधुनिक काल: 1900 ई० – अब तक
- डॉ. रामकुमार वर्मा:ग्रंथ: ‘हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास’ (1938)।
- ‘वीरगाथा काल’ के स्थान पर ‘चारण काल’ नाम दिया।
- 750 से 1000 विक्रमी तक की अवधि को ‘संधिकाल’ नाम दिया, हिंदी साहित्य का आरंभ 750 वि० सं० से माना।
- डॉ. गणपतिचंद्र गुप्त:ग्रंथ: ‘हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास’ (1965 ई०)।
- वैज्ञानिक तरीका अपनाया, लेकिन अनेक इतिहासकारों द्वारा तर्कसंगत नहीं माना गया।
- डॉ. नगेन्द्र:ग्रंथ: ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ (संपादक)।
- इनके द्वारा किए गए ‘काल-विभाजन और नामकरण’ को अन्य विद्वानों की अपेक्षा अधिक मान्यता मिली है और यह काफी हद तक वैज्ञानिक है।
- आधुनिक काल को उपकालों में विभाजित किया है (भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगति-प्रयोग काल, नवलेखन काल)।
V. सामान्य स्वीकृत काल-विभाजन (अध्ययन की सुगमता हेतु)
- आदिकाल: 750 ई० – 1350 ई०
- भक्तिकाल: 1350 ई० -1650 ई०
- रीतिकाल: 1650 ई० – 1850 ई०
- आधुनिक काल: 1850 ई० – अब तक (उपकालों सहित)
लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरी (2-3 वाक्य प्रत्येक)
- हिंदी साहित्य के काल-विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
- मिश्र बंधुओं ने काल-विभाजन के उद्देश्य को किस रूप में व्यक्त किया है?
- हिंदी साहित्य के काल-विभाजन का मुख्य आधार क्या माना जाता है?
- हिंदी भाषा की उत्पत्ति मोटे तौर पर कब से मानी जाती है और इसके आरंभिक रूप को क्या कहा गया?
- राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है और उनका समय क्या बताया है?
- आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों और नाथ योगियों की रचनाओं को शुद्ध साहित्य के अंतर्गत क्यों नहीं माना?
- आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य शुक्ल के ‘वीरगाथा काल’ नाम का विरोध क्यों किया?
- डॉ. रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या नाम दिया और एक नया ‘संधिकाल’ किसे कहा?
- आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के काल-विभाजन की मुख्य विशेषता क्या है?
- आधुनिक काल में साहित्यिक कालखंडों के दशकों में सिमट जाने के मुख्य कारण क्या थे?
उत्तर कुंजी
- हिंदी साहित्य के काल-विभाजन की आवश्यकता काव्य-रचना का कालक्रम की दृष्टि से अवलोकन करने और यह जानने के लिए पड़ती है कि लोगों की विचारधारा कब, कैसे और किस दिशा में परिवर्तित हुई। यह साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित रूप से समझने में मदद करता है।
- मिश्र बंधुओं ने काल-विभाजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि “काल-विभाजन इतिहास के प्रासाद की दीवारें हैं।” इसके द्वारा यह जाना जा सकता है कि लोगों की विचारधारा कब, कैसे और किधर प्रवर्तित हुई।
- साहित्य के काल-विभाजन का मुख्य आधार साहित्यिक प्रवृत्तियाँ मानी जाती हैं। किसी भी काल विशेष में पाई जाने वाली प्रमुख साहित्यिक धाराएँ और उनकी समानता-विषमता ही विभाजन का मुख्य आधार बनती हैं।
- हिंदी भाषा की उत्पत्ति मोटे तौर पर 1000 ई० के आसपास मानी जाती है। इससे पूर्व की भाषा अपभ्रंश थी, और 7वीं-8वीं शताब्दी के मध्य उभरी नई भाषा ‘उत्तर अपभ्रंश’ या ‘अवहट्ठ’ को ‘पुरानी हिंदी’ कहा गया।
- राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना है। उन्होंने सरहपाद का समय 769 ई० के आसपास बताया है, जो पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे।
- आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों और नाथ योगियों की रचनाओं को शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं माना क्योंकि वे तांत्रिक विधान, योग साधना और सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। उनके अनुसार, इन रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है।
- आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य शुक्ल के ‘वीरगाथा काल’ नाम का विरोध इसलिए किया क्योंकि जिन रचनाओं के आधार पर शुक्ल जी ने यह नाम दिया, उनमें से कई अनुपलब्ध या प्रामाणिकता में संदिग्ध हैं। साथ ही, यह नाम वीर रस से इतर महत्वपूर्ण रचनाओं (जैसे विद्यापति पदावली, अमीर खुसरो के पद) को मुख्यधारा से बाहर कर देता है।
- डॉ. रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को ‘चारण काल’ नाम दिया है। उन्होंने विक्रम संवत् 750 से 1000 तक की अवधि को जोड़ते हुए एक नया नाम ‘संधिकाल’ भी दिया है, जिसे उन्होंने हिंदी साहित्य के आरंभिक बिंदु के रूप में देखा।
- आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किए गए काल-विभाजन की मुख्य विशेषता यह है कि उन्होंने आचार्य शुक्ल की पद्धति को स्वीकार किया, लेकिन काल-विभाजन का आधार पूरी शताब्दी को माना। साथ ही, उन्होंने विक्रम संवत् के स्थान पर ईसवी सन् का प्रयोग किया।
- आधुनिक काल में साहित्यिक कालखंडों के दशकों में सिमट जाने के मुख्य कारण प्रकाशन की सुविधा का सुलभ होना, पत्रकारिता का प्रचार-प्रसार बढ़ना, साहित्यकारों को लेखन के क्षेत्र में अनेक सुविधाएँ मिलना, और राजनीतिक स्तर पर भी शीघ्र-शीघ्र परिवर्तन होना था, जिनका सीधा असर साहित्य पर पड़ा।
निबंध प्रारूप प्रश्न (उत्तर न दें)
- हिंदी साहित्य के काल-विभाजन की आवश्यकता और उसके विभिन्न आधारों का विस्तार से विश्लेषण करें। साहित्यिक प्रवृत्तियों को सर्वाधिक तर्कसंगत आधार क्यों माना जाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें।
- हिंदी भाषा की उत्पत्ति और हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के निर्धारण से जुड़े विभिन्न विद्वानों के मतभेदों पर प्रकाश डालें। सिद्ध साहित्य की भूमिका और आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचारों की तुलना करें।
- आदिकाल के नामकरण को लेकर हिंदी साहित्य में हुए विभिन्न विवादों की समीक्षा करें। ‘वीरगाथा काल’ और ‘आदिकाल’ नामों के पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों का मूल्यांकन करते हुए बताएं कि ‘आदिकाल’ नाम को क्यों सर्वाधिक मान्यता मिली।
- हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकारों (जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉ. नगेन्द्र) द्वारा किए गए काल-विभाजन और नामकरण की पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें। उनके योगदान और सीमाओं पर चर्चा करें।
- आधुनिक काल में साहित्यिक प्रवृत्तियों में आए तीव्र परिवर्तनों के क्या कारण रहे हैं, और इन परिवर्तनों ने कालखंडों के निर्धारण को किस प्रकार प्रभावित किया है? स्वातंत्र्योत्तर काल तक की विभिन्न साहित्यिक धाराओं का संक्षिप्त परिचय दें।
शब्दावली
- काल-विभाजन (Periodization): साहित्य के इतिहास को अध्ययन की सुविधा और प्रवृत्तियों के आधार पर विभिन्न समय खंडों में बांटना।
- नामकरण (Nomenclature): किसी विशिष्ट साहित्यिक कालखंड को उसकी प्रमुख प्रवृत्ति या विशेषता के आधार पर एक उपयुक्त नाम देना।
- अपभ्रंश (Apabhramsha): मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी मानी जाने वाली एक भाषा अवस्था, जिसका समय लगभग 500 ई० से 1000 ई० तक माना जाता है।
- अवहट्ठ (Avahaṭṭha): उत्तर अपभ्रंश का ही एक रूप, जो 7वीं-8वीं शताब्दी के मध्य उभरी और जिसे हिंदी का आरंभिक या ‘पुरानी हिंदी’ रूप माना जाता है।
- सिद्ध साहित्य (Siddha Literature): 7वीं-8वीं शताब्दी के आसपास बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित सिद्धों द्वारा रचित साहित्य, जो तंत्र-मंत्र और गुह्य साधना पर बल देता था। हिंदी साहित्य का आरंभ इसी से माना जाता है।
- वज्रयान (Vajrayana): बौद्ध धर्म की एक शाखा जो तंत्र-मंत्र, गुह्य साधना और अलौकिक शक्तियों में विश्वास पर आधारित थी।
- पंचमकार (Panchamakara): वज्रयान साधना में प्रयुक्त पांच “म” वर्ण वाले तत्व: मद्य, मांस, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा।
- सरहपाद (Sarahapada): सिद्ध परंपरा के सबसे पुराने कवि, जिन्हें राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है।
- आदिकाल (Adikala): हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सबसे स्वीकृत नाम, जो उसकी प्रारंभिक, विविध और व्यापक प्रवृत्तियों को दर्शाता है।
- वीरगाथा काल (Viragatha Kala): आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के लिए दिया गया नाम, जो मुख्य रूप से वीर रस प्रधान रचनाओं पर आधारित था, लेकिन विवादित रहा।
- चारण काल (Charana Kala): डॉ. रामकुमार वर्मा द्वारा आदिकाल के लिए दिया गया नाम, जो राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करने वाले कवियों (चारणों) की प्रवृत्ति पर आधारित था।
- संधिकाल (Sandhikala): डॉ. रामकुमार वर्मा द्वारा प्रस्तावित एक अतिरिक्त कालखंड (750-1000 वि० सं०), जो हिंदी साहित्य के अपभ्रंश से हिंदी में संक्रमण काल को दर्शाता है।
- भक्तिकाल (Bhakti Kala): हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना जाने वाला कालखंड, जिसमें भक्ति आंदोलन और उससे संबंधित काव्य की प्रधानता रही।
- रीतिकाल (Riti Kala): उत्तर मध्यकाल का नाम, जिसमें लक्षण-ग्रंथों की रचना, श्रृंगारिकता और रीति-परंपरा की प्रमुखता रही।
- आधुनिक काल (Adhunika Kala): हिंदी साहित्य का वर्तमान कालखंड, जिसमें गद्य साहित्य का विकास, राष्ट्रीय चेतना और विभिन्न साहित्यिक आंदोलनों की प्रमुखता रही।
- भारतेन्दु युग (Bharartendu Yuga): आधुनिक काल का एक उपकाल (1850-1900 ई०), जिसे पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, भारतेन्दु हरिश्चंद्र के नाम पर।
- द्विवेदी युग (Dwivedi Yuga): आधुनिक काल का एक उपकाल (1900-1918 ई०), जिसे जागरण-सुधार काल भी कहते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर।
- छायावाद (Chhayavada): आधुनिक काल की एक प्रमुख काव्यधारा (1918-1936 ई०), जिसमें रहस्यवाद, प्रकृति प्रेम और वैयक्तिक भावनाओं की प्रधानता थी।
- प्रगतिवाद (Pragativada): छायावादोत्तर काल की एक काव्यधारा (1936-1943 ई०), जो मार्क्सवादी विचारधारा और सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित थी।
- प्रयोगवाद (Prayogavada): प्रगतिवाद के बाद की काव्यधारा (1943-1953 ई०), जिसमें काव्य में नए प्रयोगों और शिल्पगत नवीनता पर बल दिया गया।
- नई कविता (Nayi Kavita): प्रयोगवाद के बाद की काव्यधारा (1953 ई० से अब तक), जिसमें आधुनिक संवेदनशीलता और यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रमुखता है।
- राहुल सांकृत्यायन (Rahul Sankrityayan): प्रसिद्ध विद्वान और इतिहासकार, जिन्होंने सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना।
- आचार्य रामचंद्र शुक्ल (Acharya Ramchandra Shukla): हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में मील का पत्थर माने जाने वाले ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ के लेखक।
- आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी (Acharya Hazariprasad Dwivedi): महत्वपूर्ण साहित्यकार और आलोचक, जिन्होंने शुक्ल जी के ‘वीरगाथा काल’ नाम का विरोध कर ‘आदिकाल’ नाम का समर्थन किया।
- डॉ. नगेन्द्र (Dr. Nagendra): हिंदी साहित्य के इतिहास के संपादक, जिनके काल-विभाजन को काफी हद तक वैज्ञानिक और मान्य माना जाता है।