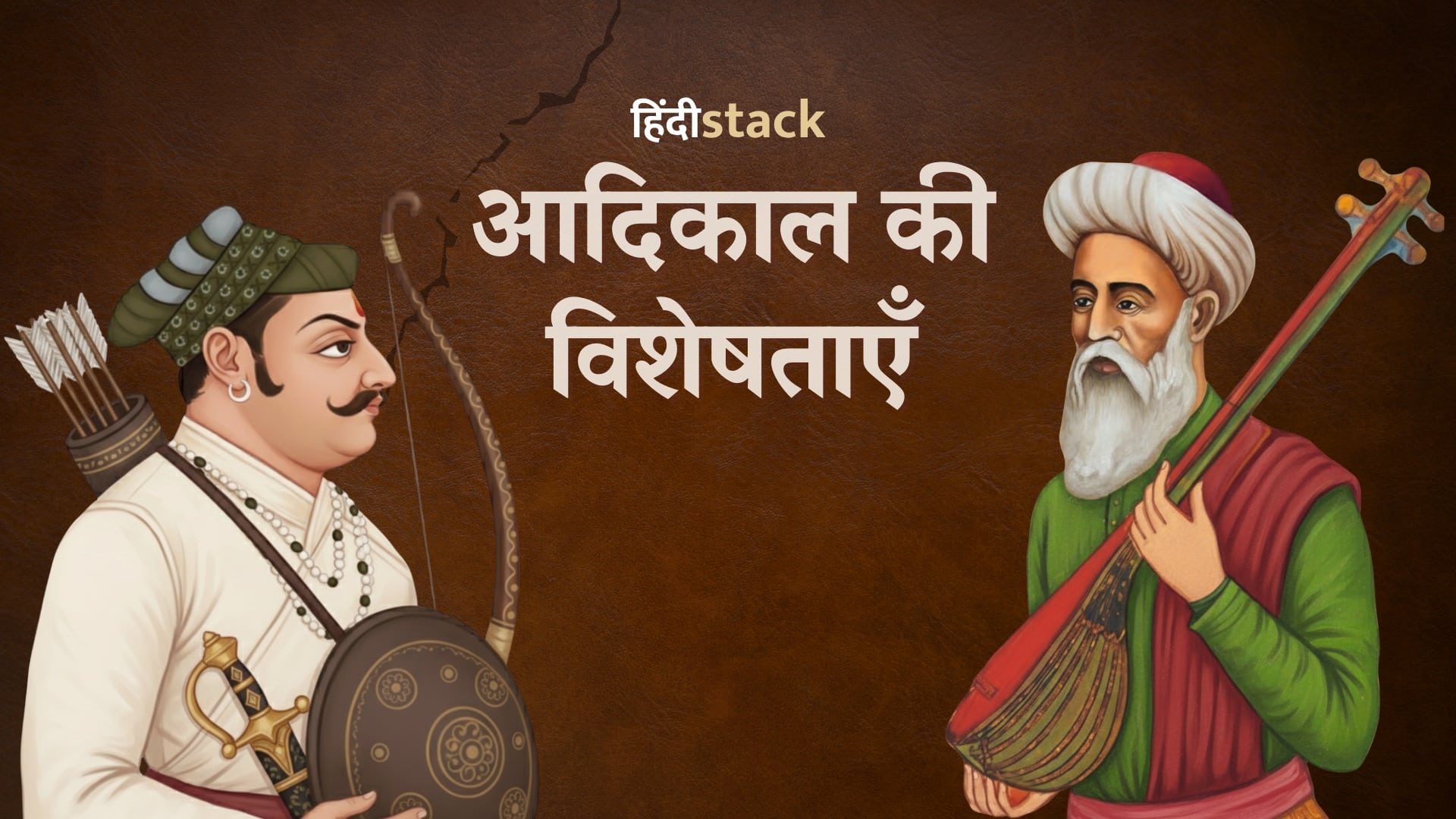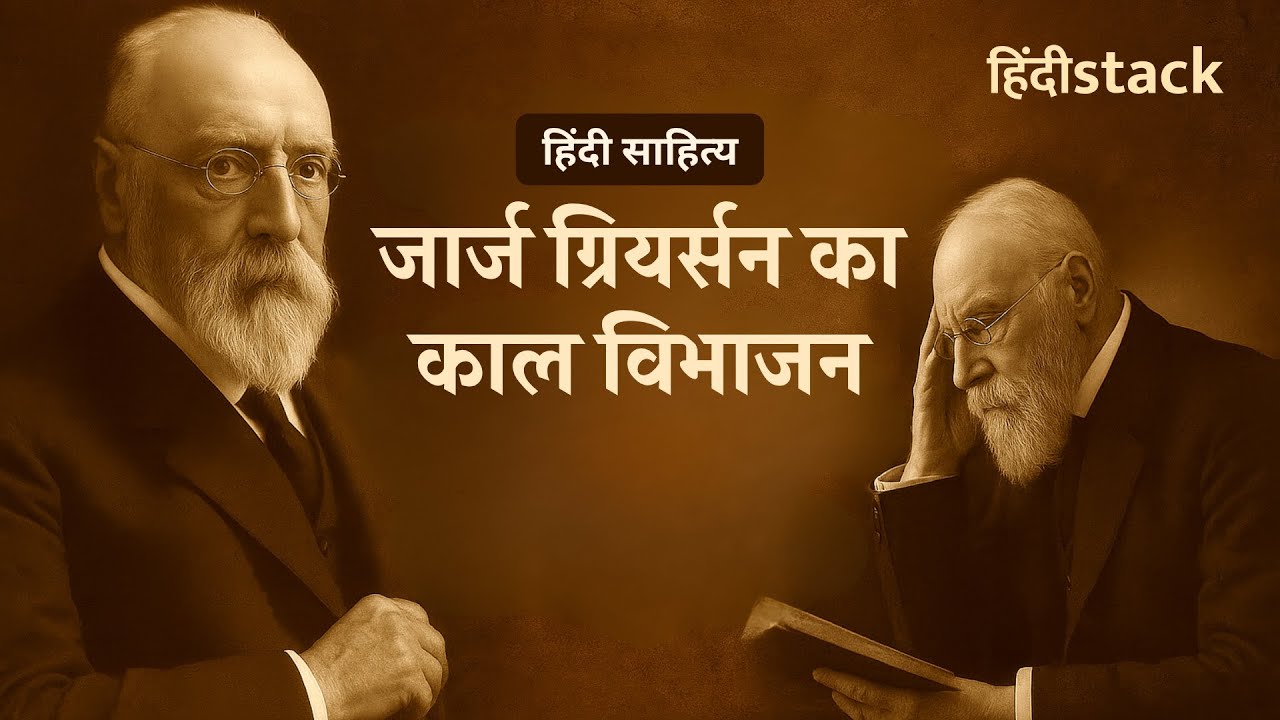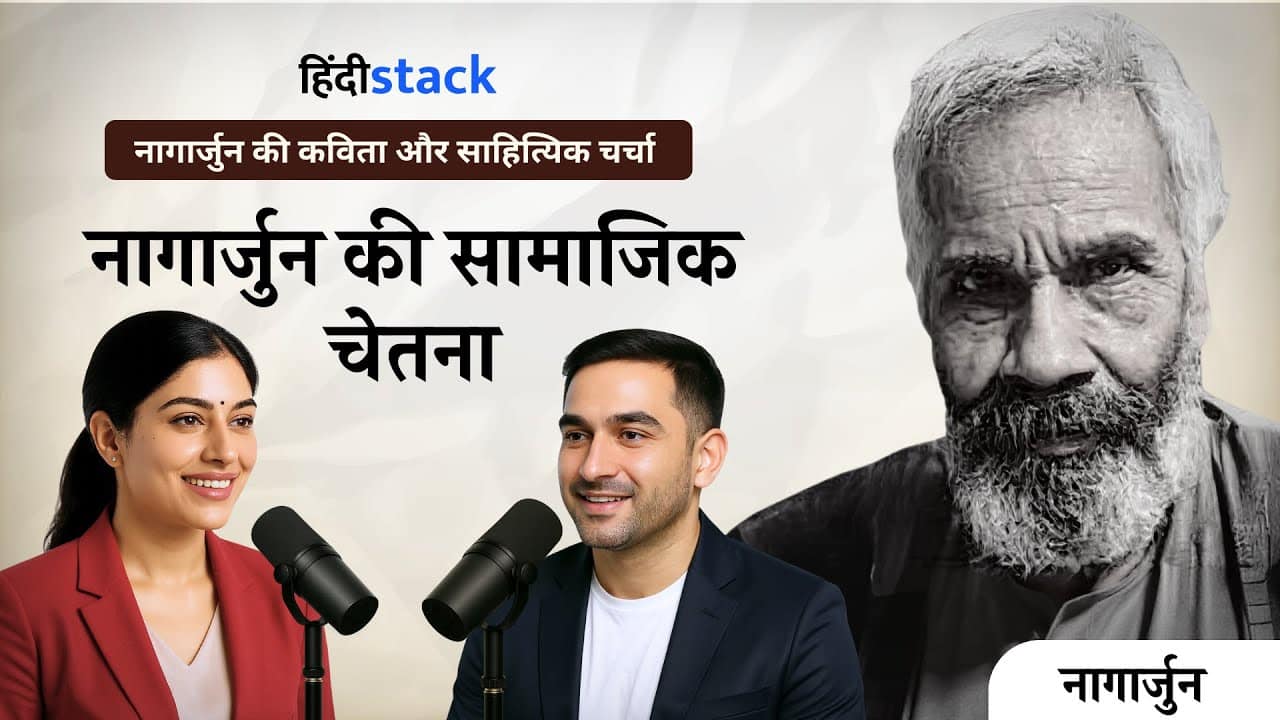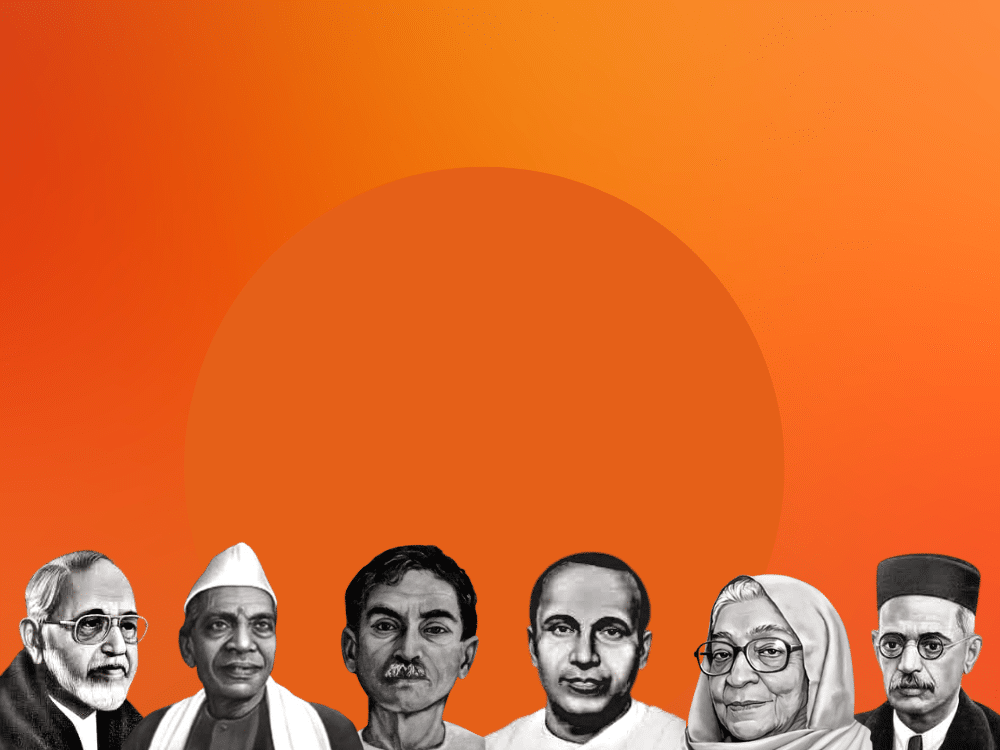यह स्टडी गाइड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कालजयी ग्रंथ ‘हिंदी साहित्य का इतिहास’ की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत करता है, जिसमें इसके महत्व, लेखन प्रक्रिया, पद्धति, प्रमुख अवधारणाओं और योगदान पर प्रकाश डाला गया है। यह प्रदान किए गए विभिन्न स्रोतों “शुक्ल का हिंदी साहित्य: इतिहास और विवेचन”, “शुक्ल का हिंदी साहित्य: इतिहास की दृष्टि”, “शुक्ल का हिन्दी साहित्य इतिहास: एक दृष्टि”, “शुक्ल के हिन्दी साहित्य इतिहास का वक्तव्य”, “हिंदी साहित्य का इतिहास: प्रथम संस्करण का वक्तव्य”, “शुक्ल साहित्य: इतिहास और आलोचना” और “हिंदी साहित्य का विकास: प्रमुख पड़ाव और पात्र” पर आधारित है।
1. ग्रंथ का महत्व और छात्रों के पूर्वाग्रह
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का “हिंदी साहित्य का इतिहास” (प्रकाशन: जनवरी 1929) हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए एक “अत्यंत महत्वपूर्ण” और “अनिवार्य” ग्रंथ है। प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे TGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, NET, KVS) में “कम से कम 10 क्वेश्चन के आसपास” प्रश्न सीधे इसी ग्रंथ से पूछे जाते हैं।
हालांकि, छात्रों में इसे लेकर एक “पूर्वाग्रह” है कि “रामचंद्र शुक्ला को पढ़ना बहुत कठिन है।” यह पूर्वाग्रह अक्सर सीनियर्स या दोस्तों से सुनकर बनता है, जिससे छात्र इसे पढ़ना शुरू करके भी “कुछ दिनों में ही छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं।” इस समस्या के समाधान के लिए, स्रोत “प्रश्नोत्तरी और थ्योरी के माध्यम से” ग्रंथ को पढ़ने का सुझाव देते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण पैराग्राफों की व्याख्या और उन पर आधारित प्रश्नोत्तर शामिल होंगे।
यह ग्रंथ मूल रूप से सन् 1929 के जनवरी महीने में “हिंदी शब्दसागर” की भूमिका के रूप में “हिंदी साहित्य का विकास” नाम से प्रकाशित हुआ था। बाद में शुक्ल जी ने इसे एक स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ के रूप में “हिंदी साहित्य का इतिहास” नाम से प्रकाशित किया, जिसमें “विकास” शब्द को हटाकर “इतिहास” शब्द का प्रयोग किया गया। इसका उद्देश्य “आलोचनात्मक दृष्टि” को अधिक स्थान देना था, क्योंकि “विकास में मुकता आलोचनात्मक दृष्टिका प्रयोग कम किया जाता है इतिहास में हमारा जो है आलोचनात्मक दृष्टि भी होता है।”
2. पूर्ववर्ती कविवृत्त-संग्रह और इतिहास लेखन की आवश्यकता
शुक्ल जी अपने ग्रंथ की आवश्यकता पर जोर देते हुए बताते हैं कि उनसे पहले के प्रयास “केवल कविवृत्त-संग्रह” थे, न कि व्यवस्थित इतिहास।
- ठाकुर शिवसिंह सेंगर का ‘शिवसिंह सरोज’ (1833 ई.): इसे “हिंदी कवियों का एक वृत्तसंग्रह” कहा गया।
- डॉ. ग्रियर्सन का ‘मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑव नार्दर्न हिंदुस्तान’ (1889): इसे “एक वैसा ही बड़ा कविवृत्त-संग्रह” बताया गया।
- नागरीप्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्टें (1900-1911): सभा ने सरकार की सहायता से हजारों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज की, जिससे “सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगा” और साहित्येतिहास के लिए “कच्चा माल प्राप्त हुआ।”
- मिश्रबंधुओं का ‘मिश्रबंधु विनोद’ (1913): इसे “एक बड़ा भारी कविवृत्त-संग्रह” कहा गया, जिसमें “वर्तमान लेखकों का भी समावेश” था।
शुक्ल जी इन संग्रहों की सीमाएँ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि “भिन्न-भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपर्युक्त वृत्तमालाएँ साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थीं?” उनके अनुसार, “सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में ऑंख मूँद कर बाँट देना… किसी वृत्तसंग्रह को इतिहास नहीं बना सकता।”
विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा के विधान के बाद “साहित्य के विचार-श्रृंखला-बद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्रा और अध्यापक दोनों कर रहे थे।” शुक्ल जी का मानना था कि “शिक्षित जनता की जिन-जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो-जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन-जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य-धारा की भिन्न-भिन्न शाखाएँ फूटती रही हैं, उन सबके सम्यक् निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत कालविभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था।” उनका मुख्य उद्देश्य “अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढाँचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना।”
3. विधेयवादी पद्धति और काल-विभाजन का आधार
शुक्ल जी के काल-विभाजन पर फ्रेंच इतिहासकार तेन (Taine) के “विधेयवादी प्रभाव” को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। विधेयवाद, जिसे “प्रत्यक्षवादी” भी कहा जाता है, तीन मुख्य बातों पर आधारित है: “जाति, वातावरण और क्षण।” शुक्ल जी ने अपने नामकरण और विश्लेषण में इन्हीं “क्षण विशेष” का प्रयोग किया, जहाँ एक निश्चित कालखंड में किसी विशेष प्रकार की साहित्यिक रचनाओं की प्रधानता थी।
शुक्ल जी ने अपने काल-विभाजन और उनके नामकरण के लिए दो मुख्य बातों को ध्यान में रखा:
- “रचनाओं की प्रचुरता”: “जिस कालविभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है।” ‘प्रचुरता’ का अर्थ है कि किसी एक प्रकार की रचना अन्य किसी एक प्रकार की रचना से संख्या में अधिक हो, भले ही अन्य सभी प्रकार की रचनाओं का कुल योग अधिक हो (उदाहरण: 10, 5, 6, 7, 2 के अनुपात में 10 को प्रचुर माना जाएगा)।
- “ग्रंथों की प्रसिद्धि”: “किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी…।” शुक्ल जी प्रसिद्धि को “किसी काल की लोकप्रवृत्ति की प्रतिध्वनि” मानते हैं। उनका जोर है कि मात्रात्मक प्रचुरता के साथ-साथ प्रसिद्धी भी महत्वपूर्ण है, भले ही कुछ अप्रसिद्ध रचनाएँ कोनों में पड़ी मिलें।
4. आदिकाल का नामकरण ‘वीरगाथा काल’
शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम “वीरगाथा काल” (संवत् 1050 से 1375 तक) रखा है, उपर्युक्त दो प्रवृत्तियों (प्रचुरता और प्रसिद्धी) को ध्यान में रखते हुए।
रचनाओं के प्रकार: आदिकाल के भीतर दो प्रकार की रचनाएँ मिलती हैं:
- अपभ्रंश की रचनाएँ: जो हिंदी के विकास की पूर्व स्थिति को दर्शाती हैं। शुक्ल जी ने अपभ्रंश की चार साहित्यिक पुस्तकों को माना है:
- विजयपाल रासो
- हम्मीर रासो
- कीर्तिलता
- कीर्तिपताका शुक्ल जी स्पष्ट करते हैं कि जैन धर्म तत्व निरूपण से संबंधित अपभ्रंश की पुस्तकें “साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं,” उनका उल्लेख केवल अपभ्रंश भाषा के व्यवहार को दिखाने के लिए किया गया है। हम्मीर रासो के संबंध में विशेष उल्लेख है कि यह पुस्तक रूप में नहीं मिला, बल्कि इसके कुछ छंद “प्राकृत पिंगल सूत्र” में लक्ष्मीधर द्वारा संकलित मिले थे, जिससे शुक्ल जी को पूर्ण निश्चय हो गया कि “ये पद्य शारंगधर के प्रसिद्ध हम्मीर रासो के ही हैं।”
- देशभाषा (बोलचाल) की रचनाएँ: जिसमें अवधी, बघेली, मैथिली, राजस्थानी आदि आती हैं। शुक्ल जी ने देश भाषा काव्य की आठ पुस्तकों का उल्लेख किया है:
- खुमान रासो
- बीसलदेव रासो
- पृथ्वीराज रासो
- जयचंद प्रकाश
- जय मयंक जस चंद्रिका
- परमाल रासो (आल्ह खंड का मूल रूप)
- खुसरो की पहेलियां
- विद्यापति पदावली
वीरगाथात्मक रचनाएँ (नामकरण का आधार): कुल 12 पुस्तकों में से (4 अपभ्रंश + 8 देश भाषा), शुक्ल जी ने तीन को वीरगाथात्मक नहीं माना:
- बीसलदेव रासो (इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है)
- विद्यापति पदावली (मुख्यतः श्रृंगार और भक्ति रस पर आधारित)
- खुसरो की पहेलियां
इन तीनों को छोड़कर शेष नौ ग्रंथ (चार अपभ्रंश और पाँच देश भाषा के) वीरगाथात्मक हैं। इन्हीं नौ प्रसिद्ध वीरगाथात्मक पुस्तकों की प्रचुरता और प्रसिद्धी के आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण “वीरगाथा काल” किया।
मिश्रबंधुओं के आदिकाल संबंधी मत का खंडन: शुक्ल जी ने मिश्रबंधुओं द्वारा आदिकाल में उल्लिखित अतिरिक्त पुस्तकों (जैसे भगवत्गीता, वृद्ध नवकार आदि) पर आपत्ति जताई। उन्होंने ‘भगवत्गीता’ को उसकी भाषा के आधार पर बाद की रचना सिद्ध किया और जैन धर्म तत्व निरूपण परक पुस्तकों को साहित्य कोटि में न आने वाला बताया। वे कहते हैं, “यदि ये भिन्न-भिन्न प्रकार की नौ पुस्तकें साहित्यिक भी होतीं, तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थीं, क्योंकि मैंने नौ प्रसिद्ध वीरगाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है।”
5. भक्तिकाल और रीतिकाल का विभाजन और आलोचनात्मक दृष्टिकोण
भक्तिकाल: शुक्ल जी ने भक्तिकाल को दो मुख्य काव्यधाराओं में विभाजित किया:
- निर्गुण धारा:ज्ञानाश्रयी शाखा (जैसे कबीर)
- प्रेममार्गी (सूफी) शाखा (जैसे जायसी)
- सगुण धारा:रामभक्ति शाखा (जैसे तुलसीदास)
- कृष्णभक्ति शाखा (जैसे सूरदास)
उन्होंने स्पष्ट किया कि “इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यों ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है। उनकी एक-दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएँ अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में आ भी जाएँगी।”
रीतिकाल: रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की परंपरा में शुक्ल जी को उपविभाग करने का कोई संगत आधार नहीं मिला। उनका तर्क था कि “किसी कालविस्तार को लेकर यों ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता।” वे “विभाग का कोई पुष्ट आधार” होना आवश्यक मानते थे, जो उन्हें इस काल में नहीं मिला, हालाँकि उन्होंने भविष्य में गहरी छानबीन से आधार मिलने की संभावना जताई।
6. कवियों के परिचयात्मक विवरण और आलोचना की सीमाएँ
शुक्ल जी का उद्देश्य “साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढाँचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना।” इसलिए उन्होंने कवियों के “परीक्षात्मक विवरण” के लिए मुख्य रूप से मिश्रबंधु विनोद से सहायता ली, विशेषकर रीतिकाल के कवियों के लिए। उन्होंने कुछ कवियों (जैसे ठाकुर, दीनदयाल गिरि) के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किया।
शुक्ल जी का मानना था कि “इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती है।” वे आलोचना के लिए “स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक” लिखने के पक्षधर थे। उन्होंने स्वयं “त्रिवेणी” नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने तीन प्रिय कवियों (तुलसीदास, जायसी, सूर) की आलोचना प्रस्तुत की।
7. आधुनिक काल और गद्य का महत्व
शुक्ल जी आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव को “सबसे प्रधान साहित्यिक घटना” मानते हैं। इसलिए उन्होंने इसके प्रसार का वर्णन “विशेष विस्तार के साथ” किया है।
वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में लिखना उन्हें “अपने सर पर एक बड़ा मूल्य ना समझ पड़ता था” या “अपने सिर एक बला मोल लेना ही” समझ पड़ता था, क्योंकि समकालीन लेखकों के बारे में निष्पक्ष और पूर्ण विवरण देना कठिन होता है और इससे विवाद उत्पन्न हो सकते थे। इसके बावजूद, “जी न माना,” और उन्होंने “वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े-बहुत विवेचन के साथ डरते-डरते किया।” उन्होंने स्वीकार किया कि जल्दबाजी और भूल से कई प्रभावशाली लेखकों के नाम छूट गए होंगे, जिसके लिए उन्होंने क्षमा याचना की। उनका मुख्य ध्यान “सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर ही अधिक” था, न कि संग्रह की ओर।
8. अन्य स्रोतों का आभार और विनम्रता
मिश्र बंधु विनोद के अतिरिक्त, शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ के लिए निम्नलिखित स्रोतों से भी सामग्री एकत्र की और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की:
- श्याम सुंदर दास की “हिंदी कोविद्रत्न माला”
- रामनरेश त्रिपाठी की “कविता कौमुदी”
- श्री वियोगी हरि जी की “ब्रज माधुरी सार”
- ‘प्राकृत पिंगल सूत्र’ (हम्मीर रासो के छंदों की पुष्टि के लिए)
उन्होंने अपने पुराने मित्र पं. केदारनाथ पाठक का भी उल्लेख किया, जिन्होंने आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय सहायता की थी। शुक्ल जी ने विनोदपूर्ण ढंग से कहा कि वे उन्हें धन्यवाद नहीं दे सकते क्योंकि पाठक जी ‘धन्यवाद’ को ‘आजकल की एक बदमाशी’ समझते हैं।
अंत में, शुक्ल जी अपनी त्रुटियों, भूलों और अपराधों के लिए “क्षमा की पूरी आशा” करते हैं, जिससे उनके श्रम से “कुछ संतोष लाभ” हो सके। यह उनकी विद्वत्तापूर्ण विनम्रता और आलोचनात्मक संस्कार को दर्शाता है।
निष्कर्ष:
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ‘हिंदी साहित्य का इतिहास’ मात्र कवियों का संग्रह नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित, तर्कपूर्ण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित साहित्येतिहास है। उनकी विधेयवादी पद्धति, काल-विभाजन के स्पष्ट मानदंड (रचनाओं की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि), और आदिकाल को ‘वीरगाथा काल’ नाम देने के पीछे के तर्क हिंदी साहित्य के अध्ययन को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। यह ग्रंथ आज भी हिंदी साहित्य के छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक मौलिक और अपरिहार्य संदर्भ स्रोत बना हुआ है।
एक विस्तृत अध्ययन मार्गदर्शिका
लघु उत्तरीय प्रश्न
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दें:
- रामचंद्र शुक्ल से पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के क्षेत्र में कौन से दो प्रमुख कविवृत्त-संग्रह प्रकाशित हुए थे?
- नागरीप्रचारिणी सभा ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया?
- शुक्ल जी ने साहित्य के इतिहास के अध्ययन में पूर्ववर्ती वृत्त-संग्रहों की किस सीमा का उल्लेख किया है?
- रामचंद्र शुक्ल ने अपने काल-विभाजन की पद्धति के दो मुख्य आधार क्या बताए हैं?
- शुक्ल जी ने ‘आदिकाल’ का नाम ‘वीरगाथा काल’ क्यों रखा?
- मिश्रबंधुओं द्वारा आदिकाल में उल्लिखित ‘भगवत्गीता’ को शुक्ल जी ने क्यों नहीं स्वीकार किया?
- शुक्ल जी ने भक्तिकाल को किन मुख्य काव्यधाराओं और उनकी शाखाओं में विभाजित किया है?
- रीतिकाल के भीतर उपविभाग न करने के पीछे शुक्ल जी का क्या तर्क था?
- आधुनिक काल के संबंध में शुक्ल जी ने किस साहित्यिक घटना को सबसे प्रधान माना है?
- ‘हिंदी साहित्य का इतिहास’ मूल रूप से किस पुस्तक की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था?
उत्तर कुंजी
- रामचंद्र शुक्ल से पहले ठाकुर शिवसिंह सेंगर का ‘शिवसिंह सरोज’ (1833 ई.) और डॉ. ग्रियर्सन का ‘मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑव नार्दर्न हिंदुस्तान’ (1889) नामक दो प्रमुख कविवृत्त-संग्रह प्रकाशित हुए थे। ये संग्रह कवियों के परिचय और उनकी रचनाओं का संकलन थे।
- नागरीप्रचारिणी सभा ने 1900 से 1911 तक सरकार की आर्थिक सहायता से हजारों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया। इसकी आठ रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों और ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता चला, जिससे इतिहास लेखन के लिए प्रचुर सामग्री उपलब्ध हुई।
- शुक्ल जी के अनुसार, पूर्ववर्ती वृत्त-संग्रह साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कम सहायता पहुँचा सकते थे क्योंकि वे हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी वृत्तमालाएँ थीं। उनमें शिक्षित जनता की प्रवृत्तियों या काव्य-धाराओं के विकास के सम्यक् निरूपण का अभाव था।
- शुक्ल जी ने अपने काल-विभाजन की पद्धति के दो मुख्य आधार बताए हैं: पहला, किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता; और दूसरा, उस काल के भीतर किसी एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथों की प्रसिद्धि। इन दोनों के आधार पर ही कालविभागों का नामकरण किया गया।
- शुक्ल जी ने ‘आदिकाल’ का नाम ‘वीरगाथा काल’ इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने उस काल की आठ देशभाषा काव्य की प्रसिद्ध पुस्तकों और चार अपभ्रंश की साहित्यिक पुस्तकों में से अधिकांश को वीरगाथात्मक पाया। उनके अनुसार, इन बारह पुस्तकों की दृष्टि से ही आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है।
- मिश्रबंधुओं द्वारा आदिकाल में उल्लिखित ‘भगवत्गीता’ को शुक्ल जी ने उसकी भाषा के आधार पर पीछे की रचना माना और कहा कि वह संवत् 1000 के क्या संवत् 500 की भी नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इसकी संवत्सूचक पंक्ति का पाठ भी गड़बड़ था।
- शुक्ल जी ने भक्तिकाल को पहले दो मुख्य काव्यधाराओं – निर्गुण धारा और सगुण धारा में विभाजित किया। फिर निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेममार्गी (सूफी) शाखाओं में, तथा सगुण धारा को रामभक्ति और कृष्णभक्ति शाखाओं में बांटा।
- रीतिकाल के भीतर उपविभाग न करने के पीछे शुक्ल जी का तर्क था कि उन्हें रीतिबद्ध रचना की परंपरा में रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित करने का संगत आधार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बिना अलग-अलग लक्षणों के “पूर्व” और “उत्तर” जैसे नाम देकर विभाजन करना ऐतिहासिक नहीं कहला सकता।
- आधुनिक काल के संबंध में शुक्ल जी ने गद्य के आविर्भाव को सबसे प्रधान साहित्यिक घटना माना है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि गद्य के प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है, क्योंकि यह आधुनिक साहित्य की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण था।
- ‘हिंदी साहित्य का इतिहास’ मूल रूप से ‘हिंदी शब्दसागर’ की भूमिका के रूप में ‘हिंदी साहित्य का विकास’ के नाम से सन् 1929 के जनवरी महीने में प्रकाशित हुआ था। बाद में इसे एक अलग पुस्तकाकार संस्करण के रूप में संशोधित और परिवर्धित किया गया।
निबंधात्मक प्रश्न (Essay Questions)
- रामचंद्र शुक्ल ने अपने से पूर्ववर्ती कविवृत्त-संग्रहों की क्या आलोचनाएँ की हैं और उनके अनुसार एक ‘सच्चे साहित्य के इतिहास’ के लिए क्या आवश्यक है?
- शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित काल-विभाजन की पद्धति को विस्तार से समझाइए। आदिकाल को ‘वीरगाथा काल’ नाम देने के पीछे उनके क्या तर्क थे और उन्होंने मिश्रबंधुओं के मत का खंडन कैसे किया?
- आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल और रीतिकाल के वर्गीकरण और निरूपण में किन सिद्धांतों का पालन किया है? रीतिकाल के उपविभाजन में उनकी क्या चुनौतियाँ थीं और उन्होंने उन्हें कैसे संबोधित किया?
- ‘हिंदी साहित्य का इतिहास’ के लेखन में शुक्ल जी की ‘उद्देश्य हानि’ और ‘बला मोल लेने’ जैसी टिप्पणियाँ उनकी लेखन प्रक्रिया, सीमाओं और विनम्रता को कैसे दर्शाती हैं? विस्तृत विवेचन कीजिए।
- रामचंद्र शुक्ल ने ‘हिंदी साहित्य का इतिहास’ के प्रथम संस्करण की भूमिका में किन स्रोतों का आभार व्यक्त किया है? यह उनके शोध की गंभीरता और पूर्ववर्ती कार्यों के प्रति उनके दृष्टिकोण को कैसे दर्शाता है?
पारिभाषिक शब्दावली (Glossary of Key Terms)
- आदिकाल: हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल (लगभग 10वीं से 14वीं शताब्दी तक), जिसे रामचंद्र शुक्ल ने ‘वीरगाथा काल’ नाम दिया।
- अपभ्रंश: मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी मानी जाने वाली प्राकृत भाषा का अंतिम रूप। शुक्ल जी ने इसे ‘भाषाकाव्य’ के अंतर्गत शामिल किया।
- आलोचनात्मक दृष्टि: किसी साहित्यिक कृति या प्रवृत्ति का गुण-दोष विवेचन करने वाला दृष्टिकोण।
- काल-विभाजन: साहित्य के इतिहास को विभिन्न समय-खंडों में विभाजित करना। शुक्ल जी ने इसे रचनाओं की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर करने पर बल दिया।
- कविवृत्त संग्रह (Kavivritta Sangrah): कवियों के जीवन-परिचय और उनकी रचनाओं के उदाहरणों का संकलन। यह साहित्य के इतिहास से भिन्न होता है क्योंकि इसमें कालगत प्रवृत्तियों और विकास का विश्लेषण नहीं होता। उदाहरण: शिवसिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑव नार्दर्न हिंदुस्तान, मिश्रबंधु विनोद।
- खुसरो की पहेलियां: अमीर खुसरो द्वारा रचित पहेलियां, जिन्हें शुक्ल जी ने वीरगाथा काल की 12 पुस्तकों में शामिल किया, पर वीरगाथात्मक नहीं माना।
- गद्य का विकास: आधुनिक काल में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि गद्य विधाओं का विकास, जिसे शुक्ल जी ने आधुनिक युग का प्रमुख परिवर्तन माना।
- ज्ञानाश्रयी शाखा (Gyanashrayi Shakha): निर्गुण भक्तिधारा की एक शाखा जिसमें ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति पर बल दिया जाता है (जैसे कबीर)।
- जाति, वातावरण, क्षण: विधेयवादी पद्धति के तीन प्रमुख आधार, जो साहित्य पर तत्कालीन परिस्थितियों के प्रभाव को दर्शाते हैं। (फ्रेंच इतिहासकार तेन Taine द्वारा प्रतिपादित)
- त्रिवेणी: आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एक आलोचनात्मक पुस्तक जिसमें उन्होंने तीन प्रमुख कवियों – तुलसीदास, जायसी और सूरदास – पर विचार किया है।
- नगरी प्रचारिणी सभा (Nagari Pracharini Sabha): काशी (वाराणसी) में स्थापित एक प्रमुख संस्था जिसने हिंदी साहित्य और भाषा के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, विशेष रूप से हस्तलिखित ग्रंथों की खोज में और ‘हिंदी शब्द सागर’ के संपादन में।
- नामकरण: किसी ऐतिहासिक कालखंड को उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर एक नाम देना।
- पूर्वाग्रह: किसी विषय या व्यक्ति के बारे में पहले से ही बनाई गई धारणा, अक्सर नकारात्मक, जो उसे समझने में बाधा डालती है।
- प्रकाण्ड कविवृत्त संग्रह: मिश्रबंधु विनोद के लिए शुक्ल जी द्वारा प्रयुक्त विशेषण, जो उसकी विशालता और कवियों के वृत्तों की बहुतायत को दर्शाता है।
- प्राकृत पिंगल सूत्र (Prakrit Pingal Sutra): प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के छंदों से संबंधित एक ग्रंथ, जिसका उपयोग शुक्ल जी ने ‘हम्मीर रासो’ के पदों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए किया।
- प्रचुरता (Prachurata): किसी विशेष काल में किसी एक प्रकार की रचनाओं की संख्यात्मक अधिकता, भले ही अन्य सभी प्रकार की रचनाओं का कुल योग अधिक हो। शुक्ल जी ने इसे काल-विभाजन का आधार बनाया।
- प्रत्यक्षवादी: विधेयवादी पद्धति का ही दूसरा नाम, जिसमें तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित अध्ययन पर जोर दिया जाता है।
- प्रसिद्धि (Prasiddhi): किसी काल में किसी एक ही ढंग के ग्रंथों का अधिक प्रचलित या मान्य होना, जिसे उस काल की लोकप्रवृत्ति का प्रतिध्वनि माना जाता है। शुक्ल जी ने इसे काल-विभाजन का दूसरा आधार बनाया।
- प्रेममार्गी (सूफी) शाखा (Premmargi (Sufi) Shakha): निर्गुण भक्तिधारा की एक शाखा जिसमें प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुँचने पर बल दिया जाता है, अक्सर प्रतीकात्मक प्रेमाख्यानों के रूप में (जैसे जायसी)।
- बीसलदेव रासो: नरपति नाल्ह द्वारा रचित एक रासो काव्य, जिसे शुक्ल जी ने 12 पुस्तकों में शामिल किया पर वीरगाथात्मक नहीं माना, क्योंकि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है।
- भूमिका: किसी पुस्तक के आरंभ में दिया गया परिचय, जिसमें लेखक अपनी कृति के उद्देश्य, पद्धति और स्रोतों का उल्लेख करता है।
- मिश्रबंधु विनोद: मिश्रबंधुओं (गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, शुकदेव बिहारी मिश्र) द्वारा रचित एक विशाल हिंदी साहित्येतिहास ग्रंथ (प्रकाशन 1913)।
- रामभक्ति शाखा (Ram Bhakti Shakha): सगुण भक्तिधारा की एक शाखा जिसमें राम को आराध्य मानकर उनकी भक्ति की जाती है (जैसे तुलसीदास)।
- रामचंद्र शुक्ल (आचार्य): हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक और इतिहासकार, जिनकी पुस्तक ‘हिंदी साहित्य का इतिहास’ मील का पत्थर मानी जाती है। (जन्म 1884, मृत्यु 1941)
- रीतिकाल: हिंदी साहित्य के इतिहास का एक कालखंड (मध्यकाल का उत्तरार्द्ध, लगभग 17वीं से 19वीं शताब्दी) जिसमें रीति-ग्रंथों और श्रृंगारपरक रचनाओं की प्रधानता रही।
- वीरगाथा काल (Veergatha Kaal): आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आदिकाल को दिया गया नाम, जिसमें वीर रस प्रधान काव्य रचनाओं की प्रमुखता मानी गई है।
- विद्यापति पदावली: विद्यापति द्वारा रचित मैथिली भाषा की पदावलियां, जो मुख्यतः श्रृंगार और भक्ति रस पर आधारित हैं, जिन्हें शुक्ल जी ने वीरगाथात्मक नहीं माना।
- विधेयवादी पद्धति (Positivist Method): साहित्येतिहास लेखन की एक पद्धति जिसमें साहित्य को तत्कालीन जाति, वातावरण और क्षण (परिस्थिति) के प्रभावों से जोड़कर देखा जाता है।
- शिवसिंह सरोज: शिवसिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह (प्रकाशन 1833 ई.)।
- हिंदी शब्द सागर: नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा संपादित एक विशाल हिंदी कोश, जिसकी भूमिका के रूप में शुक्ल जी ने अपना इतिहास ग्रंथ ‘हिंदी साहित्य का विकास’ लिखा था।
- कृष्णभक्ति शाखा (Krishna Bhakti Shakha): सगुण भक्तिधारा की एक शाखा जिसमें कृष्ण को आराध्य मानकर उनकी भक्ति की जाती है (जैसे सूरदास)।