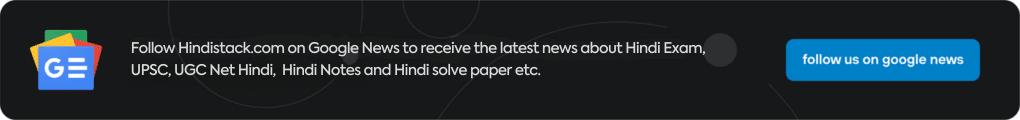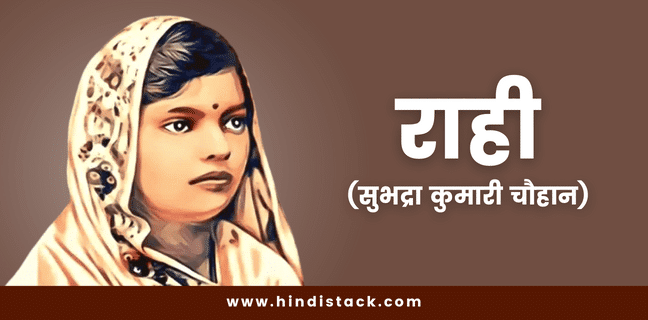वर्तमान युग मे अनुवाद कई अर्थों मे प्रयुक्त होता है। जैसे सामान्य अनुवाद, व्याख्या अनुवाद, पूर्वकथित बात का अनुवाद, टीका टिप्पणी का अनुवाद, विवरण, भाषिक अंतरण आदि। अनुवाद का आदि या पूर्व रूप–भाष्य तथा टीका है। निर्वचन-किसी शब्द का एक धातु अथवा अनेक धातुओं के साथ सम्बन्ध स्थापित करके उसका अर्थ निर्धारण करना निर्वचन कहलाता है। वेद के मंत्रो का अर्थ स्पष्ट करने के लिये ब्राम्हण ग्रंथो तथा आरण्यको मे कई स्थलों पर इस प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है।
- ब्राम्हण ग्रंथ भाष्य रूप है।
- आरण्यक टीका रूप है।
- यास्क कृत निरुक्त निर्वचन रूप है।
भाषिक अंतरण की दॄष्टि से हकीम बुजोई द्वारा छठी शताब्दी मे किया गया पंचतंत्र का अनुवाद सम्भवत: पहला अनुवाद है। वैदिक साहित्य का अनुवाद वैदिक साहित्य का भी कई भाषाओं मे अनुवाद किया गया है। वेदों और वेदांगो का भी अनुवाद किया गया है। वैदिक साहित्य मुख्यत: संस्कृत भाषा मे लिखा जाता था और संस्कृत से उसका अनुवाद हिंदी मे भी किया गया है।
- ऋग्वेद का लैटिन भाषा मे अनुवाद
- शतपथ एवं एतरेय ब्राम्हण ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा मे अनुवाद
- तैतरीयोपनिषद एवं कठोपनिषद् का अंग्रेजी मे अनुवाद
- धर्मसूत्रो की अंग्रेजी मे व्याख्या
इस युग मे मुख्य रूप से दो बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है-
- इस युग मे शब्दानुवाद पर बल दिया गया था।
- शब्दों को ज्यों का त्यों स्वीकार किया गया था।
रामायण का अंग्रेजी मे पद्यानुवाद और गद्यानुवाद किया गया और गीताप्रेस द्वारा अंग्रेजी मे प्रकाशित किया गया। महाभारत का भी विभिन्न भाषाओं मे अनुवाद किया गया। श्री मद्भगवत् गीता का विशेष रूप से अनुवाद किया गया। श्री मद्भगवत् गीता का अनुवाद करने के लिये अनुवादक नियुक्त किये जाते थे। पुराणों का भी अंग्रेजी अनुवाद किया गया। रामायण के अनुवाद के समय की दो विशेष बातें थी–
- टीका-टिप्पणी की परम्परा का प्रारम्भ
- भावानुवाद का आरम्भ
रामायण के अनुवाद के समय टीका-टिप्पणी के अनुवाद की परम्परा का प्रारम्भ हुआ उससे पहले हमें टीका-टिप्पणी के अनुवाद की परम्परा नहीँ दिखायी देती है और इसी समय ही भावानुवाद का आरम्भ शुरु होता है।
संस्कृत के महाकाव्यों का अनुवाद:
कालिदास द्वारा संस्कृत भाषा मे रचित महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम का कई विद्वानो ने कई भाषाओ मे अनुवाद किया। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह और महादेवी वर्मा ने किया। उर्दू मे विशेश्वर प्रसाद मुनव्वर ने किया। एम.एस. विलियम्स ने इसका अंग्रेजी मे अनुवाद किया। संस्कृत के कई अन्य ग्रंथों के अनुवाद भी हिंदी और अंग्रेजी भाषा मे होते रहे हैं। गोरखपंथो की भी कई पुस्तकों का हिंदी अनुवाद किया है।
हिंदी के अन्य महाकाव्यों का कई भाषाओं मे अनुवाद किया गया जैसे– रामचरित मानस, सूरसागर, रासपंचाध्यायी, रामचन्द्रिका आदि का अनेक भाषाओं मे अनुवाद किया गया। संस्कृत के कई ग्रंथों का सारानुवाद और भावानुवाद किया गया। 19वीं शताब्दी मे अनुवाद का कार्य भाषांतरण के साथ-साथ भाव प्रसार के रूप मे भी सामने आया। उमर खय्याम की रूबाइयो का अनुवाद अंग्रेजी मे फिट्जेराल्ड ने किया और फिट्जेराल्ड के अनुवाद को मूल मानकर हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला नाम से हिंदी मे अनुवाद किया। हिंदी के कई अन्य कवियों जैसे- पंत, प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त आदि ने फिट्जेराल्ड की रचना का हिंदी अनुवाद किया। आज अनुवाद साहित्य के संरक्षण एवं प्रसार के रूप मे सामने आ रहा है।
भारतीय परिप्रेक्ष्य मे अनुवाद का प्रारम्भ भाष्य तीकाओं से हुआ था। हिंदी मे अनुवाद की परम्परा हिंदी गद्य के विकास से जुड़ी है। 18वीं शती मे राम प्रसाद निरंजनी ने “भाषा योगवशिष्ठ” के रूप मे किया। इस विकास क्रम को हम निम्नलिखित क्रम मे देख सकते हैं।
प्रारम्भिक दौर:
हिंदी अनुवाद के विकास मे अंग्रेजी पादरियों का विशेष योगदान रहा। विलियम केरे ने न्यू टेस्टामेंट का हिंदी मे अनुवाद प्रकाशित कराया। आगरा मे एक स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी खोली गयी जहाँ 1894 मे इंग्लैंड के इतिहास का तथा प्राचीन इतिहास का कथासार के नाम से अनुवाद किया । इसी दौर मे राजा राम मोहन राय ने भाष्य के वेदांग सूत्रो का हिंदी अनुवाद प्रकाशित कराया। हितोपदेश और राजा लक्ष्मण सिंघ के कालिदास के नाटक ‘अभिज्ञान शाकुंतलम’ के अनुवाद हुए।
भारतेंदु युग:
भारतेंदु युग मे उपन्यास, नाटक, निबंध रचना के साथ साथ इन विधाओं के अनुवाद भी हुए। इन अनुवादो मे अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, मराठी, भाषाओं के नाटकों के अनुवाद विशेष उल्लेखनीय हैं । भारतेंदु ने स्वयं के हरिश्चंद्र नाटक और शेक्ससपियर के Marchent of Venis नाटक का अनुवाद किया। श्रीनिवास दास, तोताराम, बाबू रामकृष्ण वर्मा आदि ने भी कई अनुवाद किये।
द्विवेदी युग:
पिछले युग की तरह द्विवेदी युग मे भी अनुवाद जारी रहे । गोपीनाथ पुरोहित ने शेक्सपियर के ‘रोमियो जुलियेट’ का ‘प्रेमलीला’ नाम से अनुवाद किया। पं. मथुरा प्रसाद चौधरी ने शेक्सपियर के नाटक ‘मैकबेथ’ और ‘हेमलेट’ का क्रमश: ‘साहसेंद्र साहस’ और ‘जयंत’ नाम से अनुवाद किया। अनेक बंगला लेखकों के उपन्यास के अनुवाद हुए।
श्रीधर पाठक ने अंग्रेजी साहित्य की कृतियों का अनुवाद किया। उन्होंने “Goldsmith“ के Traveller, Dessert Village तथा Hermit का क्रमश: श्रांत पथिक, उजड़ ग्राम तथा एकांतवासी योगी शीर्षक से अनुवाद किये। यह अनुवाद सुंदर और परिष्कृत मालूम होते हैं। मैथिली शरण गुप्त, हरिवंशराय बच्चन ने भी बहुत से अनुवाद किये हैं। वर्तमान युग मे अनुवादो की भरमार है। बच्चन ने फिट्जेराल्ड की रचना का मधुशाला नाम से हिंदी अनुवाद किया है।