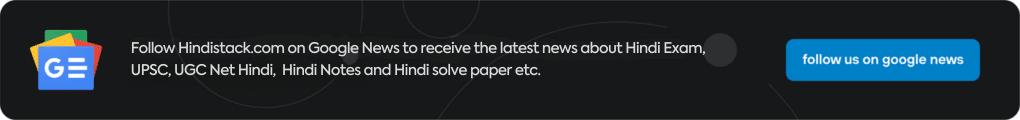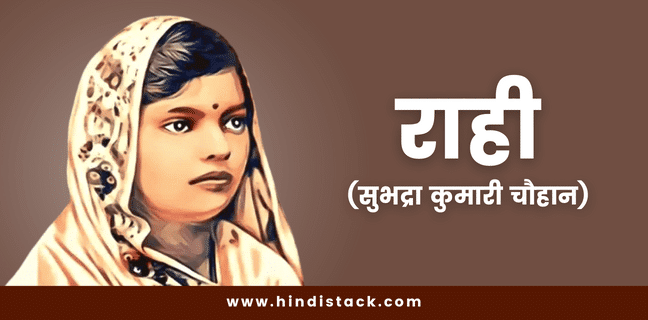हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में ‘आदिकाल’ को लेकर हमेशा से एक विवाद रहा है। अब चाहे इसके नामकरण की बात हो या काल-विभाजन की सभी इतिहासकारों व विद्वानों में पर्याप्त मतभेद मिलते हैं। कारण यह है कि उस समय के इतिहास का समुचित पर्यालोचन करने में इतिहासकारों व विद्वानों को कठिनाई होती है, ग्रंथों का प्राप्त ना होना, रचनाओं पर प्रमाणिकता – आप्रमाणिकता का सवाल लगना, उनमें ऐतिहासिक सामंजस्य ना होना आदि ऐसी बातें हैं जिनके अभाव में कोई निश्चित व्यवस्थित धारणा बना लेना अपने आप में बड़े कौशल का कार्य है। साथ ही इस युग में धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक आदि सभी क्षेत्रों में भी परस्पर विरोधी तत्व दिखाई देते हैं जिसकी और संकेत करके आचार्य हजारी प्रसाद ‘द्विवेदी’ ने अक्षरश: स्तय ही लिखा है-
“शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों और स्वतोव्याघातों का युग कभी आया होगा।……संक्षेप में इतना जान लेना यहाँ पर्याप्त है कि यह काल भारतीय विचारों के मंथन का काल है, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।”
ऐसी स्थिति में ऐसे समय को किस नाम से पुकारा जाए यह भी एक समस्या है। विद्वानों ने आदिकाल को अपनी आलोचनात्मक दृष्टि से मूल्यांकन करने के पश्चात इसे अलग-अलग नामों से पुकारना चाहा। जिसे हम संक्षेप में देख सकते हैं जैसे-
- जार्ज ग्रियर्सन – चारण कविता
- मिश्र बन्धु – पूर्व प्रारंभिक काल
- रमाशंकर शुक्ल रसाल – बाल्यावस्था काल
- आचार्य रामचंद्र शुक्ल – आदिकाल या वीरगाथा काल
- महापंडित राहुल सांकृत्यायन – सिद्ध सामंत काल
- डॉ रामकुमार वर्मा – संधि काल तथा चारण काल
- आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी – आदि काल
- डॉक्टर गणपति चंद्र – आदि काल और स्वर्ण काल
- हिंदी साहित्य का इतिहास – संक्रमण काल
- डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ – अंधकार काल
- डॉ राकेश – उत्तर अपभ्रंशकाल या आविर्भावकाल
वीरगाथा काल:
जिस काल में आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उस समय बहुत से सहायक ग्रथों की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हो सकी थी। उनके रचना-काल का निर्धारण भी निर्विवाद नहीं था। अतः शुक्ल जी के इतिहास-लेखन की कुछ सीमा अवश्य हो सकती है। यह अवश्य ही उनकी असाधारण गवेषणा शक्ति का परिणाम है कि उनके द्वारा किये गए काल-विभाजन एंव नामकरण को अधिकांशतः स्वीकार किया गया है। आदिकाल के नामकरण पर अवश्य हिनकुच गतिरोध है। इसका नामकरण शुक्ल जी ने ‘वीरगाथा-काल’ के रूप में किया है जिससे सभी विद्वान संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि इस काल की वीरगाथाओं की प्रामाणिकता संदेहास्पद है। आदिकाल के सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रन्थ ‘पृथ्वीराज रासो’ की प्रमाणिकता में भी कतिपय विद्वानों ने संदेह किया है। शुक्ल जी ने स्वयं भी लिखा है-
“इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर जो थोड़ा- बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ेगा।”
संधिकाल एंव चारण-काल:
डॉ० रामकुमार वर्मा ने “हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास” (1938) में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिपाटी का ही अनुसरण किया है। नामकरण में अवश्य ही सरलीकरण की नीति अपनाई गयी है। वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम युग को आठवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक माना है तथा उसे दो भागों में बाँटकर ‘संधिकाल’ एंव ‘चारण-काल’ नाम प्रदान किये हैं।
प्रारम्भिक काल
मिश्रबन्धुओं ने अपने ‘मिश्रबन्धु-विनोद’ में 643 ई०-1387 ई० तक के आदिकाल को ‘प्रारम्भिक काल’ नाम दिया, जो एक सामान्य संज्ञा है; उसके पीछे किसी प्रवर्ति आदि का आधार नहीं है। उन्होंने अपने ‘विनोद’ में प्रारंभिक काल के पीछे ‘हिंदी भाषा’ को अवश्य ध्यान में रखा है, इसलिये अध्यायों के अंतर्गत ‘पूर्व प्रारंभिक हिंदी’ (643 ई० – 1290 ई०), ‘चंद-पूर्व की हिंदी’ (643 ई० – 1143 ई०), ‘रासो-काल’ (1143 ई०-1290 ई०), ‘उत्तरआरम्भिक हिंदी’ (1291 ई०-1387 ई०) आदि नाम दिये हैं। किंतु इन नामों से भी आदिकाल की कोई उपयुक्त संज्ञा नहीं बनती।
अंधकार काल:
डॉ० पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने इस काल का नामकरण ‘अंधकार काल’ किया है। उन्होंने इस संदर्भ में कई तर्क दिए हैं। उनके अनुसार इसे वीरगाथाकाल इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि इस युग की कोई प्रामाणिक वीर-गाथात्मक कृति उपलब्ध नहीं होती। श्रीधर का ‘रंगमल छंद’ एक ऐसा अकेला ग्रन्थ है, जो आज प्राप्त है लेकिन इस एक रचना के कारण पूरे काल की प्रवृत्ति को सिद्ध नहीं किया जा सकता। खोज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अभी तक यह अंधकार-युग ही है। इस युग की मूल प्रमाण कृति कोई नहीं मिली है। मिश्रबंधु हिंदी साहित्य के प्रथम सोपान का आरंभ 713 ई० से मानते हैं- राहुल सांकृत्यायन 760 ई० से मानते हैं। वस्तुतः 1007 से लेकर 1400 ई० तक के बीच में ही निश्चित- साहित्य मिलना शुरू हो पाता है। ऐसी स्थिति में संदिग्ध अव्यवस्था वाले काल-खंड को अंधकार युग कहना अधिक समीचीन है। लेकिन यह मत विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया।
अपभ्रंश काल:
डॉ० हरीश ने इसे उत्तर-अपभ्रंश-काल कहा है। उनका तर्क है कि यह उत्तर अपभ्रंश ही देसी-भाषा है- पुरानी हिंदी। इसकी रचनाएं भी उपलब्ध हैं। राजस्थान आदि राज्यों के जैन एवं अन्य प्राचीन भंडारों में सैकड़ों/ हजारों की तादाद में पांडुलिपियाँ पड़ी हुई है जिनका पाठालोचन, विश्लेषण- विवेचन और सही मूल्यांकन होना अभी बाकी है। ‘उत्तर-अपभ्रंश’ शब्द में अपभ्रंश के उत्तरवर्ती युग के समस्त साहित्यिक प्रवृत्तियों/काव्य-रूढ़ियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सिद्धों, नाथों, जैनियों, लोककवियों की अवधी, ब्रजी, पुरानी राजस्थानी, जूनी या गुजराती आदि में लिखी गई रचनाओं का समावेशन हो जाता है।
आदिकाल:
हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक एवं चिंतक साहित्य मनीषी आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा और साहित्य के प्रथम सोपान का अभिषान ‘आदिकाल’ दिया है। इसी शीर्षक से उन्होंने विशद विस्तृत एवं विशिष्ट वक्तव्य दिए जो ‘आदिकाल’ नामक शीर्षक से ही अलग पुस्तकाकार प्रकाशित भी हुए हैं और बहुचर्चित भी हुए हैं। शुक्ल जी के विपरीत उन्होंने एक सामान्य कालखंड को आधार मानकर नामकरण कर दिया है। आदि का अर्थ अधकच्चा/आरम्भिक या एकदम लूंजपुंज नहीं है। यहां आदि शब्द भाषिक/साहित्यिक वृतियों का वाचक है जो एक पृथक- स्वतंत्र रूप में धीरे-धीरे हिंदी के रचनाफलक पर उतरने लगती है । दिवेदी जी ने अपभ्रंश और हिंदी में भेद किया है। राहुल जी के मत का खंडन करते हुए उन्होंने कहा है–
“अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने का विचार भाषा-शास्त्रीय और वैज्ञानिक नहीं है। भाषा-शास्त्र के अर्थ में जिसे हम हिंदी कहते हैं , वह इस साहित्यिक अपभ्रंश से सीधी विकसित नहीं हुई है ।अपभ्रंश को अब कोई भी प्राणी हिंदी नहीं कहता ।”
दिवेदी जी ने जैन मुनियों एवं सिद्धों की रचनाओं को पर्याप्त महत्व दिया है । उन्होंने उस समय की रचनाओं में दो प्रकार की भाषिक प्रवृतियां देखी हैं –
- कुछेक में साहित्यिक अपभ्रंश के गुण ज्यादा हैं
- कुछेक में लोकभाषा या अपभ्रंश से कुछ आगे बढ़ी हुई भाषा ( परिनिष्ठित हिंदी ) के गुण अधिक हैं ।
यह और बात है कि दूसरे वर्ग की अधिकांश रचनाओं का मूल स्वरूप या तो विकृत हो चुका है अथवा वे अब उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार द्विवेदी जी सातवीं शती के समस्त लोकसाहित्य को स्वीकारते हैं जो साहित्यिक या असाहित्यिक गुणों से भरपूर है। पर वे उसे रखते अलग ही दायरे में हैं – अपभ्रंश के दायरे में। द्विवेदी द्वारा दिये गए अभिधान पर डॉ० गणपति चंद्र गुप्त ने तीखी चुटकी ली है। उन्होंने तर्क देकर एक नई प्रतिस्थापना का प्रयास किया है कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिस तरह परिश्रमपूर्वक गहन गवेषणा करके उस युग के ग्रंथों को समझने/समझाने का प्रयास किया है और हिंदी भाषा और साहित्य के प्रथम सोपान की उलझनों को जिस तरह से और जिस हद तक वैज्ञानिक/तार्किक तरीके से सुलझाने का यत्न किया है उसके फलस्वरुप विद्वत परंपरा में ‘आदिकाल’ नाम गृहीत किया गया है ।
निष्कर्ष :
वास्तव में ‘आदिकाल’ ही ऐसा नाम है, जिसे किसी न किसी रूप में सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है तथा जिससे हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा, भाव, विचारणा, शिल्प-भेद आदि से संबंद्ध सभी गुत्थियां सुलझ जाती हैं। इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है, जिस पर आगे का साहित्य खड़ा है। भाषा की दृष्टि से हम इस काल के साहित्य में हिंदी के आदि रूप का बोध पा सकते हैं, तो भाव की दृष्टि से इसमें भक्तिकाल से आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदिम बीज खोज सकते हैं। जहां तक रचना शैलीयों का प्रश्न है, उनके भी वे सभी रूप, जो परवर्ती काव्य में प्रयुक्त हुए, अपने आदि रूप में मिल जाते हैं। इस काल की आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का ही विकसित रूप परवर्ती साहित्य में मिलता है। अतः ‘आदिकाल’ ही सबसे अधिक उपयुक्त एंव व्यापक नाम है।