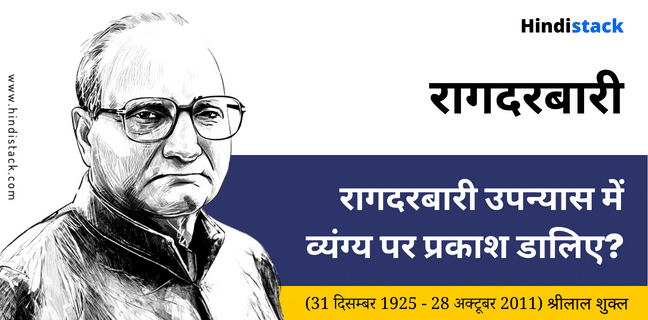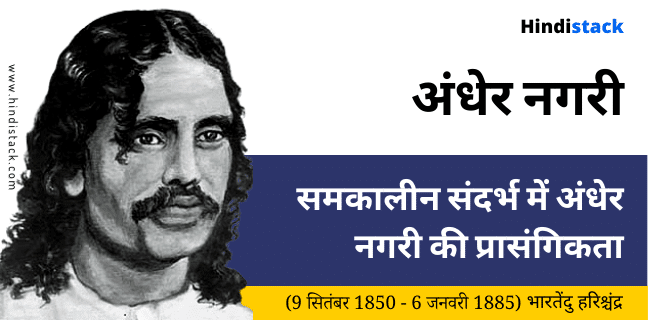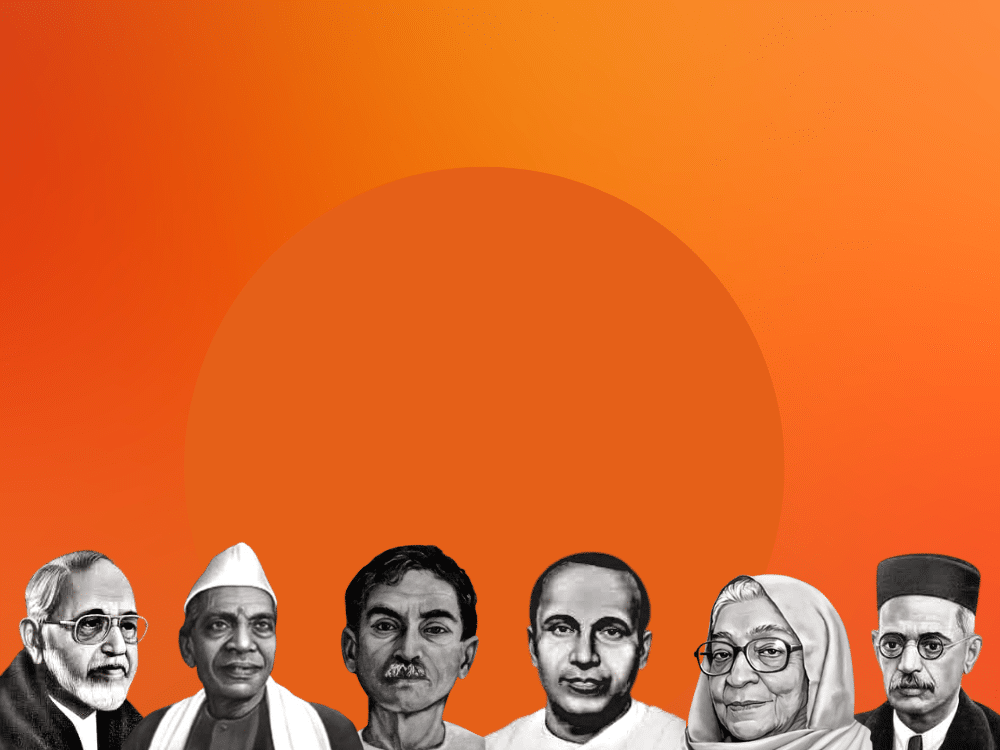संत कबीरदास का भारतीय समाज तथा संत साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। मध्यकाल भारत में अनेक समस्याएं जड़ जमा चुकी थी। धार्मिक रूढ़िया,अंधविश्वास, ऊँच-नीच, वर्ण व्यवस्था, हिंदू मुस्लिम झगड़े, अपनी चरम सीमा पर थे ऐसे समय में कबीर का जन्म हुआ। संत कबीरदास जी के समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक,अर्थिक एंव धार्मिक शोचनीय थी। एक तरफ जनता मुस्लमान शासकों धर्मान्धता से दुखी थी तो दूसरी ओर हिंदु धर्म के कर्मकांड और पाखंड का पतन हो रहा था। संत कबीर उस समय अवतरित हुए जब मध्यकाल घोर निराशा एंव अधंकार से घिरा हुआ था। छुआछूत, रुढ़िवादिता का बोला बाला था, और हिंदु मुस्लिम आपस में दंगा फसाद करते रहते थे। कबीर ने इन सभी सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। आचार्य द्विवेदी ने बहुत बल देकर कहा है-
कबीर ने धार्मिक पांखड़ो, सामाजिक कुरीतियों, अनाचारों, पारस्परिक विरोधों आदि को दूर करने की अपूर्व शक्ति है। उसमें समाज के अन्तर्गत, क्रांति उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता है और उसमें चित्तवृतियों को परिमार्जित करके हद्वय को उदार बनाने की अनुपम साम्थर्य है। इस प्रकार कबीर का साहित्य जीवन को उन्नत बनाने वाला है, मानवतावाद का पोषक है, विश्वबंधुत्व की भावना को जाग्रत करने वाला है, विश्व प्रेम का प्रचारक है, पारस्परिक भेदभाव को मिटाने वाला है, तथा प्राणिमात्र में प्रेम का संचार करने वाला है। इसलिए कबीर अन्य सन्तों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रसिद्ध है वे एक महान साधक है, उच्चकोटि के सुधारक है, निर्गुण भक्ति के प्रबल प्रचारक है तथा हिंदी संतकाव्य के प्रतिनिधि कवि है। इसी कारण हिन्दी की संत काव्यधारा में उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
कबीर का काव्य आम आदमी का काव्य है। उन्होने समाज के विभिन्न वर्गों के परस्पर संबंधों, सामाजिक विसंगाति-विरोध के बीच सूत्रबद्धता, व्यक्ति और समाज के बीच सामजंस्य की भावना, आर्थिक विषमताओं को सहते हुए भी नैतिकता बनाए रखना, अभावजन्य परिस्थितियों में संतुलन सामाजिक एंव मानसिक विवश्ताओं को सहते हुए भी हीनता का अनुभव करना आदि बातों का सजीव आंकलन अपनी वाणी द्वारा किया है। समाज का यथार्थ वर्णन कबीर ने अपने साहसी और निर्भयतापूर्ण दृष्टिकोण द्वारा किया है। समाज में व्याप्त क्रूर और विषम वातावरण में भी कबीर अपना विरोध प्रकट करने का चारित्रिक साहस बनाए रहे:-
कबीर की साहसिकता एंव मौलिकता इस बात में है कि उन्होंने अपने अनुभूत सत्य की प्रतिष्ठा के लिए धार्मिक पांखड़, अधंविश्वास और संकीर्णताओं पर करारी चोट की। कबीर के समय में समाज अधोमुखी था। हिंदू-मुस्लमान आपस में सद्भाव से नहीं रहते थे। आए दिन दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। हिंदू अपनी परंपरागत सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सचेष्ट थे तो मुसलमान अपने को भारतीय समाज में एक प्रमुख स्थान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। रूढ़ियों, परंपराओं, आंडबरों और ढकोसलों के कारण समाज की जडें खोखली हो गई थी। इस समय कबीर अपनी पैनी दृष्टि से इन सबके क्रियाकलापों को बड़ी सावधानी से देख रहे थे। उन्हें जनता के शोषकों के ये व्यवहार नितांत निंदनीय प्रतीत होते थे। इसीलिए उन्होंने उनेक विरूद्ध निर्भीक होकर आवाज उठाई। यदि हम अपने आपको सुधार लें तो समाज में स्थित वर्ग या सप्रंदाय का प्रभुत्व स्वयमेव समाप्त हो जाएगा। इस संदर्भ मे उन्होंने कहा है :-
“बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय
जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई।।”(3)
कबीर ने समाज में व्याप्त जाँति-पाँति व ऊंच नीच की बड़े कड़े शब्दों में निंदा की है। वस्तुत: ऊंच नीच का भेद मिथ्या है, क्योंकि सारे जगत की उत्पत्ति पवन, जल, मिट्टी आदि पचंभूतों से हुई है। इनका स्रष्टा एक ही भ्रम है। सभी में एक ही ज्योंति समान रूप से व्याप्त है। केवल भौतिक स्वरूप के द्वारा नाम रूप का भेद है।
“जात पाँत पूछै न कोई
हरि को भजै सो हरि को होई।।”(4)
कबीर जी का मानना है कि धर्म सुधार से ही समाज का कल्याण हो सकता है, यही उनका लक्ष्य था इसलिए उन्होंने अपनी वाणी को समाज सुधारक के रूप में प्रस्तुत किया। कबीर छुआछूत जातिँ-पाँति के भेदभाव को अनर्गल प्रलाप मानते थे। छुआछूत का खण्डन करते उन्होंने कहा है:-
“ज्यों तू बामन बांमनी जाया
तौ आन बाट ह्ववै क्यों नहीं आया।।”(5)
कबीर ने समाज में व्याप्त धर्म के नाम पर जो विविध प्रकार के बाह्याचार प्रचलित थे, कबीर ने उनकी तीखी आलोचना की है। जहाँ उन्होंने एक ओर हिन्दु धर्म में प्रचलित जप, तप, छापा तिलक, वेदपाठ, तीर्थ-स्नान, अन्य कर्मकाण्डों की निस्सारता का उल्लेख किया है। वही दूसरी ओर मुस्लिम धर्मानुयाइयों को रोजा, नमाज तथा धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा की निंदा की है। कबीर ने हिंदु मुस्लमान दोनों की आडंबरवादी दृष्टि पर कुठाराघात किया है। उनका विचार है कि वे दोंनों ही अनेक आडंबरवादी दृष्टि के माध्यम से समाज को रोगी बनाने के दोषी है:-
“यह सब झूठी बदंगी, बिरथा पंच निवाज
साँचै मोरे झूठ पाढ़े, काजी करै कजाज।।”(6)
कबीर शास्त्र ज्ञान से अधिक महत्व प्रेम और भक्ति को देते थे। अत: काजी और पण्डित को फटकारते हुए कहा है :-
पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय,
ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।।(7)
बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुँच गए, पर सभी विद्वान न हो सके, कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले तो वही सच्चा ज्ञानी होगा।
कबीर ने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है कुछ लोगों के अनुसार क्योंकि वे मुसलमान जुलहा थे। उनके समय में मुसलिम शासकों द्वारा मूर्तियां तोड़ी जाती थी, इसलिए उन्होंने भी मूर्तिपूजा का तिस्कार किया। कबीर कहते है अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता है तो मैं तो पूरे पहाड़ को ही पूजने लग जाऊंगा।
“पाथर पूजे हरि मिलै, तो मैं पूजूँ पहार।
घर की चाकी कोउ न पूजै, जा पीसा खाए संसार।।”(7)
कबीर जी हिंसा का विरोध करते हैं। एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो कबीर को बहुत ही टीस होती है। वे उन्हें समझाते हुए कहते हैं –
बकरी पाती खात है, ताकी काठी खाल,
जो नर बकरी खात है, तिनको कौन हवाल।”(8)
कबीर ने गुरू को बहुत महत्व दिया है। उनकी अहम् प्रेरणा का मूल स्त्रोत उनके गुरू ही थे जिनकी कृपा से उन्होंने सभी संकीर्ण बन्धनों को तोड़ा, वे स्वतन्त्र-चिन्तक, उन्होंने बहुत-सी ज्ञानपूर्ण सच्चाईयों को सामान्य जन तक पहुँचाया, आत्म-ज्ञान प्राप्त करना, मूल सत्य से परिचित होना, इस सब कार्यों की प्रेरणा देने वाले उनके गुरू ही थे। वही इस मार्ग को बताने वाले थे।
“सतगुर की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार,
लोचन, अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार।।”(9)
कबीर ने नारी की निंदा की है। उन्होंने नारी को भक्ति के मार्ग में बाधा माना है। नारी को माया स्वरूप माना है:-
“नारी की झांई परै, अंधा होत भुजंग।
कबीर तिनकी कौन गति, जो नित नारी के संग।।”(10)
कबीर जी पूरे विश्व को एक कुटुम्ब मानते हैं। इसलिए वे पूरे विश्व का ही सुधार चाहते हैं –
“सीलवन्त सबसे बड़ा, सर्व रतन की खानि
तीन लोक की संपदा, रही सील में आनि।।”(11)
अतः हम कह सकते हैं कि कबीर अपने समय एवं समाज के कटु आलोचक ही नहीं समाज को लेकर स्वप्न द्रष्टा भी थे। उनके मन में भारतीय समाज का एक प्रारूप था जिस पर वे एक विजन के साथ काम कर रहे थे। “वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे। वे हिन्दू होकर भी हिन्दू नहीं थे। साधु होकर भी योगी नहीं थे, वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे।
निष्कर्ष :
संत कबीरदास जी के काव्य में सामाजिक चेतना पर्याप्त रूप से लक्षित होती है। उन्होंने अपने समय के समाज की विसंगतियाँ देखी और काव्य के माध्यम से उन पर कड़ा प्रहार किया। कबीर जितने प्रासंगिक आज है उतने भविष्य में भी रहेंगें क्योंकि उनकी वाणी ने जिन समस्याओं को इंगित किया वह मानव जीवन में सदा रहने वाली है।
संदर्भ :
- कबीर ग्रंथावली – रामकिशोर शर्मा, लोकभारती प्रकाशन, सांतवा संस्कंरण – 2008
- हिंदी कविता – आदिकालीन एंव भक्तिकालीन काव्य – हेमंत कुकरेती, सतीश बुक डिपो नई दिल्ली, 2015, पृष्ठ सं – 50
- कबीर – ऋतुश्री, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रथम संस्कंरण-जून 1978, पृष्ठ संख्या -141
- कबीर मींमासा – डाँ रामचन्द्र तिवारी, लोकभारती प्रकाशन, तृतीय संस्कंरण-1989, पृष्ठ सं – 135
- कबीर एक पुर्नमूल्यांकन – डाँ बलदेव वंशी, आधार प्रकाशन, 2006, पृष्ठ संख्या -123
- कबीर – ऋतुश्री, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रथम संस्कंरण-जून 1978, पृष्ठ संख्या-142
- कबीर ग्रंथावली – श्यामसुंदरदास
- कबीर ग्रंथावली – श्यामसुंदरदास
- श्यामसुन्दर दास,कबीर ग्रन्थावली, पृ सं -59
- श्यामसुन्दर दास,कबीर ग्रन्थावली, पृ सं -59
- डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर, पृ॰ 77-78