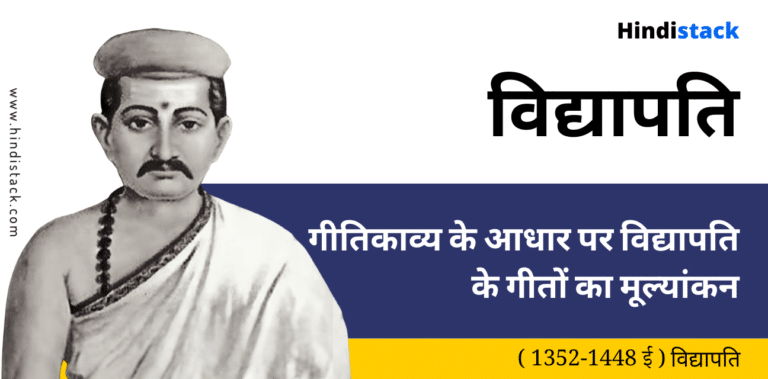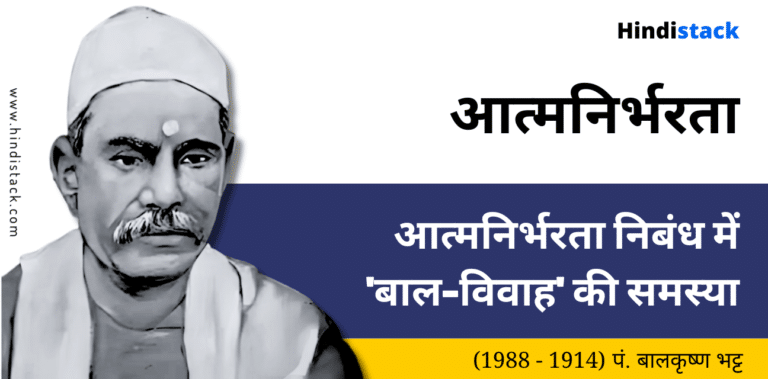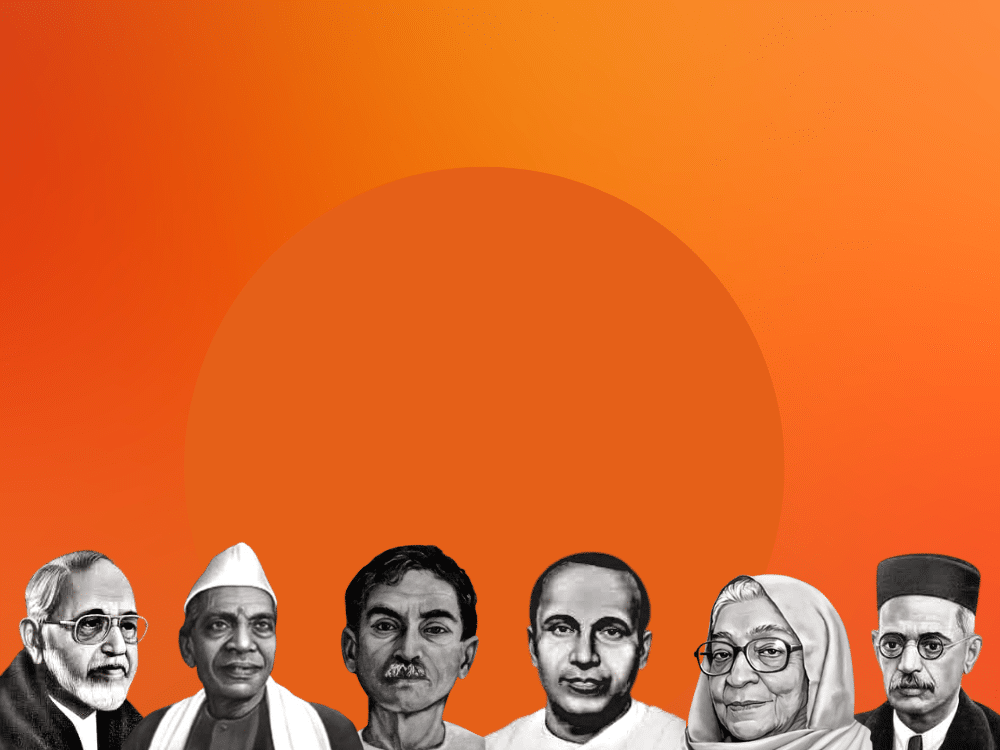फोर्ट विलियम कॉलेज (Fort William College) का हिंदी गद्य के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को कोलकाता में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने की थी। यह संस्था भारत में आने वाले ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं, संस्कृति, धर्म और प्रशासनिक ज्ञान से परिचित कराने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। इस कॉलेज ने संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि भाषाओं के अध्ययन और अनुवाद को बढ़ावा दिया। इसके माध्यम से हजारों पुस्तकों का अनुवाद किया गया, जिससे भारतीय भाषाओं और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला।
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना और उद्देश्य
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत में आने वाले ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं और संस्कृति से परिचित कराना था। इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित किया गया और विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का अनुवाद कराया गया। इस कॉलेज ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
हिंदी गद्य का विकास
फोर्ट विलियम कॉलेज ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस संस्था ने हिंदी गद्य को एक साहित्यिक माध्यम के रूप में स्थापित करने में मदद की। कॉलेज के अधीन काम करने वाले लेखकों और विद्वानों ने हिंदी गद्य में कई महत्वपूर्ण रचनाएँ लिखीं, जिनमें कहानियाँ, निबंध, और अनुवाद शामिल हैं। इन रचनाओं ने हिंदी गद्य को एक नई दिशा दी और इसे साहित्यिक मान्यता प्रदान की।
फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रभाव से हिंदी गद्य का विकास तेजी से हुआ। इसके बाद हिंदी गद्य ने धीरे-धीरे अपना स्थान साहित्य में बना लिया और आगे चलकर यह हिंदी साहित्य का एक प्रमुख अंग बन गया। इस कॉलेज ने हिंदी गद्य को एक व्यवस्थित और सुसंगत रूप प्रदान किया, जिससे हिंदी साहित्य का विकास संभव हुआ।
खड़ी बोली हिंदी का विकास
खड़ी बोली हिंदी का विकास भी फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रयासों से जुड़ा हुआ है। खड़ी बोली हिंदी, जो आधुनिक हिंदी का आधार है, को इस कॉलेज ने प्रोत्साहित किया। गिलक्रिस्ट और उनके सहयोगियों ने खड़ी बोली को एक साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने खड़ी बोली में व्याकरण और शब्दकोश तैयार किए, जिससे इस भाषा को मानकीकरण मिला।
खड़ी बोली हिंदी का विकास 19वीं शताब्दी में तेजी से हुआ। इसके बाद यह भाषा हिंदी साहित्य की प्रमुख भाषा बन गई और आधुनिक हिंदी साहित्य का आधार बनी। फोर्ट विलियम कॉलेज ने खड़ी बोली को एक साहित्यिक और प्रशासनिक भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
फोर्ट विलियम कॉलेज ने हिंदी गद्य और खड़ी बोली हिंदी के विकास में अहम भूमिका निभाई। इस संस्था ने हिंदी को एक साहित्यिक और प्रशासनिक भाषा के रूप में स्थापित करने में मदद की। गिलक्रिस्ट और उनके सहयोगियों के प्रयासों से हिंदी गद्य और खड़ी बोली हिंदी को मानकीकरण मिला, जिससे हिंदी साहित्य का विकास संभव हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज का योगदान हिंदी साहित्य के इतिहास में सदैव याद किया जाएगा।
विभिन्न संस्थाओं और पत्र-पत्रिकाओं का योगदान
फोर्ट विलियम कॉलेज के अलावा, हिंदी गद्य के विकास में विभिन्न संस्थाओं और पत्र-पत्रिकाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन संस्थाओं और पत्र-पत्रिकाओं ने हिंदी गद्य को एक नई दिशा दी और इसे साहित्यिक मान्यता प्रदान की।
स्कूल बुक सोसायटी
सन् 1803 ई0 में हिन्दी गद्य के विकास का सबसे अधिक लाभ ईसाई धर्म प्रचारकों ने उठाया। विलियम केरे और अन्य अंग्रेज पादरियों के प्रयास से ईसाई धर्म पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद हुआ। सिरामपुर प्रेस से ईसाई धर्म की पुस्तकें तो प्रकाशित हो ही रही थीं। धीरे-धीरे ईसाइयों के छोटे-छोटे स्कूल खुलने के साथ-साथ शिक्षा सम्बंधी पुस्तकें भी प्रकाशित होने लगीं। सन् 1833 ई0 में आगरा के पादरियों ने स्कूल बुक सोसायटी स्थापना की। जिसने सन् 1837 ई0 में इंग्लैंड के एक इतिहास का और सन् 1839 ई0 में मार्शमैन साहब के लिखे प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार नाम से पं0 रतन लाल ने किया। सन् 1855 ई0 से सन् 1862 ई0 के बीच मिर्जापुर के आरफान प्रेस से शिक्षा संबंधी पुस्तकें- भूचरित्र दर्पण, भूगोल विद्या, मनोरंजक वृतांत, जंतु प्रबंध, विद्यासागर, विद्वान संग्रह, आदि पुस्तकें प्रकाशित हुईं।
हिन्दी पत्र-पत्रिकायें
ईसाइयों के द्वारा हिन्दी गद्य का प्रचार-प्रसार तो अवश्य किया गया, लेकिन हिन्दी धर्म की स्थूल और बाहरी बातों जैसे- मूर्तिपूजा, तीर्थाटन, जाति-पाँति, छुआछूत, आदि का खंडन कर ही अपने ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। जिसके विरोध स्वरूप हिन्दुओं के शिक्षित वर्ग में स्वधर्म रक्षा की आकुलता उत्पन्न हुई। अतः राजा राम मोहन राय ने हिन्दू धर्म की कुरीतियों को दूर कर शुद्ध ब्रह्मोपासना का प्रवर्तन करने के लिये ब्रह्म समाज की नींव डाली। राजा राम मोहन राय ने सन् 1815 ई0 में वेदांत सूत्रों के भाष्य का हिन्दी में अनुवाद करके प्रकाशित कराया व सन् 1829 ई0 में बंगदूत नाम का संवाद पत्र भी हिन्दी में निकाला। राजा साहब की भाषा कुछ बँगलापन लिये हुये थी। 30 मई, सन् 1826 ई0 को पं0 जुगल किशोर(कानपुर) ने हिन्दी में उदन्त मार्तण्ड नामक समाचार पत्र निकाला, जो एक साल चलकर बंद हो गया।
उन्नीसवीं सदी से पहले अदालत की भाषा फारसी थी जिससे आम जनता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। सन् 1836 ई0 में अंग्रेजी सरकार ने इश्तहारनामे निकाले और अदालती कार्यवाही देश की प्रचलित भाषाओं में होने के आदेश दिये, मुसलमानों के घोर प्रयत्न करने के कारण दफ्तरों के कामकाज की भाषा फारसी के स्थान पर उर्दू हो गयी। ऐसी विपरीत परिस्थिति में राजा शिव प्रसाद जी का ध्यान हिंदी भाषा की ओर गया और हिन्दी भाषा के उत्थान के लिये प्रयत्नशील हुये। सन् 1845 ई0 में हिन्दी भाषा में काशी से बनारस अखबार प्रकाशित किया जिसकी भाषा उर्दू होते हुये भी लिपि देवनागरी थी। सन् 1850 ई0 में बाबू तारा मोहन मित्र ने सुधाकर नामक हिन्दी पत्र निकाला। सन् 1852 ई0 में मुंशी सदासुखलाल के प्रबंध व संपादन में बुद्धि प्रकाश निकला, जो कई वर्ष तक चलता रहा। इस प्रकार मुसलमानों के विरोध के बाबजूद उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिन्दी गद्य का विकास होने लगा और हिन्दी में अखबार निकलने लगे व पुस्तकें प्रकाशित होने लगीं.
6 मार्च, सन् 1835 ई0 को ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का प्रस्ताव पारित हो जाने से अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलने लगे. अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि हिन्दी भाषा को शिक्षा क्रम में शामिल किया जाये लेकिन सर सैय्यद अहमद के नेतृत्व में मुसलमान हिन्दी भाषा का विरोध कर अंग्रेजो को उर्दू भाषा की ओर झुकाने का प्रयत्न करते रहे. राजा शिवप्रसाद जी लगातार हिन्दी भाषा का समर्थन करते रहे. उर्दू भाषा और हिन्दी भाषा का झगड़ा भारतेन्दु युग तक चलता रहा.
सन् 1856 ई0 में राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुये. राजा साहब ने स्वयं पाठ्यक्रम के लिये उपयोगी कई कहानियाँ लिखीं जैसे- राजा भोज का सपना, वीरसिंह का वृतांत, आलसियों का कोड़ा, आदि. शिक्षा सम्बन्धी कई पुस्तकें लिखीं व अपने मित्रों पं0 श्रीलाल, पं0 बंशीधर, आदि को पुस्तकें लिखने के लिये प्रेरित किया. सन् 1852 ई0 से सन् 1862 ई0 के बीच अनेक शिक्षा संबंधी पुस्तकें प्रकाशित हुईं जैसे- पुष्प वाटिका(गुलिस्ताँ का अनुवाद), भारतवर्षीय अनुवाद, जीविका परिपाटी(अर्थशास्त्र की पुस्तक), जगत वृतांत,आदि. इन पुस्तकों की हिन्दी उर्दूपन लिये हुये थी.
सन् 1861 ई0 में राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से प्रजा हितैषी नाम का पत्र निकाला, जिसकी भाषा शुद्ध हिन्दी थी. शुद्ध और सरल हिन्दी में ही अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद प्रकाशित किया. हिन्दी गद्य के विकास में फ्रेडरिक पिंकाट का योगदान भी अविस्मरणीय है. फ्रेडरिक पिंकाट के संपादन में आईने सौदागरी(व्यापार पत्र) उर्दू भाषा में निकलता था जिसमें वह स्वयं हिन्दी भाषा में लेख लिखकर प्रकाशित करते थे और अन्य हिन्दी समाचार पत्रों जैसे- हिंदोस्तान, आर्य दर्पण, भारत दर्पण से उद्धरण भी प्रकाशित करते थे.
जिस प्रकार संयुक्त प्रांत(उत्तर प्रदेश) में राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में रहकर किसी न किसी प्रकार हिन्दी भाषा का विकास कर रहे थे उसी प्रकार पंजाब में नवीन चंद्र राय हिन्दी भाषा के विकास में अपना सहयोग दे रहे थे. मार्च, सन 1867 ई0 में ज्ञानदायिनी नाम से एक पत्रिका निकाली जिसमें शिक्षा संबंधी व साधारण ज्ञान के लेख प्रकाशित होते थे. सन् 1863 ई0 से सन् 1879 ई0 के बीच नवीन चंद्र राय नें हिन्दी भाषा में विभिन्न विषयों में हिन्दी में पुस्तकें तैय्यार कीं व ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के प्रचार के लिये कई पत्रिकायें निकालीं.
स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन् 1865 ई0 में आर्य समाज की स्थापना की और सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन हिन्दी भाषा में हुआ. आर्य समाज के प्रभाव से संयुक्त प्रांत के पश्चिमी जिलों और पंजाब में हिन्दी गद्य का प्रचार तेजी से हुआ. पं0 श्रद्धा राम फुल्लौरी ने भी हिन्दी भाषा में अनेक पुस्तकें लिखी. पं0 श्रद्धा राम फुल्लौरी ने सत्यामृत प्रवाह(सिद्धांत ग्रंथ) लिखा व सन् 1877 ई0 में भाग्यवती नामक एक सामाजिक उपन्यास लिखा.
राजा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी का प्रभाव हिन्दी भाषा और हिन्दी साहित्य दोनों पर ही बहुत अधिक है. भारतेन्दु जी के विषय में पं0 रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है- उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिन्दी साहित्य को भी नये मार्ग पर लाकर खड़ा किया और वे वर्तमान हिन्दी गद्य के प्रवर्तक माने गये. मुंशी सदासुख लाल की भाषा साधु होते हुये भी पंडिताऊपन लिये थी, लल्लूलाल में ब्रजभाषापन और सदलमिश्र में पूरबीपन था. राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक ही परिमित न था, वाक्यविन्यास तक में घुसा था, राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध और मधुर अवश्य थी, पर आगरे की बोलचाल का पुट उसमें कम न था. भाषा का निखरा हुआ शिष्ट सामान्य रूप भारतेन्दु की कला के साथ ही प्रकट हुआ.
भारतेन्दु जी ने हिन्दी साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे शिक्षित जनता के साहचर्य में हिन्दी को ले आये. भारतेन्दु जी ने स्वयं अनेक विधाओं में हिन्दी में रचना की और नये-नये विषयों की ओर अन्य लेखकों को भी प्रोत्साहित किया. आधुनिक हिन्दी गद्य साहित्य का प्रवर्तन नाटक विधा से हुआ. भारतेन्दु जी से पहले महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित आनंद रघुनंदन नाटक के अतिरिक्त कोई भी नाटक नाटकत्व गुणों से पूर्ण नहीं लिखा गया था. सन् 1868 ई0 में भारतेन्दु जी ने विद्या सुन्दर नाटक बँगला भाषा से अनुवाद कर लिखा, जिसमें हिन्दी गद्य का बहुत ही सुधरा हुआ रूप देखने को मिलता है. भारतेन्दु जी ने अपना मौलिक नाटक वैदिक हिंसा हिंसा न भवति लिखा. भारतेन्दु जी ने अनेक पत्र-पत्रिकायें निकालीं जैसे कवि वचन सुधा, हरिश्चन्द्र मैग्जीन, बाल बोधिनी. जिस हिन्दी को पूरे भारतवर्ष की जनता ने सहर्ष स्वीकार किया उसका रूप इन्हीं पत्रिकाओं में देखने को मिलता है. भारतेन्दु जी के समय के लेखकों में मौलिकता थी, इन्होंने अन्य भाषाओं(बँगला, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी) से अनुवाद नहीं किया जैसा कि बीस-पच्चीस साल पूर्व के लेखकों की रचनाओं में देखने को मिलता है. पं बद्रीनारायण चौधरी, पं0 प्रतापनारायण मिश्र, बाबू तोताराम, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, पं0 बालकृष्ण भट्ट, पं0 केशवराम भट्ट, पं0 अंबिकादत्त व्यास, पं0 राधाचरण गोस्वामी, आदि अनेक प्रौढ़ और प्रतिभाशाली लेखकों ने हिन्दी साहित्य के इस नूतन विकास में अपना योगदान दिया और विभिन्न प्रकार के गद्य प्रबन्ध, नाटक, उपन्यास, आदि लिखे.
हिन्दी गद्य के समुचित विकास का अनुमान भारतेन्दु जी के समय प्रकाशित होने वाली पत्र-पत्रिकाओं से चलता है-
अल्मोड़ा अखबार, (सन् 1871 ई0, सं0 पं0 सदानंद सलवास)
हिन्दी दीप्ति प्रकाश, (सन् 1872 ई0, कलकत्ता, सं0 कार्तिक प्रसाद खत्री)
बिहार बंधु, (सन् 1872 ई0, केशवराम भट्ट)
सदादर्श, (सन् 1874 ई0, दिल्ली, लाला श्रीनिवास दास)
काशी पत्रिका, (सन् 1876 ई0, बाबा बलदेव प्रसाद, शिक्षा संबंधी मासिक)
भारत बंधु, (सन् 1876 ई0, अलीगढ़, तोताराम)
भारत मित्र, (सन् 1877 ई0, कलकत्ता, रूद्रदत्त)
मित्र विलास, (सन् 1877 ई0, लाहौर, कन्हैयालाल)
हिन्दी प्रदीप, (सन् 1877 ई0, प्रयाग, बालकृष्ण भट्ट)
आर्य दर्पण, (सन् 1877 ई0, शाहजहाँपुर, मु0 वख्तावर सिंह)
सार सुधानिधि, (सन् 1878 ई0, कलकत्ता, सदानंद मिश्र)
उचित वक्ता, (सन् 1878 ई0, कलकत्ता, दुर्गा प्रसाद मिश्र)
सज्जन कीर्ति सुधाकर, (सन् 1879 ई0, उदयपुर, बंशीधर)
भारत सुदशाप्रवर्तक, (सन् 1879 ई0, फरूखाबाद, गणेश प्रसाद)
आनंद कादंबिनी, (सन् 1881 ई0, मिर्जापुर, बदरी नारायण चौधरी उपाध्याय)
देश हितैषी, (सन् 1881 ई0, अजमेर)
दिनकर प्रकाश, (सन् 1883 ई0, लखनऊ, रामदास वर्मा)
धर्म दिवाकर, (सन् 1883 ई0, कलकत्ता, देवीसहाय)
प्रयाग समाचार, (सन् 1883 ई0, देवकीनंदन त्रिपाठी)
ब्राह्मण, (सन् 1883 ई0, कानपुर, प्रतापनारायण मिश्र)
शुभ चिंतक, (सन् 1883 ई0, जबलपुर, सीताराम)
सदाचार मार्तंड़, (सन् 1883 ई0, जयपुर, लालचन्द शास्त्री)
हिंदोस्थान, (सन् 1883 ई0, इंग्लैंड, राजा रामपाल सिंह)
पीयूष प्रवाह, (सन् 1884 ई0, काशी, अंबिका दत्त व्यास)
भारत जीवन, (सन् 1884 ई0, काशी, रामकृष्ण वर्मा)
भारतेंदु, (सन् 1884 ई0, वृंदावन, राधाचरण गोस्वामी)
कविकुलकुंज दिवाकर, (सन् 1884 ई0, बस्ती, रामनाथ शुक्ल)
भारतेन्दु जी के समय लेखकों ने साहित्य निर्माण के साथ-साथ हिन्दी भाषा और नागरी अक्षरों की उपयोगिता के लिये भी सम्यक् प्रचार किया क्योंकि उस समय अदालतों की भाषा उर्दू थी और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सरकारी नौकरियों के योग्य बनाना था. अतः स्कूलों में या तो उर्दू की शिक्षा दी जाती थी या अंग्रेजी के साथ उर्दू की. स्वयं भारतेन्दु जी हिन्दी भाषा और नागरी अक्षरों की उपयोगिता समझाने के लिये बहुत से नगरों में व्याख्यान देने के लिये जाते थे. वे जहाँ जाते थे अपना यह मूलमंत्र अवश्य सुनाते थे,
निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।।
इसी प्रकार पं0 प्रताप नारायण मिश्र भी हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी का प्रचार करते थे. हिंदी प्रचार के लिये सभायें भी स्थापित हुईं. अलीगढ़ में बाबू तोताराम ने भाषा संवर्द्धिनी सभा की स्थापना की. सन् 1886 ई0 में प्रयाग में हिंदी उद्धरिणी प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई. सन् 1893 ई0 में बाबू श्याम सुंदर दास, पं0 राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह के सहयोग से काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई. नागरी प्रचारिणी सभा के दो मुख्य उद्देश्य थे- नागरी अक्षरों का प्रचार और हिन्दी साहित्य की समृद्धि. सन् 1895 ई0 में जब लॉर्ड मैकडानल काशी आये तो सभा ने उन्हें जनता की कठिनाईयों से परिचित कराया कि किस प्रकार सरकारी दफ्तरों में हिन्दी भाषा के प्रयोग के बिना जनता परेशान हो रही है. पं0 मदन मोहन मालवीय ने अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा नाम की एक अंग्रेजी पुस्तक लिखकर प्रकाशित की जिसमें नागरी लिपि को सरकारी दफ्तरों से दूर रखने के दुष्परिणामों का अनुसंधानपूर्ण विस्तृत वर्णन किया. सन् 1896 ई0 से नागरी प्रचारिणी पत्रिका प्रकाशित होने लगी जिसमें साहित्यिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक, आदि अनेक विषयों में लेख प्रकाशित होने लगे. काशी नागरी प्रचारिणी सभा का सबसे बड़ा कार्य हिन्दी का सबसे बड़ा और प्रामाणिक व्याकरण व शब्दकोश(शब्द सागर) का निर्माण है. भारतेन्दु जी के समय से चले रहे अथक प्रयासों के फलस्वरूप सन् 1990 ई0 में अंग्रेजी सरकार ने अदालती कार्यवाही के लिये नागरी लिपि को मान्यता दे दी.
भारतेन्दु जी के समय हिन्दी गद्य का बहुमुखी विकास तो हुआ लेकिन भाषा की शुद्धता व व्याकरण सम्बन्धी त्रुटियों की ओर लेखकों का अधिक ध्यान नहीं गया. द्विवेदी युग में हिन्दी भाषा की अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास किया गया व व्याकरण सम्बन्धी अनियमितता को दूर किया गया. सन् 1905 ई0 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हुये और उन्होंने लेखकों का ध्यान भाषा की शुद्धता की ओर दिलाया. सरस्वती पत्रिका में जो भी लेख प्रकाशित होते थे उन्हें वे स्वयं ठीक करते थे. उस समय हिन्दी भाषा में विभक्तियों को लेकर भी लेखक काफी असमंजस में थे कि विभक्तियाँ शब्दों से मिलाकर लिखी जायें या अलग से. पं0 गोविंद नारायण मिश्र ने विभक्ति-विचार नाम की एक छोटी सी पुस्तक लिखी व हिन्दी भाषा की शुद्ध विभक्तियों को बताकर उन्हें शब्दों के साथ मिलाकर लिखने की सलाह दी. जिसे सभी लेखको ने सहर्ष स्वीकार किया. वाक्य-विन्यास में अधिक स्पष्टता आई. विराम चिह्नों का आवश्यक प्रयोग होने लगा. अंग्रेजी, बँगला, आदि अन्य समुन्नत भाषाओं की उच्च विचारधारा से परिचित और अपनी भाषा पर भी यथेष्ट अधिकार रखने वाले लेखकों की कृपा से हिन्दी भाषा की अर्थोद्घाटिनी शक्ति की अच्छी वृद्धि हुई और अभिव्यंजन प्रणाली का समुचित विकास हुआ. हिन्दी भाषा सघन और गुंफित विचार सूत्रों को व्यक्त करने तथा सूक्ष्म व गूढ़ भावों को अभिव्क्त करने में समर्थ हुई. धीरे-धीरे हिन्दी साहित्य का स्तर ऊँचा उठने लगा. आज हिन्दी भाषा में सभी विषयों- विज्ञान, तकनीकी, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, आदि में पुस्तकें लिखी जा रही हैं.
विमल कुमार
आज हम लोग जिस हिंदी को बोलते सुनते हैं और जिस में साहित्य का सृजन करते हैं, उस हिंदी की कहानी कोलकाता के एक कालेज से हुई थी जिसका नाम फोर्ट विलियम कॉलेज था। वह हिंदी का पहला घर था।तब किसी ने कल्पना नही की होगी कि कालांतर में हिंदी के कई घर बनेंगे और पहले घर को ही भूल जाएंगे।।सौ साल बाद काशी नागरी प्रचारिणी सभा हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसे अनेक घर बने।अनेक पत्रिकाएं और प्रकाशन गृह भी हिंदी के घर ही थे जो उन्नीसवीं और बीसवीं सदी में बने।
आज से 220 साल पहले हमारी हिंदी का क्या स्वरूप था और हमारी हिंदी कैसे विकसित हुई और किन किन नामों से गुजरी किस किस तरह के विमर्श हुए उसका पहला लेखा-जोखा अगर कहीं मिलता है तो यह फोर्ट विलियम कॉलेज ही था, लेकिन दुर्भाग्य है कि हिंदी पट्टी में इस कॉलेज की चर्चा बहुत कम है या नहीं के बराबर है या यह कालेज हिंदी साहित्य के इतिहास में दबकर रह गया है ।
आज से 220 साल पहले हमारी हिंदी का क्या स्वरूप था और हमारी हिंदी कैसे विकसित हुई और किन किन नामों से गुजरी किस किस तरह के विमर्श हुए उसका पहला लेखा-जोखा अगर कहीं मिलता है तो यह फोर्ट विलियम कॉलेज ही था, लेकिन दुर्भाग्य है कि हिंदी पट्टी में इस कॉलेज की चर्चा बहुत कम है या नहीं के बराबर है या यह कालेज हिंदी साहित्य के इतिहास में दबकर रह गया है ।
लार्ड वेलेजली द्वारा अट्ठारह सौ में स्थापित उस कॉलेज का महज 54साल का इतिहास रहा लेकिन इन 5 दशकों में इस कॉलेज ने कई ऐतिहासिक कार्य किये और इतने उतार-चढ़ाव देखे और इस तरह की चुनौतियों का सामना किया कि उसकी कहानी को दर्ज करना बहुत आसान नहीं है। हिंदी सहित्य के पुराने इतिहासकार लक्ष्मी शंकर वार्ष्णेय ने एक जमाने में इस कॉलेज पर एक किताब लिखी थी लेकिन आज खुद वार्ष्णेय जी हिंदी की दुनिया से विस्मृत कर दिए गए हैं और अब उन्हें केवल शोधार्थी ही जरूरत पड़ने पर यदा-कदा पढ़ते हैं। ऐसे में उनकी इस कॉलेज पर लिखी गई किताब के बारे में आज हिंदी वाले कम ही जानते हैं ।युवा शोधार्थी शीतांशु ने बड़ी मेहनत से इस कॉलेज पर एक शोध ग्रंथ लिखा है ।अगर यह शोध ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा गया होता तो उसे हाथों हाथ लिया जाता लेकिन हिंदी में लिखे जाने के कारण यह किताब हिंदी वालों के बीच भी उपेक्षित और अलक्षित रह गई ।
उनकी पुस्तक 2018 में ही आई थी लेकिन इन 2 वर्षों में शायद ही किसी पत्र पत्रिका में इस पर कोई समीक्षा नजर आई हो या हिंदी आलोचना के समुदाय में इस पर कोई विशेष चर्चा या गोष्ठी हुई हो लेकिन यह किताब न केवल इस कॉलेज पर शोध ग्रंथ है बल्कि वह हिंदी के आरंभिक निर्माण कार्य के 50 सालों का एक दस्तावेज भी है जिसमें औपनिवेशिक काल मे ब्रिटिश प्राच्यवाद हिंदी हिंदुस्तानी प्रसंग ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति की एक झांकी भी पेश की गई है। इसके स्रोत सीधे राष्ट्रीय अभिलेखागार से लिए गए हैं जो अब तक हिंदी की दुनिया को प्राप्त नहीं थे ।इससे इस किताब का महत्व और बढ़ जाता है और यह किताब अत्यंत प्रमाणिक हो जाती है। शीतांशु के एम.फिल. का शोध कार्य इसी कालेज पर था और हिंदी के प्रख्यात मार्क्सवादी आवश्यक नामवर सिंह ने उन्हें इस काम को अंजाम देने का जिम्मा सौंपा था।
शीतांशु ने इस किताब के बहाने सर विलियम जॉन से लेकर जान गिल क्रिस्ट जेम्स मोअट, जान विलियम टेलर, कप्तान विलियम प्राइस तक की विस्तृत चर्चा है और यह बताने का प्रयास किया है कि लॉर्ड मैकाले के आने से पहले अंग्रेजों की भाषा नीति और शिक्षा नीति क्या थी तथा भारत में सांस्कृतिक ज्ञान और प्राच्यवाद के प्रति बढ़ते अंग्रेजों के आकर्षण के पीछे क्या राजनीतिक निहितार्थ थे लेकिन केवल इन राजनीतिक आशयों के कारण हिंदी के विकास में इस कॉलेज का योगदान कम नहीं हो जाता।
शीतांशु ने इस किताब के बहाने सर विलियम जॉन से लेकर जान गिल क्रिस्ट जेम्स मोअट, जान विलियम टेलर, कप्तान विलियम प्राइस तक की विस्तृत चर्चा है और यह बताने का प्रयास किया है कि लॉर्ड मैकाले के आने से पहले अंग्रेजों की भाषा नीति और शिक्षा नीति क्या थी तथा भारत में सांस्कृतिक ज्ञान और प्राच्यवाद के प्रति बढ़ते अंग्रेजों के आकर्षण के पीछे क्या राजनीतिक निहितार्थ थे लेकिन केवल इन राजनीतिक आशयों के कारण हिंदी के विकास में इस कॉलेज का योगदान कम नहीं हो जाता ।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में जरूर कॉलेज के दो मुंशियों सदल मिश्र और लल्लू लाल की चर्चा की है यह चर्चा जितनी अपेक्षित थी वह शुक्ल नहीं कर पाए हैं। शायद उनका तब जोर हिंदी के उस पूरे इतिहास लिखने का था और उसमें सारे परिदृश्य को पेश करने का प्रयास था लेकिन फिर भी फोर्ट विलियम कॉलेज के योगदान को देखते हुए उनसे अपेक्षा बनती है कि वह इस काम को अगर और विस्तार देते तो शायद आज हिंदी को लेकर चर्चा कुछ और ही होती पर इस कमी को बाद में वार्ष्णेय ने पूरा किया।रामविलास शर्मा ने जरूर भारतेंदु और हिंदी नवजागरण तथा भाषा और समाज जैसी पुस्तकों की रचना के क्रम में फोर्ट विलियम कॉलेज के कार्य को रेखांकित किया है और हिंदी हिंदुस्तानी की शुरुआत से पहले उस पूरे प्रदेश में चल रहे विमर्श को रेखांकित करने की कोशिश की है।
शीतांशु ने इस किताब को केवल एक कॉलेज के विकास के रूप में नहीं बल्कि औपनिवेशिक कॉल के टूल के रूप में तथा अंतर संबंधों और उस दौर में भाषा नीति को लेकर भी विचार बस किया है ।उन्होंने अपनी भूमिका में यह स्पष्ट कर दिया है कि इस संस्थान के संदर्भ में हिंदी जगत में अनेक प्रकार के मत विवाद और भ्रांतियां मिलती हैं जैसे कि एक तरफ अगर यह मान्यता है कि हिंदी भाषा की दृष्टि से कॉलेज कोई विशेष योगदान न दे सका तो दूसरी तरफ यह मान्यता है कि कॉलेज द्वारा प्रस्तुत कृतियों और उसकी भाषा नीति से हिंदी साहित्य की दशा और दिशा प्रभावित हुई ।एक तरफ अगर यह मान्यता है कि प्रेम सागर एक अत्यंत उबाऊ और निम्न कोटि की रचना है तो दूसरी तरफ यह कि प्रेम सागर(लल्लू लाल) हिंदी साहित्य का अमूल्य कृति है और इतिहास ग्रंथों में उसका अवमूल्यन किया गया है।
लेखक ने इस किताब के पहले अध्याय में ही यह स्पष्ट कर दिया है इस कॉलेज की स्थापना भारतीय इतिहास के उस मोड़ पर हुई थी जो परंपरा से एक ऐसे विच्छेद का दौर है जिससे भारतीय समाज संस्कृति राजनीति धर्म दर्शन कृषि व्यापार आदि के चरित्र को बदल कर रख दिया ।यह वह दौर है जब स्वयं ईस्ट इंडिया कंपनी को भी इंग्लैंड में आकार ले रहे गंभीर आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों का सामना करना पड़ रहा था ।
लेखक ने इस किताब के पहले अध्याय में ही यह स्पष्ट कर दिया है इस कॉलेज की स्थापना भारतीय इतिहास के उस मोड़ पर हुई थी जो परंपरा से एक ऐसे विच्छेद का दौर है जिससे भारतीय समाज संस्कृति राजनीति धर्म दर्शन कृषि व्यापार आदि के चरित्र को बदल कर रख दिया ।यह वह दौर है जब स्वयं ईस्ट इंडिया कंपनी को भी इंग्लैंड में आकार ले रहे गंभीर आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों का सामना करना पड़ रहा था ।
लेखक का यह मानना है कि जब विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना के पीछे नियत कार्य को पर विचार किया जाता है तो वहां भी अंततः राजनीतिक आर्थिक बर्ताव से उपजे सुगठित प्रशासनिक ढांचे की जरूरत या समाजवादी आकांक्षाओं पर ही बातें केंद्रित होकर रह जाती हैं जबकि कहानी कुछ और ही है ।इस कहानी की शुरुआत विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना वर्ष के समय औपनिवेशिक सत्ता के चारित्रिक विकास को एक बार फिर समझे बगैर नहीं हो सकती क्योंकि वह समय है जब औद्योगिक पूंजीवाद अपने पैर पसार रहा था और व्यापारिक पूंजीवाद का इंग्लैंड की राजसत्ता से गठबंधन टूटा नहीं था ।
लेखक ने कुल 5 अध्याय में पुस्तक को समेटा है। इसमें पहला अध्याय सत्य ज्ञान और संस्थान, दूसरा अध्याय” कंपनी का व्यापारिक चरित्र और फोर्ट विलियम कॉलेज” तीसरा अध्याय “कंपनी और कॉलेज की भाषा नीति का फर्क” तथा चौथा अध्याय “हिंदी उर्दू एक बार फिर और पांचवा अध्याय “हिंदी साहित्य की परंपरा की चिंता इसके बाद ” है।उन्होंने करीब 10 पेज का एक उप संहार भी लिखा है और एक परिशिष्ट भी दिया। शीतांशु ने इस पुस्तक का नायक विलियम जॉन्स और जॉन गिलक्रिस्ट को बनाया है लेकिन उन तमाम अन्य विदेशी भारत विदों की चर्चा की है और कॉलेज के जो जो प्राचार्य रहे हैं उनके योगदान को रेखांकित किया है।इतना ही नहीं इस संस्थान से प्रकाशित पुस्तकों की एक सूची भी पेश की है और उसमे कार्यरत मुंशियों का भी जिक्र किया है । गिलक्रिस्ट के महज 5 साल के कार्यकाल में 28 ग्रंथ तैयार किये गए जिनमे लल्लू लाल और सदल मिश्र की किताबों के अलावा दसेक मुस्लिम लेखक भी थे। लल्लू लाल ने सिहांसन बत्तीसी से लेकर शकुंतला नाटक और लालचन्द्रि का भी शामिल है।
लेखक ने सर विलियम जॉन्स के बारे में लिखते हुए बताया है कि उन्हें ग्रीक रोमन फ्रेंच स्पेनिश इतालवी चीनी संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। मनुस्मृति, हितोपदेश, महाभारत, ऋग्वेद, कालिदास, जयदेव, भारतीय प्राचीन संगीत, भारतीय प्रकृति दर्शन, पुराण, ज्योतिष, बीजगणित, नाट्यशास्त्र, मोहम्मद फिरदौसी, खुसरो, निजामी के संदर्भ में उन्हें विस्तृत जानकारी भी थी और इस जानकारी का उन्होंने अंग्रेजी में उपलब्ध कराया था ।जोन्स ने हिंदुस्तान के प्राचीन तत्वों को परखा। उनकी छानबीन की और यूरोपीय बौद्धिकों के सामने भारतीय इतिहास के श्रेष्ठ तत्वों को स्थापित किया ।भारतीय साहित्यकारों और इतिहासकारों ने इस विकास से प्रेरणा ग्रहण की ।
सर जॉन शोर ने विलियम जॉन्स पर केंद्रित अपने व्याख्यान में कहां है “ज्ञान और सत्य उनके संपूर्ण अध्ययन के अभिप्रेत थे और उनका लक्ष्य मनुष्य के लिए उपयोगी होना था। इस दृष्टि से उन्होंने अपने अध्ययन का विस्तार सभी भाषाओं देश और काल के लिए किया। विलियम जोंस ने तो हिंदू धर्म के देवी-देवताओं कामदेव, प्रकृति, दुर्गा भवानी, सूर्य, लक्ष्मी-नारायण, सरस्वती, गंगा को आधार बनाकर लंबी कविताएं भी लिखी हैं, फारसी संस्कृत अध्ययन किया था। उन्होंने संदर्भ ग्रंथ भी दिए हैं। जोंस के बाद चार्ल्स विलिकिन्स एच.टी. कोलब्रुक भी ऐसे ही भारतविद थे।
पुस्तक के अनुसार फोर्ट विलियम कॉलेज के पाठ्यक्रम में जो ग्रंथ शामिल किए गए थे उसमें शकुंतला नाटक, बेताल पच्चीसी, तूती नामा, गुलिस्ता, श्रीमद्भागवत, पुराण, प्रेमसागर, चंद्रावती की पुस्तकें। विषयों के चुनाव की दृष्टि से उन पर भी ब्रिटिश सांसद की छाप महसूस की जा सकती है।
लेखक के अनुसार इस कॉलेज में 1835 तक इसके पुस्तकालय में यूरीपीय विभाग में 5224 पुस्तकें प्राच्य शाखा में 11718 प्रकाशित पुस्तकें और 4225 पांडुलिपियां थी ।आज भी राष्ट्रीय अभिलेखागार में इस कॉलेज से जुड़ी 199 पांडुलिपियां और 742 पुस्तकें उपलब्ध हैं। इस से अनुमान लगाया जा सकता है इस कॉलेज का कितना बड़ा योगदान था।
लेकिन कालांतर में कम्पनी और कॉलेज की भाषा नीति में फर्क और कॉलेज के विभागाध्यक्षों के नजरिये में फर्क के कारण कालेज में खींचतान शुरू हुई और छात्रों की अनुशासनहीनता के कारण यह कालेज 1854 में बन्द हो गया। इस कॉलेज का बंद होना हिंदी के लिए बड़ी दुर्घटना थी लेकिन इस कॉलेज पर भाषायी विभेद और भाषायी सम्प्रदायिकता के बीज बोने के आरोप लगे। कहा गया कि हिंदी उर्दू के झगड़े भी शुरू हुए। अगर शीतांशु औपनिवेशि और पूंजीवाद के आईने में देखने के साथ-साथ भारत मे राष्ट्रवाद के विकास के बरअक्स इस किताब को लिखते तो तस्वीर सुर प्यूरी हो जाती दरअसल कम्पनी ने इस कालेज में दिलचस्पी लेना भी कम कर दिया और लार्ड मैकाले के बाद तो पूरा परिदृश्य ही बदल गया।इसके पीछे ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति काम कर रही थी। 1857 की क्रांति के बाद तो इस कॉलेज के फिर से खुलने का सवाल ही नही उठता था।इस हिंदी का यह पहला घर और चमकने की जगह बिखर गया ।उसके बाद भारतेंदु, सितारे हिन्द, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी का अपना घर बनाया।