सूर काव्य में भ्रमरगीत का अपना अलग स्थान है। भ्रमरगीत सूरसागर के भीतर का एक सार रत्न है। भ्रमरगीत नौसिखिए सूर की रचना नहीं है अपितु, एक अनुभवी महात्मा और महान प्रतिभाशाली कवि की रचना है। अनेक वर्षो तक भक्ति सागर में गोता लगाने एवं विस्तृत संसार का सूक्ष्म निरीक्षण करने के पश्चात सांसारिक लोगों को निर्गुण के कंटकाकीर्ण मार्ग से बचकर उन्हें भक्ति का विशद राजमार्ग दिखाने के लिए ही भ्रमरगीत की रचना की गई है। ज्ञान की कोरी वचनावली और योग की थोथी साधनावली का यदि साधारण लोगों में विशेष प्रचार हो तो अव्यवस्था फैलने लगती है। निर्गुण पंथ ईश्वर की सर्व व्यापकता भेदभाव की शून्यता सब मतों की एकता आदि लेकर बढ़ा जिस पर चलकर अनपढ़ इतना ज्ञान की अनगढ़ बातों और योग के टेढ़े-मेढ़े अभ्यासों को ही सब कुछ मान बैठी तथा दंभ अहंकार आदि दु:वृतियों से उलझने लगी। ज्ञान का कहकहा भी न जानने वाले लोग उसके पारंगत पंडितो से मुँह जोरी करने लगे । अज्ञान से जिनकी आँखे बंद थी वे ज्ञान-चक्षुओं को आँख दिखाने लगे जैसे तुलसी के मानस में यह लोक विरोधी धारा खटकी वैसे ही सूर की आँखो में थी। तुलसी ने स्पष्ट शब्दों में और कड़ाई से इसका परिहार करने की ठानी। प्रबंध का क्षेत्र चुनने से उन्हें इसके लिए विस्तृत भूमि मिल गई I पर गीतो में सूर ने इसका प्रतिवाद प्रत्यक्ष नही प्रच्छन्न रूप से किया। उन्होंने उद्धव प्रसंग में ‘भ्रमरगीत’ के भीतर इसके लिए स्थान निकाला । उद्धव के योग और ज्ञान का जो प्रतिकार गोपियों ने “सूरसागर” में किया वह सूर की योजना है।
ज्ञान और योग की साधना भली न हो, सो नही। वस्तुत: वह कठिन है, सामान्य विद्या बुद्धि वालों की पहुँच से परे है। पक्ष में उद्धव ऐसे ज्ञान वरिष्ठ पुरुष और विपक्ष में ब्रजवासिनी ऐसी ज्ञान-कनिष्ठ स्त्रियों को खड़ा करके सूर ने ज्ञान एवं योग का प्रतिरोध साधारण जनता की दृष्टि से किया। ज्ञान की ऊँची तत्वचिंता उनके लिए नहीं। ज्ञानयोग के प्रतिपक्ष में प्रेमयोग का मंडन करके यह प्रत्तिपन्न किया गया है कि भक्ति की भी वही चरमावधि है जो ज्ञान की –
“अहो अजान। ज्ञान उपदेशत ज्ञानरूप हमहीं
निशिदिन ध्यान सूर प्रभु को अलि ! देखत जित तुतहीं”
सूर ने ज्ञान या योग मार्ग को संकीर्ण, कठिन और नीरस तथा भक्ति मार्ग को विशाल, सरल और सरस कहा है। ज्ञान तथा योग का अभ्यासी विश्व की विभूति से अपनी वृत्ति समेटकर अंतर्मुख हो जाता है। इसलिए गुह्य रहस्य एवं उलझन की वृद्धि होती है। पर भक्ति का अनुरागी बहिर्मुख हो जाता है। इसलिए गुह्य रहस्य एवं उलझन की वृद्धि होती है। पर भक्ति का अनुरागी बहिर्मुख रहता है। वह जगत के ऊर्जस्वित रूपों में अपनी वृत्ति रमाए रहता है। उसके लिए सब कुछ सुलझा हुआ है। इस प्रकार भक्ति का मार्ग चौड़ा, निष्कंटक और सीधा है। उसमें गोपन, रहस्य या उलझाव कहीं नही –
“काहे को रकत मारग सूधो। सुनहु मधुप ! निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रूँधो।।”
यो तो संपूर्ण सूर-साहित्य पर भागवत की स्पष्ट छाया है। किंतु एक महान कवि के अनुरूप उन्होंने प्रत्येक स्थल को अपनी प्रतिभा के रंग में रंगकर मौलिक बना डाला है। भ्रमरगीत का प्रसंग भागवत में भी आया है किंतु अत्यंत संक्षेप में है और उसका उद्देश्य भी सूर के भ्रमरगीत से भिन्न है। भागवत के अनुसार कृष्ण राजनैतिक कारणों से जो एक बार मथुरा जाते हैं तो फिर वहाँ की राजनीति में इतने विंध जाते है कि फिर लौट नहीं पाते। कृष्ण के ब्रज आने की अवधि जब समाप्त हो जाती है तो संपूर्ण ब्रज उन्हें विरह में आकुल व्याकुल होने लगता है। गोपियाँ विशेष रूप से व्यथित हैं। गोपियों की विरह व्यथा को शांत करने अथवा कम करने के लिए श्री कृष्ण अपने ज्ञानी सखा उद्धव जी को ब्रज भेजते है। उद्धव वहाँ जाकर अपने ज्ञान मार्ग का प्रसार करते हैं और ब्रजवासियों को समझाते हैं कि कृष्ण परब्रह्म के अवतार है। व्यक्ति नहीं है इसलिए कृष्ण का मोह छोड़कर सबको निराकार ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए क्योकि वह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वान्तरयामी है। सूर ने भ्रमरगीत के द्वारा निर्गुण का खंडन किया है और साकारोपासना का समर्थन या प्रसार किया है। भ्रमरगीत में उद्धव की पराजय, ज्ञानमार्ग की पराजय और निर्गुण का खंडन तथा भक्ति और सगुणोपासना की विजय दुदुंभी ही है। यह स्मरणीय है कि सूर ने तीन भ्रमरगीतों की रचना की है।
- पहला भ्रमरगीत भागवत का उल्था मात्र है जिसमें ज्ञान वैराग्य आदि की ही अधिक चर्चा है किन्तु जहाँ भी सूर को अवसर मिला है उन्होंने ज्ञान की महत्ता बढ़ाने का प्रयत्न किया है। यह भ्रमरगीत चौपाई छन्द में लिखा गया है। इस भ्रमरगीत से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रारंभ से ही सूर का दृष्टिकोण भागवत से भिन्न है।
- दूसरा भ्रमरगीत पदों में रचा गया है। पहले भ्रमरगीत और इसमें भ्रमर के आने की चर्चा नहीं है। मधुकर नाम से ही उद्धव पर व्यंग्य किए गए हैं।
- तीसरे भ्रमरगीत की रचना भी पदों में ही हुई किन्तु वह दो अन्य भ्रमरगीतों से अधिक विस्तृत काव्यपूर्ण एवं आकर्षक है। इसमें पहली बार भ्रमर उड़कर आता है उस समय जब उद्धव गोपियों से बात का रहे हैं और गोपियाँ उसी भ्रमर के माध्यम से उद्धव और कृष्ण पर व्यंग्य बाणों की वर्षा करने लगती हैं। सूर का यही भ्रमरगीत हिन्दी साहित्य का गौरव है, और उसकी अक्षय निधि है।
इस भ्रमरगीत में सूर ने खुले शब्दों में निराकार का खंडन और साकार का मंडन किया है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के द्वारा प्राप्त अपरिमित ज्ञान की सूर इस भ्रमरगीत में साहित्यिक या काव्यात्मक अभिव्यक्ति दे सके हैं। सूर के इस भ्रमरगीत में पहली बार सूर के भक्ति विषयक विचार स्पष्ट रूप से सामने आते है। इसी प्रकार यदि सूर चाहते तो बिना ज्ञानमार्ग की निंदा किए केवल सगुण भक्ति की विजय दिखाकर ज्ञान और योग की हीनता प्रदर्शित कर सकते थे, पर उन्हें यह पसंद नही था। इसलिए सगुण भक्ति के प्रचारक के रूप में उन्होंने भ्रमरगीत में निर्गुण का निर्मम विरोध किया है और गोपियों के समक्ष ज्ञान के प्रतीक उद्धव की पराजय दिखाकर उन्होंने सगुण भक्ति की पताका ही ऊँची रखी है।
ज्ञान के प्रतीक उद्धव अपने ह्रदय में अपार साहस और मस्तिष्क में ज्ञान का अपार दंभ लेकर आए थे कि जाते-जाते गोपियों की आस्था सगुण भक्ति से हटाकर निर्गुण में कर सकेंगे। वे केवल अपनी ही बात सोचकर ब्रज में आए थे जैसे दूसरे पक्ष के पास कहने योग्य कुछ सामग्री ही नहीं है और फिर भोली-भाली गोपियाँ उनके ज्ञान को चुनौती देंगी। इसकी कल्पना तो उन्होने स्वप्न में भी न की होगी। उद्धव ब्रज में आकर अपना भाषण प्रारंभ करते हैं और गोपियों को बताते हैं कि तुम सब लोग अभी तक भ्रम में पड़ी हुई हो, सबका आराध्य तो निर्गुण ब्रह्म ही है जिसके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह वर्णनातीत है, उसका केवल अनुभव ही किया जा सकता है विश्लेषण नहीं। जिस श्रीकृष्ण को तुम प्रेम करती हो, वे ब्रह्म के ही प्रतीक हैं। उनका बाह्य रूप मिथ्या है। जिससे तुम प्रेम करती हो, इस प्रकार के प्रेम से तो तुम्हारा चित्त अस्थिर और अज्ञात ही रहेगा। सच्ची शांति प्राप्त करने के लिये योग का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। योग में दक्षता प्राप्त करने के लिए कुछ शारीरिक साधनाओं की अपेक्षा है जो साधारण कठिनाई के पश्चात संभव हो सकेगी। उद्धव ने समझा था कि उनका भाषण इतना सारगर्भित, विचारोत्तेजक और मार्मिक है कि किसी को उनके ज्ञान और योग के प्रवचन पर शंका नहीं हो सकती है। यह उनके लिए कल्पनातीत बात थी। किंतु अचानक एक गोपी खड़ी हो गई और अपनी शंका को उसने इस सीधे-साधे शब्दों में प्रकट किया –
“हे अलि क्या जोग में नीको। तजि रस रीति नंदनंदन की सिखवत निर्गुण फीको।”
उद्धव यह अप्रत्याशित प्रश्न सुनकर भौचक्के रह गए। ये मूर्ख गोपियाँ निराकार ब्रह्म को चुनौती देने लगी, यह तो बड़ी असह्य बात है। अभी उद्धव इस अप्रत्याशित बात से अपना पीछा भी नहीं छुड़ा पाए थे कि एक और गोपी खड़ी हो गई। उसे उद्धव के ज्ञान पर भी शंका है। वह उद्धव से प्रश्न करती है कि क्या आपने निर्गुण ब्रह्म का दर्शन किया है ?
“रेख न रूप बरन नहिं जाके, ताको हमें बतावत। अपनी कहो दरस वैसे को तुम कबहूँ हो पावत ?”
उद्धव निरुत्तर हो गए। उद्धव ने देखा कि ऐसे काम नहीं चलेगा तब उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने सोचा कि इस मंडली में कृष्ण के नाम पर कोई बात कही जाए तब तो ये सुनेंगे भी नहीं तो सुनने को भी तैयार नहीं हैं। अंततः उन्होने गोपियों को विश्वास दिलाया कि ये बाते मेरी मनगढंत नहीं हैं अपितु तुम्हारे प्रियतम कृष्ण का संदेश है। वे चाहते हैं कि आपके विरह का दुख किसी प्रकार कम हो और मेरे द्वारा प्रचारित संदेश से ही ऐसा संभव हो। अब गोपियाँ जरा चक्कर में पड़ गई, वे कृष्ण के संदेश की अवहेलना तो नहीं कर सकती थी। परंतु अचानक एक गोपी की समझ में सब रहस्य आ गया। जरूर इसे कुब्जा ने भेजा है, यह उसी का भेदिया है। वह चाहती है कि हम सब कृष्ण की ओर से विमुख हो जाए और कृष्ण सदैव मथुरा में ही बने रहे उसने तुरंत उठकर यह घोषित कर दिया-
“मधुकर कान्ह कही नहि होही। यह तो नई सखी सिखई है, निज अनुराग वरोही। सचि राखी कूबरी पीठि पै ये बातें चकचोंही”
उद्धव ने बिगड़ती हुई परिस्थिति को संभालने की लाख चेष्टा की, बौद्धिक स्तर पर गोपियों को समझाने का अनन्त प्रयत्न किया किन्तु असफल रहे। लाख प्रयत्नों के बावजूद वे गोपियों में ज्ञान के प्रति आकर्षण नही जगा सके। परंतु उद्धव भी अपनी पराजय को स्वीकारना उचित नहीं समझते थे, उन्होंने सोचा कि ये गोपियाँ तो स्री जाति की हैं इसलिए मेरे ज्ञान गाम्भीर्य की थाह नहीं पा रही हैं। मेरा कर्तव्य तो उन्हें उचित मार्ग बताना ही है, यह सोचकर उद्धव ने फिर योग का संदेश देना प्रारंभ किया। शास्त्रो में योग स्रियों के लिए वर्जित है यह बात उद्धव स्वयं ज्ञान के उमंग में आकर विस्मृत कर जाते हैं तब गोपियाँ उन्हें उनकी भूल उन्हें बताती हैं और कहती हैं कि उद्धव तुम तो इतने बड़े मूर्ख हो कि यह भी नहीं जानते कि योग की बातें अबलाओं के लिए वर्जित हैं।
“अटपटि बात तिहारी ऊद्धौ, सुनै सो ऐसी को है।
हम अहीर अबला सठ मधुकर। तिन्हे योग कैसे सोहै।।”
उद्धव के बार-बार समझाने पर गोपियाँ कहती हैं कि ऐ उद्धव आप अपनी यह ज्ञान चर्चा संभाल कर रखे रहें, इसे ले जाकर मथुरा की नागरी स्रियों को बताना क्योंकि वे ही इसकी कीमत ठीक ढंग से जाँच सकेंगी और आपकी सफलता का मान वहीं पर होगा। जिस प्रकार मछली को जीने के लिए पानी को छोड़कर और कोई उपाय नहीं है उसी प्रकार हम अबलाओं को कृष्ण चर्चा के अलावा अन्य चर्चा प्राण घातक भी हो सकती है।
“हमको हरि की कथा सुनाव।
अपनी ज्ञान कथा हे उद्धौ। मथुरा ही लै जाव।
नागरि नारि भले बूझेगी अपने वचन सुझाव।
पा लागों, इन बातीन रे अलि। उनहीं जाय रिझाव।।”
गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारा प्रेम केवल वासना की तृप्ति के लिए नहीं अपितु उसमें सतीत्व की दृढ़ और निश्चल भावना है। कली कली का रस चखने वाले बहुरंगी इस प्रेम के महत्त्व को नही समझ सकते। जिन्हे इस पवित्र प्रेम की अनुभूति नहीं हुई, वे तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिर उद्धव के ज्ञान-उपदेश से तंग आकर गोपियाँ साफ कह देती हैं। उद्धव जी। आप योग अपने पास रखिए उसका हम क्या करेंगी ? हम तो अपना सर्वस्व पुंडरीकाक्ष श्याम सुंदर को जो नंद और यशोदा के प्यारे है, को अर्पण का चुकी हैं। जो कुछ भी तन मन था वह तो कृष्णार्पण हो गया अब निर्गुण हेतु हमारे पास कुछ भी शेष नहीं है। उपदेश के लिए पहली बात आचरण है और फिर उपदेश देना जरूरी है क्योंकि बिना आचरण के उपदेश में प्रभाव नहीं होता है। श्रोता लोग पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिं ते नर न घनेरे कहके आचरण तीन उपदेश को की बात उड़ा दिया करते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियों ने भी उद्धव की कथनी तथा करनी की ओर संकेत करके उनके उपदेश की निस्सास्ता का प्रतिपादन किया है-
“याकी सीख सुनै ब्रज को रे ?
जाकी रहनि कहनि अनमिल, अलि कहत समुझि अति थोरे।।
धान को गाँव पयार तें जानो ज्ञान विषय रस भोरे।
सूर सो बहुत कहै न रहे रस गूलर को फल फोरे ।।”
जब उद्धव की ज्ञान चर्चा बंद नहीं होती और गोपियों को उनकी कही बाते बेसिर-पैर की गलती है जिनका कुछ स्पष्ट अर्थ नहीं जान पड़ता, तब वे ऊबकर झुंझला उठती हैं और कहती है कि ज्ञान को छोड़कर अज्ञात के प्रति आग्रह करना मूर्खता है। हमारा सगुण ज्ञात है और तुम्हारा निर्गुण अज्ञात। इसी प्रसंग में गोपियाँ उद्धव से कहती है कि आप अपने निर्गुण का रूप रंग,अता-पता और उसके इष्ट रसो का वर्णन करो ताकि हम उसे जानकर अपने भली-भाँति परिचित प्रियतम से उसकी तुलना कर सके-
“निर्गुण कौन देस को बासी ?
मधुकर। हँसि’ समुझाय, सौं हं दे बूझति साँच न हाँसि।।
को है जनक, जननि को कहितय, कौन नारि को दासी।
पावौंगे पुनि कियो आपनो जो रे कहों गे गाँसी।
कैसो बरन भेस है कैसो केहि रस में अभिलासी।
दाख छुहारा छाँडि अमृत फल विषकारा विष खात।।
सुनत् मौन हवे तह्यौ ठग्यौ सो सूर सने मति नासी।।”
भक्ति के बिना ज्ञान और कर्म व्यर्थ है, इस तथ्य को द्योतित करने के लिए सूरदास जी ने एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत उपस्थित किया है। उनका कथन है कि जिस प्रकार पतंग दीपक से प्रेम करता है और उसकी दिप्त शिखा से भी न डरता हुआ उस पर गिर पड़ता है उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी अपने ज्ञान रूप दीपक से सांसारिक दु:ख कूप को प्रकट देखता हुआ भी उसमें गिर जाता है। जड़ जंतु कालरूपी व्याल के रजस्तमोमय विषानल में क्यों जलता है ? वह अगम सिंधु को पार करने के यत्नों की नौका सजाकर उसे कर्मो के भार से भरता है, परंतु सूर का व्रत तो यही है कि मनुष्य कृष्ण भक्ति के द्वारा ही इस भवसागर को पार का सकता है। सूरदास जी के भक्ति विवेचन से ज्ञान होता है कि वल्लभ के मिलन से पहले उनका मन स्थिर नहीं था इसीलिए वे घिघियाते भी थे। यही कारण है कि उनके भक्ति विवेचन में उत्तरोत्तर निश्चित रूप से अंतर प्रतीत होता है। निर्गुण पंथ के प्रति प्रारंभ में उनकी सहिष्णुता उदासीनता में परिणत होती हुई भ्रमरगीत प्रसंग में पूर्ण विरोध के रूप में फूट निकली प्रेमी भक्त को प्राप्त का लेने के पश्चात् और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता उनकी गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं,
“हमारे मन में कोई स्थान अवशिष्ट नहीं है। हमारा हृदय तो कृष्ण के प्रेम से लबालब भरा है।”
“मन दस बीस तो होते ही नही।”
प्रिय के असाधारण गुणो पर ही रीझकर प्रेम होता हो ऐसी बात नहीं है। उससे भी अधिक गुणवान वस्तु क्यों न हो पर वह प्रेमी के ह्रदय को नहीं लुभा सकती। वह प्रेम की अनन्यता है जो सूर की गोपियों में देखी जा सकती है जिसे प्रेम भक्ति का नाम दिया गया है-
“उद्धव मन माने की बात।
सूरदास जाको मन जासो ताको सोई सुहात।।”
अंततः गोपियाँ समझ लेती हैं कि उद्धव योग की भाषा के अतिरिक्त और कोई भाषा ही नहीं समझते। तब वे योग की भाषा का ही आश्रय लेती हैं और उद्धव को बताती हैं कि हम तो पहले से ही योग साधना कर रही हैं। प्रेम ही हमारा तप भी है, योग भी है और भक्ति भी है, दुख-सुख को हमने जीत लिया है। मान-अपमान से हम ऊपर हैं। प्रेम की कठिन अग्नि में हमने अपनी सब इच्छाएं होम का दी हैं। कृष्ण के विरह में हम पंचाग्नि साधन का रही है। अब तुम्ही बताओ हमसे बड़ा योगी कौन होगा –
“हम अलि गोकुलनाथ अराध्यौ मन, वच, क्रम, हरि सौं धरि पतिव्रत, प्रेम जोग तब साध्यौ।। मुरली अधर स्रवन धुनि सो सुनि अनहद शब्द प्रमाने, बरसत रस रुचि बचन संग सुख पद आंनद समाने।। मंत्र दियो मन जात भजन लगि ज्ञान ध्यान हरि ही को, सूर कहौ गुरु कौन करै अलि कौन सुनै मति फीको।।”
आखिर ज्ञान मल्ल उद्धव ब्रज के अखाड़े में चारों कौने चित्त गिरे सो भी गोपियों के द्वारा। गोपियों की कठिन विरहग्नि से उद्धव का ब्रज हृदय भी पिघल गया। उद्धव पूर्ण रूप से पराजित होकर लौटे लेकिन उनकी यह पराजय भी उनकी बहुत बड़ी जीत थी क्योंकि इसके द्वारा उनके हाथ एक ऐसा रसायन लगा जो कि ब्रह्मानंद सदृश था। मथुरा जाकर कृष्ण के सामने उद्धव ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें ज्ञान और योगमार्ग की पराजय की स्पष्ट घोषणा तथा सगुण और प्रेम भक्ति की विजय दुदुंभी है –
“माधव यह ब्रज को त्योहार। मेरा कह्यौ पवन को भुस भयौ, गावत नंदन कुमार।।”
उद्धव ने ब्रज प्रयाण करते समय समझा था कि कृष्ण सचमुच ज्ञान मार्ग के समर्थन हैं किन्तु उद्धव को हृदय परिवर्तन देख कृष्ण भी खुल पड़े और बोले हे उद्धव मेरी भी बड़ी बुरी दशा है, ज्ञान ध्यान की ये बाते तो कोरा मजाक थी और फिर आप के ज्ञान गर्व की परीक्षा भी होनी थी। मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ कि मानस की वास्तविक शांत के लिए ज्ञान मार्ग उपयुक्त नहीं है, उसके लिए उचित रास्ता तो भक्ति का ही है, अंत में सूर कृष्ण के मुख से निम्नाकिंत पद कहलाकर भक्ति मार्ग की विजय घोषणा दिगदिंगत में कर देते हैं-
“ऊधौ मोहि ब्रज विसरत नाहीं। हंत सुता की सुंदर कगरी, उतरू कुंजन की छाहीं।”
इस प्रकार अपने भ्रमरगीत में महाकवि सूर ने एक ओर तो सगुण भक्ति का उत्कर्ष निर्गुण भक्ति की तुलना में दिखाया है ओर दूसरी ओर हृदय की कोमलतम वृत्तियाँ भी इस भ्रमरगीत में चरमतम रूप में व्याप्त हैं जो ‘भ्रमरगीत’ प्रसंग को हिन्दी की अमूल्य निधि बना देती है।









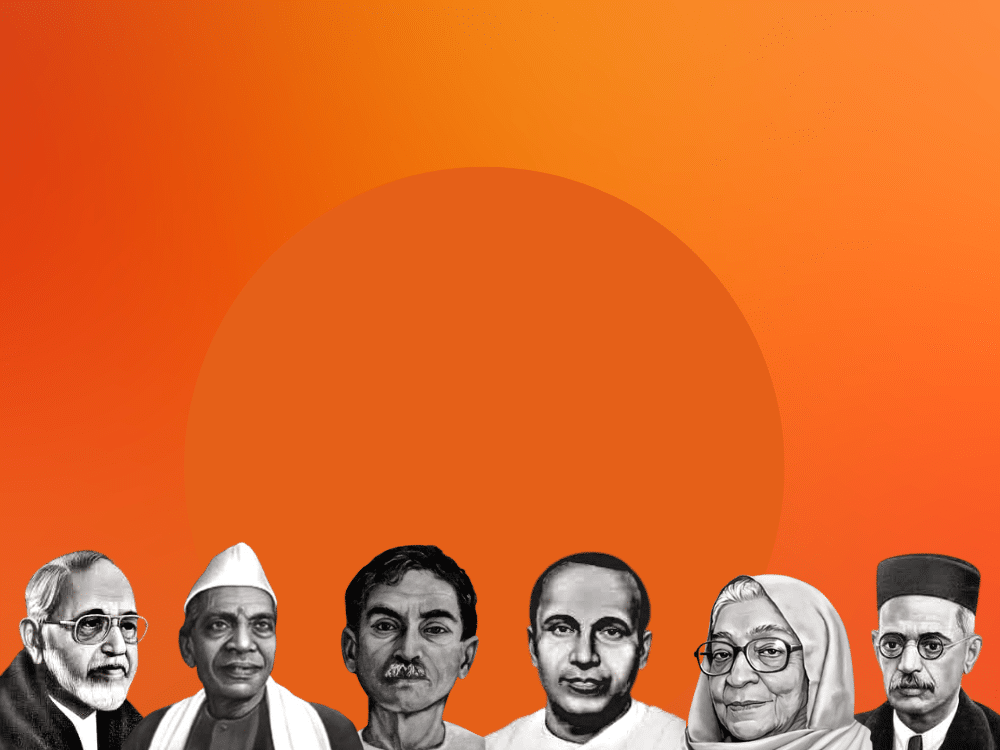

One Response
Soordas ke bhramargeeth ke udheshy