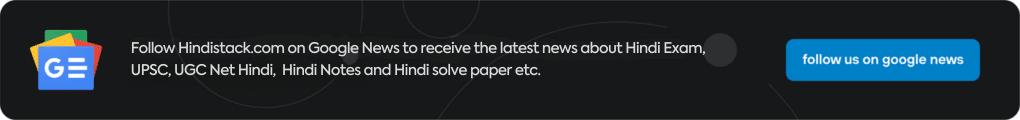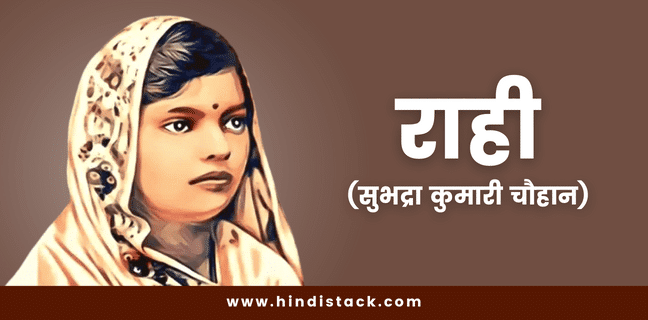हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन कब और कहाँ से आरम्भ हुआ? यह हिंदी साहित्य से जुड़े इतिहासकारों व विद्वानों के लिए एक दिलचस्प सवाल रहा है। यूँ तो हिंदी साहित्य के इतिहास को समेटने व संवारने का काम काफी पहले से अप्रत्यक्ष रूप से होता आ रहा है, लेकिन इस लेखन को इतिहासपरक दृष्टि से मुकम्मल करने का काम बहुत बाद में प्रारम्भ हुआ था। ‘डॉ रामकुमार वर्मा’ के शब्दों में कहना ही उचित होगा कि
“हिन्दी के निर्माणकाल के समय (लगभग सं०700) से विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक हिन्दी साहित्य का इतिहास बिखरी हुई रत्न-राशि के समान पड़ा रहा ; उसके संग्रह करने का प्रयास किसी के द्वारा नहीं हुआ।” (हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास : डॉ रामकुमार वर्मा , (विषय-प्रवेश), पृष्ठ संख्या : 1)
इन इतिहासकारों की कड़ी मेहनत व अथक परिश्रम के कारण जहाँ कई इतिहास ग्रन्थ रचे गए वहीं दूसरी ओर कई इतिहास ग्रन्थ समय समय पर सामने भी आए , जिसके परिणामस्वरूप हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की एक सुदीर्घ परंपरा आज हमारे सामने मौजूद हो पाई है। इतिहास लेखन की इस सुदीर्घ परंपरा को दो रूपों में बांट कर समझा जा सकता है :
- अनौपचारिक
- औपचारिक
[the_ad_placement id=”hindistack-feed-ads”]
अनौपचारिक हिंदी साहित्य
हिंदी साहित्य के इतिहास को अनौपचारिक तरीके से लिखने की शुरुआत 19वीं शताब्दी के पहले हो चुकी थी। लेकिन ये इतिहास ग्रन्थ ठीक तरीके से इतिहास की कसौटी पर नहीं ठहरते क्योंकि इनमें काल-क्रम , सन-संवत, विषय-वस्तु का विवेचन न के बराबर है। लेकिन इनमें हिन्दी के रचनाकारों का विवरण पर्याप्त मात्र में था इसलिए इन्हें वृत्त संग्रह कहना ही ठीक होगा। हिंदी साहित्य के प्रमुख अनौपचारिक इतिहास ग्रन्थों का विवरण इस प्रकार है–
भक्तमाल
● यह कृति ‘नाभादास’ जी की है।
● इस कृति का समय 1585 ई. है।
● इसमें 108 छप्पय छंदों में अन्य भक्तों सहित ‘रामानंद’ के 12 शिष्यों का भी वर्णन मिलता है।
मूल गोसाईं चरित
● यह कृति ‘बेणी माधोदास’ की है।
● इस कृति का समय 1630 ई. है।
● इसमें दोहा , चौपाई , त्रोटक छंदों में ‘गोस्वामी तुलसीदास’ का जीवन चरित्र लिखा गया है।
चौरासी वैष्णव की वार्ता
● यह कृति ‘गोकुलनाथ’ जी की है।
● इस कृति का समय 1640 ई. है।
● इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों की जीवन-कथाओं को संकलित किया गया है।
● इस ग्रन्थ की अंतिम चार वार्ताएँ यानी वार्ता संख्या 81 से 84 तक ‘अष्टछाप’ से संबंधित हैं, जैसे :
1. वार्ता संख्या 81 में ‘सूरदास’ के जीवन वृत्त एवं कवित्व का परिचय मिलता है।
2. वार्ता संख्या 82 में ‘परमानंददास’ के जीवन वृत्त एवं कवित्व का परिचय मिलता है।
3. वार्ता संख्या 83 में ‘कुंभनदास’ के जीवन वृत्त एवं कवित्व का परिचय मिलता है।
4. वार्ता संख्या 84 में ‘कृष्णदास’ के जीवन वृत्त एवं कवित्व का परिचय मिलता है।
[the_ad_placement id=”hindistack-feed-ads”]
दो सौ बावन वैष्णव की वार्ता
● यह कृति ‘गोकुलनाथ’ जी की है।
● इस कृति का समय 1640 ई. है।
● इसमें विट्ठलनाथ के शिष्यों की जीवन-कथाओं को संकलित किया गया है।
● इस ग्रन्थ की आरम्भिक चार वार्ताएँ यानी वार्ता संख्या 1 से 4 तक ‘अष्टछाप’ से संबंधित हैं, जैसे
1. वार्ता संख्या 1 में ‘गोविंद स्वामी’ की जीवन-कथा दी गई है।
2. वार्ता संख्या 2 में ‘छीतस्वामी’ की जीवन-कथा दी गई है।
3. वार्ता संख्या 3 में ‘चतुर्भुजदास’ की जीवन-कथा दी गई है।
4. वार्ता संख्या 4 में ‘नंददास’ की जीवन-कथा दी गई है।
भक्त नामावली
● यह कृति ‘ध्रुवदास’ जी की है।
● इस कृति का समय 1641 ई. है।
● इसमें 116 भक्तों का संक्षिप्त वर्णन है।
कविमाला
● यह कृति ‘तुलसी’ जी की है। ये राम भक्ति शाखा के ‘तुलसीदास’ से भिन्न हैं।
● इस कृति का समय 1655 ई. है।
● इसमें 75 कवियों की कविताओं का संग्रह है।
काव्य निर्णय
● यह कृति ‘भिखारीदास’ जी की है।
● इस कृति का समय 1705 ई. है।
● इसमें काव्य के आदर्शों के साथ साथ अनेक कवियों का निर्देश किया गया है।
कालिदास हजारा
● यह कृति ‘कालिदास त्रिवेदी’ जी की है।
● इस कृति का समय 1718 ई. है।
● इस रचना में 212 कवियों की 1000 कविताओं का संग्रह किया गया है।
[the_ad_placement id=”hindistack-feed-ads”]
औपचारिक हिन्दी साहित्य
उन्नीसवीं शताब्दी से हिन्दी साहित्य के इतिहास पर औपचारिक रूप से विचार-विमर्ष शुरू हुआ। यहाँ पर इतिहासकारों व विद्वानों के लिए इसे शब्दबद्ध करना ही एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि तब महत्वपूर्ण यह नहीं था कि हिन्दी साहित्य का इतिहास बड़े विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक तरीके से हमारे सामने आए बल्कि तब महत्वपूर्ण यह समझा गया कि हिन्दी साहित्य का इतिहास कम से कम इतिहास रूप में तो हमारे सामने हो , और काफी समय बाद यह संभव हो सका कि हिन्दी के कवियों का परिचयात्मक ही सही पर एक क्रम में उन्हें संजोने की कोशिश की गई और यह कोशिश अंधकार में पड़े हिंदी साहित्य के इतिहास को मशाल दिखाने से कम नहीं थी। यह निर्विवाद रूप से आज हमारे सामने है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को औपचारिक रूप से लिखने की पहली शुरुआत फ्रेंच विद्वान ‘तासी’ ने की थी। जिसे आगे चलकर ग्रियर्सन , आचार्य शुक्ल जैसे बड़े इतिहासकारों ने एक नई दिशा दी और यह परंपरा आज भी गतिमान है। जिसके कारण हिंदी साहित्य के इतिहास-ग्रन्थों का भी अपना एक इतिहास है जैसे –
1. इस्त्वार द ला लितरेत्युर एन्दुई एन्दुस्तानी
इतिहासकार ‘गार्सा-द-तासी’
● ‘तासी’ फ्रेंच विद्वान होते हुए भी भारतीय भाषाओं में गहरी रूचि रखते थे। ये काफी समय तक पेरिस विश्विद्यालय में उर्दू के प्राध्यापक रहे थे और इनका उर्दू और हिंदी भाषा पर विशेष ध्यान था।
● सर्वप्रथम इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को फ्रेंच भाषा में प्रस्तूत किया और इनके इतिहास ग्रन्थ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास होने का गौरव प्राप्त है।
● तासी का यह ग्रन्थ दो भागों में प्रस्तुत किया गया था। पहला सन् 1839 में और दूसरा सन् 1847 में। लेकिन इसके द्वितीय संस्करण में जो सन् 1871 में प्रकाशित हुआ था। उसमें इसके तीन भाग कर दिए गए और पहले संस्करण की अपेक्षा इसमें वृद्धि भी की गई।
● गार्सा द तासी ने “इस्तवार द ल लितरेतयूर ऐदुई ए हिंदुस्तानी” नामक इतिहास फ्रांसीसी भाषा में लिखा। गार्सा द तासी का यह ग्रंथ कालक्रमानुसार न होकर कवियों के वर्णानुक्रम से है, कालक्रमानुसार इतिहास की पहली शर्त है और वर्णानुक्रम का प्रयोग शब्दकोश में होता है। डॉ लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद “हिंदुई साहित्य का इतिहास” नाम से किया है।
ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की ओरियन्टल ट्रांसलेशन सोसायटी ने इस ग्रन्थ को प्रकाशित किया था। कवियों का वर्णन अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया है इसमें कुल 738 कवि / लेखक हैं जिनमें हिंदी के सिर्फ 72 हैं। नलिन विलोचन शर्मा ने इसे हिंदी का प्रथम साहित्येतिहास ग्रन्थ माना है । मूल्यांकन–त्रुटिपूर्ण परन्तु प्रथम महत्वपूर्ण प्रयास।
[the_ad_placement id=”hindistack-feed-ads”]
2. “तबकाशुअरा” या “तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी” इतिहासकार ‘मौलवी करीमुद्दीन’ नामक ग्रंथ लिखा जो सन 1848 में दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित हुआ।इस ग्रंथ में 1004 कवियों का उल्लेख है जिसमें केवल 60-62 हिंदी के कवि हैं। तासी ने अपने ग्रन्थ के द्वितीय संस्करण हेतु इसका प्रयोग किया । मौलवी करीमुद्दीन – साहित्येतिहास लिखने वाले प्रथम भारतीय (दिल्ली के) पुस्तक – ”तजकिरा-ई-शुअरा-ई-हिंदी” (तबकातु शुआस) प्रकाशन – 1848 में दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित कुल कवि / लेखक – 1004 हिंदी के कवि – 62 कवियों के जन्म-मरण के संवत, वैयक्तिक जीवन की झलक, काव्य संग्रह के वर्णन में आंशिक सफलता । चंद बरदाई, अमीर खुसरो, कबीर , जायसी, तुलसी आदि के कालक्रम का भी चिन्तन किया
3. शिव सिंह सेंगर ने ‘शिवसिंह सरोज’ की रचना की जो प्रथम बार सन 1878 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुई। शिवसिंह सरोज के पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने संग्रहित है, इसमें कवियों का उल्लेख अकारादि क्रम से है। उत्तरार्ध भाग में 1003 कवियों का जीवन परिचय अकारादि क्रम से दिया गया है। इसमें 687 कवियों की तिथियां भी दी गई है 263 कवियों की तिथियां नहीं है और 53 कवि विद्यमान कहे गए हैं। शिवसिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। शिवसिंग सेंगर पुस्तक शिवसिंह सरोज प्रथम संस्करण– 1878, द्वितीय संस्करण– 1883 (कालिदास हजारा पर आधारित) प्रकाशन – नवलकिशोर, लखनऊ से इस ग्रन्थ को हिंदी साहित्येतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है (पूर्णतय विश्वसनीय न होने के बावजूद)। हिंदी की जड़ की खोज करते हुए कवि पुंड तक पहुंचा गया है। कवियों को शती अनुसार अलग-अलग रखा गया है। उत्तरार्द्ध में 1003 कवियों के जीवन चरित अकारादि क्रम से, 687 कवियों की तिथियाँ दी गई हैं।
[the_ad_placement id=”hindistack-feed-ads”]
4. डॉक्टर ग्रियर्सन ने ‘मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दन हिंदुस्तान’ के लेखन में सर्वाधिक सहायता शिवसिंह सरोज से ली गई है 951 कवियों में से 886 कवि शिवसिंह सरोज से लिए गए हैं। केवल 65 कवि अन्य स्रोतों से लिए गए हैं। इस रचना का प्रकाशित समय 1888 हैं। डॉ. सर जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन – पुस्तक – ”द माडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ़ हिन्दुस्तान” प्रकाशन – 1888 (एशियाटिक सोसायटी ऑफ़ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में) (शिवसिंह सरोज का ऋण स्पष्टत: स्वीकार किया है) भाषा–अंग्रेजी विषय – केवल हिंदी के कवि हिन्दुस्तान से अभिप्राय हिंदी भाषा-भाषी प्रदेश। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसमें न तो संस्कृत-प्राकृत को शामिल किया गया है न ही अरबी-फ़ारसी मिश्रित उर्दू को। (इस प्रकार यह स्पष्टत: हिंदी से संबंधित इतिहास ग्रन्थ है) 952 कवियों का वर्गीकरण कालक्रमानुसार करते हुए उनकी प्रवृतियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास। काल विभाजन का प्रयास (12 अध्याय, प्रत्येक अध्याय एक काल का द्योतक , दोषपूर्ण लेकिन प्रथम महत्वपूर्ण प्रयास) अनेक विद्वानों ने इसे हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रन्थ स्वीकार किया। इनमें डॉ. किशोरीलाल गुप्त प्रमुख हैं । देन– चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य , दरबारी काव्य के रूप में हिंदी साहित्य को बांटना। भक्तिकाल को पन्द्रहवीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण कहना। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग (भक्तिकाल) को हिंदी का स्वर्णयुग मानना।
5. पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, तीनों सगे भाई थे और मिश्रबंधु नाम से रचना करते थे मिश्र बंधुओं ने ‘मिश्रबंधु विनोद’ नामक हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास तीन भागों में प्रकाशित करवाया I पहले तीन भाग 1913 में प्रकाशित हुए इसका चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ इसमें कुल मिलाकर 4591 कवियों का और लेखकों का विवरण है I इस रचना का प्रकाशित वर्ष 1883 हैं I मिश्र बन्धु – तीन भाई – प. गणेश बिहारी मिश्र डॉ. श्याम बिहारी मिश्र डॉ. शुकदेव बिहारी मिश्र पुस्तक – ”मिश्रबन्धु विनोद” (चार भाग) प्रकाशन – प्रथम तीन भाग -1913 चौथा भाग (काल) – 1914 ”हिंदी नवरत्न” – मिश्र बन्धु विनोद के प्रथम तीन भागों का पूरक 4591 कवियों का जीवन वृतांत संग्रहित। आचार्य शुक्ल – ”कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय: मिश्रबन्धु विनोद से ही लिए हैं ।” स्थान-स्थान पर काव्यांग विवेचन तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए कवियों की श्रेणियां बनाने का प्रयास देव-बिहारी विवाद को जन्म दिया जो अगले दस वर्षों तक चर्चा का विषय रहा।
[the_ad_placement id=”hindistack-feed-ads”]
6. रामचंद्र शुक्ल ने पहले नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित “हिंदी शब्दसागर की भूमिका” के रूप में “हिंदी साहित्य का इतिहास” लिखा था जो बाद में जनवरी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सेंगर और डॉ ग्रियर्सन के साहित्यिक ग्रंथों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है।
7. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल – पुस्तक – ”हिंदी साहित्य का इतिहास“ 1928 – नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित ” हिंदी शब्द सागर ” की भूमिका में ” हिंदी साहित्य का विकास ” के रूप में प्रकाशित । 1929 – स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1940 – संशोधित और प्रवर्धित संस्करण मूल विषय को आरंभ करने से पूर्व ही संवत 1050 से संवत 1984 तक के 900 वर्षों के इतिहास को सुस्पष्ट चार भागों में विभाजित किया है।
8. डॉ . रामकुमार वर्मा – पुस्तक – ”हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास“ इसका प्रकाशन 1938 ई. में हुआ और इसमें 1693 ई. तक के काल को सात प्रकरणों में प्रस्तुत किया है– संधिकाल, चारणकाल, भक्तिकाल की अनुक्रमणिका, भक्ति काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, प्रेम काव्य। इसमें शुक्ल की मान्यताओं को दोहरया। आदिकाल को दो भागों में बांटा– संधिकाल और चारणकाल।
[the_ad_placement id=”hindistack-feed-ads”]
9. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी – पुस्तक – हिंदी साहित्य की भूमिका (1940) मुख्य रूप से इतिहास ग्रन्थ न होते हुए भी कई इतिहास ग्रन्थों से अच्छा (पहला ग्रन्थ जिसमें साहित्य के विभिन्न स्वरूपों के विकास का विराट रूप से वर्णन) परम्परा को महत्व दस अध्याय – हिंदी साहित्य, भारतीय चिन्तन का स्वभाविक विकास, संत मत, भक्तों की परम्परा, योग मार्ग और संत मत, सगुण मतवाद, मध्ययुग के संतों का स्वाभाविक विकास, भक्तिकाल के प्रमुख कवियों का व्यक्तित्व, रीतिकाल, उपसंहार। परिशिष्ट में संस्कृत संबंधी अध्ययन द्विवेदी जी के अन्य प्रमुख ग्रन्थ– हिंदी साहित्य: उद्भव एवं विकास हिंदी साहित्य का आदिकाल (व्याखान ग्रन्थ) कबीर और नाथ संप्रदाय कबीर द्विवेदी जी आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं व स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित करने वाले पहले व्यक्ति हैं।
10. डॉ. गणपतिचन्द्र गुप्त– वर्ष 1965 ई० में डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त ने साहित्येतिहास की धरातल पर स्वरचित ‘हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास’ प्रस्तुत किया। इस ग्रन्थ में सम्पूर्ण इतिहास को तीन कालों- प्रारम्भिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित किया गया है। इसमें डॉ० गुप्त ने साहित्येतिहास के विकासवादी सिद्धान्तों की प्रतिष्टा करते हुए, उसके आलोक में हिन्दी साहित्य की नई व्याख्या प्रस्तुत करने की चेष्टा की है।
वर्ष 1986 ई० में डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ‘हिन्दी साहित्य और संवेदना का विकास’ नामक ग्रन्थ की रचना की। डॉ. चतुर्वेदी मूलतः आचार्य ‘रामचन्द्र शुक्ल के दृष्टिकोण से काफी प्रभावित हैं किन्तु उन्होंने इस ग्रन्थ में आचार्य शुक्ल के युगीन दृष्टिकोण और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के परम्परावादी दृष्टिकोण में परस्पर सामञ्जस स्थापित करने की भरपूर कोशिश की है।
एक ओर जहाँ पूर्व में वर्णित साहित्येतिहासकारों ने निजी प्रयासों से हिन्दी साहित्येतिहास सम्बन्धी स्वरचित ग्रन्थ प्रस्तुत किया है, वहीं कुछ साहित्यकारों ने मिलकर इस क्षेत्र में कार्य किया है। डॉ० धीरेन्द्र वर्मा के सम्पादन में ‘हिन्दी साहित्य’ नामक साहित्येतिहास ग्रन्थ वर्ष 1933 ई० में प्रकाशन में आया, जिसमें सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य को तीन काल खण्डों- आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक में वर्गीकृत किया है। इसमें आचार्य शुक्ल द्वारा रचित ‘हिन्दी शब्द सागर’ की भूमिका को आधार बनाया गया है, जिसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है।
इसी क्रम में डॉ० नगेन्द्र एवं डॉ० हरदयाल द्वारा सम्पादित ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ ग्रन्थ भी प्रमुख स्थान रखता है, जो सर्वप्रथम सन् 1973 में नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ था। यह ग्रन्थ भी अनेक लेखकों के सहयोग से तैयार किया गया है। इस ग्रन्थ में ईसा की सातवीं सदी से लेकर अब तक की कालावधि को क्रमश: चार कालखण्डों में विभक्त किया गया है।
1. आदिकाल
2. भक्तिकाल
3. रीतिकाल
4. आधुनिक काल
इन साहित्येतिहास ग्रन्थों के अतिरिक्त अनेक समीक्षात्मक ग्रन्थ एवं शोध ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, जिनमें हिन्दी साहित्य का सम्पूर्ण इतिहास बेशक न हो, किन्तु उसके किसी एक पक्ष को अवश्य दर्शाया गया है। उनमें प्रमुख हैं –
| क्र० | ग्रन्थ का नाम | ग्रन्थकार का नाम | प्रकाशन वर्ष (ई० में) |
| 01 | हिन्दी कोविद रत्नमाला (दो भागों में) | डॉ० श्यामसुन्दर दास | प्रथम भाग – 1909 ई० द्वितीय भाग – 1914 ई० |
| 02 | ए स्केच ऑफ़ हिन्दी लिटरेचर | पादरी एडविन ग्रीव्स | 1971 ई० |
| 03 | ए स्केच ऑफ़ हिन्दी लिटरेचर | एफ० ई० के० (फ्रैंक ई के) | 1920 ई० |
| 04 | ब्रजमाधुरी सार | वियोगी हरि | 1923 ई० |
| 05 | हिन्दी साहित्य विमर्श | पदुमलाल पुन्नालाल बक्शी | 1923 ई० |
| 06 | हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास | रामनरेश त्रिपाठी | 1923 ई० |
| 07 | हिन्दी भाषा का विकास | डॉ० श्यामसुन्दर दास | 1924 ई० |
| 08 | हिन्दी के मुसलमान कवि | गंगा प्रसाद सिंह अखौरी | 1926 ई० |
| 09 | सुकवि सरोज | गौरी शंकर द्विवेदी | 1927 ई० |
| 10 | कविता – कौमुदी | रामनरेश त्रिपाठी | 1928 ई० |
| 11 | हिन्दी भाषा एवं साहित्य | डॉ० श्यामसुन्दर दास | 1930 ई० |
| 12 | हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास | सूर्यकांत शास्त्री | 1930 ई० |
| 13 | हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास | अयोध्या सिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ | 1931 ई० |
| 14 | हिन्दी साहित्य का उपोद्घात | डाॅ मुंशीराम शर्मा | 1931 ई० |
| 15 | हिन्दी साहित्य का इतिहास | डाॅ रमाशंकर शुक्ल ‘रसाल’ | 1931 ई० |
| 16 | हिन्दी साहित्य का इतिहास | डाॅ ब्रजरत्न दास | 1932 ई० |
| 17 | आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास | कृष्णशंकर शुक्ल | 1934 ई० |
| 18 | साहित्य की झाँकी | गौरी शंकर सत्येन्द्र | 1936 ई० |
| 19 | पुरातत्व निबन्धावली | पं० राहुल सांकृत्यायन | 1937 ई० |
| 20 | हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास | बाबू गुलाबराय | 1937 ई० |
| 21 | हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास | गोपाललाल खन्ना | 1938 ई० |
| 22 | मॉडर्न हिन्दी लिटरेचर | डाॅ इन्द्रनाथ मदान | 1939 ई० |
| 23 | राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा | मोतीलाल मेनारिया | 1939 ई० |
| 24 | हिन्दी साहित्य का रेखाचित्र | उत्तमचन्द्र श्रीवास्तव | 1940 ई० |
| 25 | खड़ी बोली हिन्दी साहित्य का इतिहास | डाॅ ब्रजरत्न दास | 1941 ई० |
| 26 | आधुनिक हिन्दी साहित्य | लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय | 1941 ई० |
| 27 | आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास | डाॅ कृष्णलाल | 1942 ई० |
| 28 | हिन्दी साहित्य: बीसवीं शताब्दी | आचार्य नन्द दुलारे वाजपेयी | 1945 ई० |
| 29 | हिन्दी काव्यधारा | पं० राहुल सांकृत्यायन | 1944 ई० |
| 30 | हिन्दी वीरकाव्य | डाॅ टीकमसिंह तोमर | 1945 ई० |
| 31 | रीतिकाव्य की भूमिका | डाॅ नगेंद्र | 1949 ई० |
| 32 | आधुनिक हिन्दी साहित्य | आचार्य नन्द दुलारे वाजपेयी | 1950 ई० |
| 33 | उत्तरी भारत की संत परंपरा | परशुराम चतुर्वेदी | 1951 ई० |
| 34 | हिन्दी साहित्य का अतीत (दो भागों में) | आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र | प्रथम भाग–1959 ई० द्वितीय भाग – 1960 ई० |
| 35 | साहित्य का इतिहास दर्शन | डाॅ नलिन विलोचन शर्मा | 1960 ई० |
| 36 | हिन्दी साहित्य का बृहद् इतिहास (16 भाग) | ‘नागरी प्रचारिणी सभा’ द्वारा प्रकाशित | 1961 ई० |
| 37 | आधुनिक हिन्दी का आधुनिक | नारायण चतुर्वेदी | 1973 ई० |
| 38 | साहित्य एवं इतिहास दृष्टि | मैनेजर पाण्डेय | 1981 ई० |
| 39 | हिन्दी साहित्य का सरल इतिहास | विश्वनाथ त्रिपाठी | 1985 ई० |
| 40 | हिन्दी साहित्य और संवेदना का विकास | डाॅ रामस्वरूप चतुर्वेदी | 1986 ई० |
| 41 | हिन्दी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास | प्रोफ़ेसर वासुदेव सिंह | 1993 ई० |
| 42 | हिन्दी साहित्य का नया इतिहास | डाॅ बच्चन सिंह | 1995 ई० |
| 43 | हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास | डाॅ बच्चन सिंह | 1996 ई० |
| 44 | हिन्दी साहित्य का आधा इतिहास | सुमन राजे | 2003 ई० |
| 45 | हिन्दी साहित्य का मौखिक इतिहास | सम्पादक – नीलाभ | 2004 ई० |
| 46 | हिन्दी साहित्य का विवेचनपरक इतिहास | मोहन अवस्थी | 2008 ई० |
| 47 | हिन्दी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास | डाॅ भागीरथ मिश्र | 2010 ई० |
| 48 | हिन्दी साहित्य का ओझल नारी इतिहास | नीरजा माधव | 2012 ई० |
| 49 | हिन्दी साहित्य का इतिहास | हेमन्त कुकरेती | 2015 ई० |
| 50 | हिन्दी साहित्य का समग्र इतिहास | राम किशोर शर्मा | 2019 ई० |